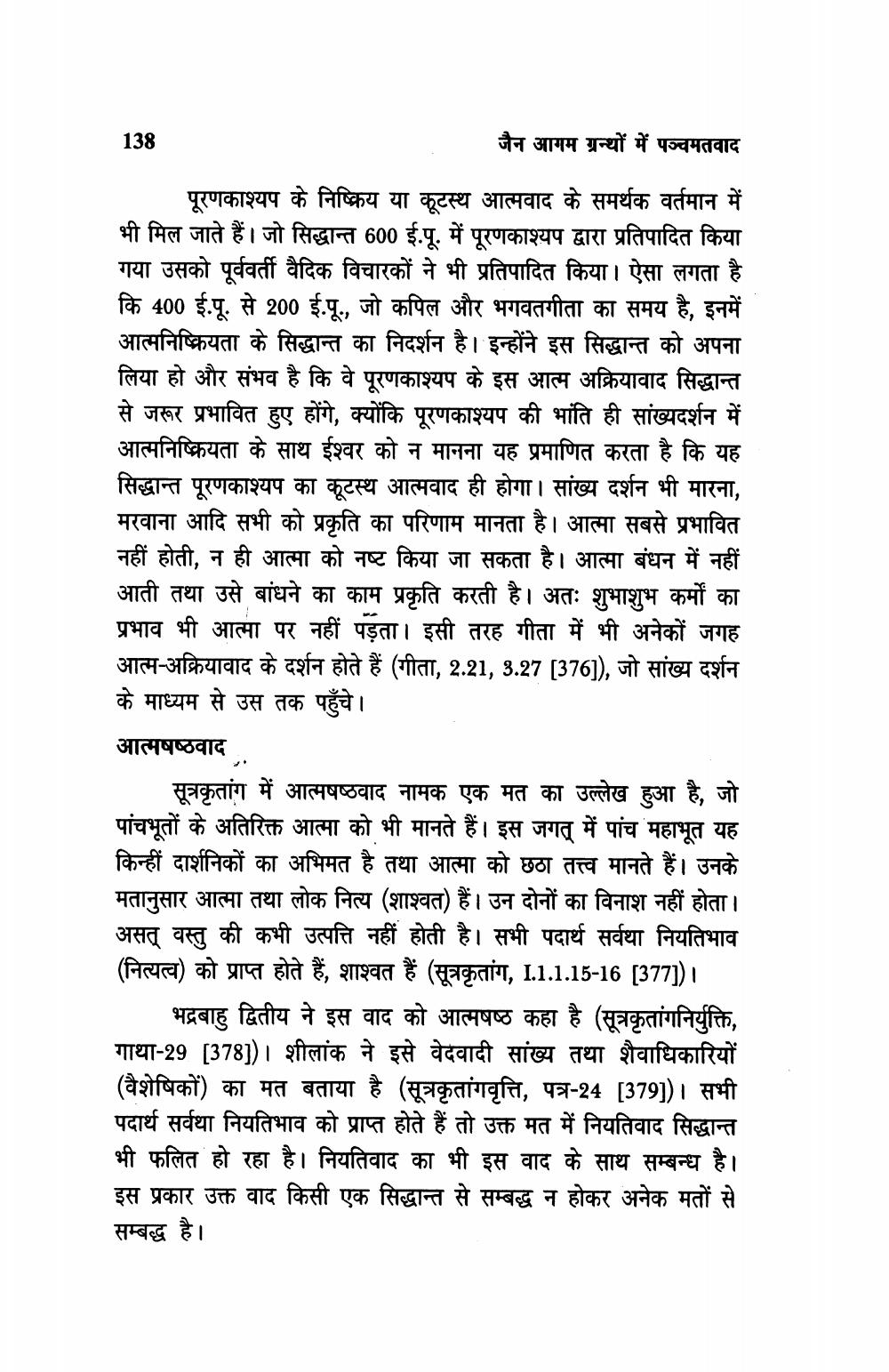________________
138
जैन आगम ग्रन्थों में पञ्चमतवाद
पूरणकाश्यप के निष्क्रिय या कूटस्थ आत्मवाद के समर्थक वर्तमान में भी मिल जाते हैं। जो सिद्धान्त 600 ई.पू. में पूरणकाश्यप द्वारा प्रतिपादित किया गया उसको पूर्ववर्ती वैदिक विचारकों ने भी प्रतिपादित किया। ऐसा लगता है कि 400 ई.पू. से 200 ई.पू., जो कपिल और भगवतगीता का समय है, इनमें आत्मनिष्क्रियता के सिद्धान्त का निदर्शन है। इन्होंने इस सिद्धान्त को अपना लिया हो और संभव है कि वे पूरणकाश्यप के इस आत्म अक्रियावाद सिद्धान्त से जरूर प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि पूरणकाश्यप की भांति ही सांख्यदर्शन में आत्मनिष्क्रियता के साथ ईश्वर को न मानना यह प्रमाणित करता है कि यह सिद्धान्त पूरणकाश्यप का कूटस्थ आत्मवाद ही होगा। सांख्य दर्शन भी मारना, मरवाना आदि सभी को प्रकृति का परिणाम मानता है। आत्मा सबसे प्रभावित नहीं होती, न ही आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। आत्मा बंधन में नहीं आती तथा उसे बांधने का काम प्रकृति करती है। अतः शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव भी आत्मा पर नहीं पड़ता। इसी तरह गीता में भी अनेकों जगह आत्म-अक्रियावाद के दर्शन होते हैं (गीता, 2.21, 3.27 [376]), जो सांख्य दर्शन के माध्यम से उस तक पहुँचे। आत्मषष्ठवाद
सूत्रकृतांग में आत्मषष्ठवाद नामक एक मत का उल्लेख हुआ है, जो पांचभूतों के अतिरिक्त आत्मा को भी मानते हैं। इस जगत् में पांच महाभूत यह किन्हीं दार्शनिकों का अभिमत है तथा आत्मा को छठा तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार आत्मा तथा लोक नित्य (शाश्वत) हैं। उन दोनों का विनाश नहीं होता। असत् वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। सभी पदार्थ सर्वथा नियतिभाव (नित्यत्व) को प्राप्त होते हैं, शाश्वत हैं (सूत्रकृतांग, I.1.1.15-16 [377])।
भद्रबाहु द्वितीय ने इस वाद को आत्मषष्ठ कहा है (सूत्रकृतांगनियुक्ति, गाथा-29 [378])। शीलांक ने इसे वेदवादी सांख्य तथा शैवाधिकारियों (वैशेषिकों) का मत बताया है (सूत्रकृतांगवृत्ति, पत्र-24 [379])। सभी पदार्थ सर्वथा नियतिभाव को प्राप्त होते हैं तो उक्त मत में नियतिवाद सिद्धान्त भी फलित हो रहा है। नियतिवाद का भी इस वाद के साथ सम्बन्ध है। इस प्रकार उक्त वाद किसी एक सिद्धान्त से सम्बद्ध न होकर अनेक मतों से सम्बद्ध है।