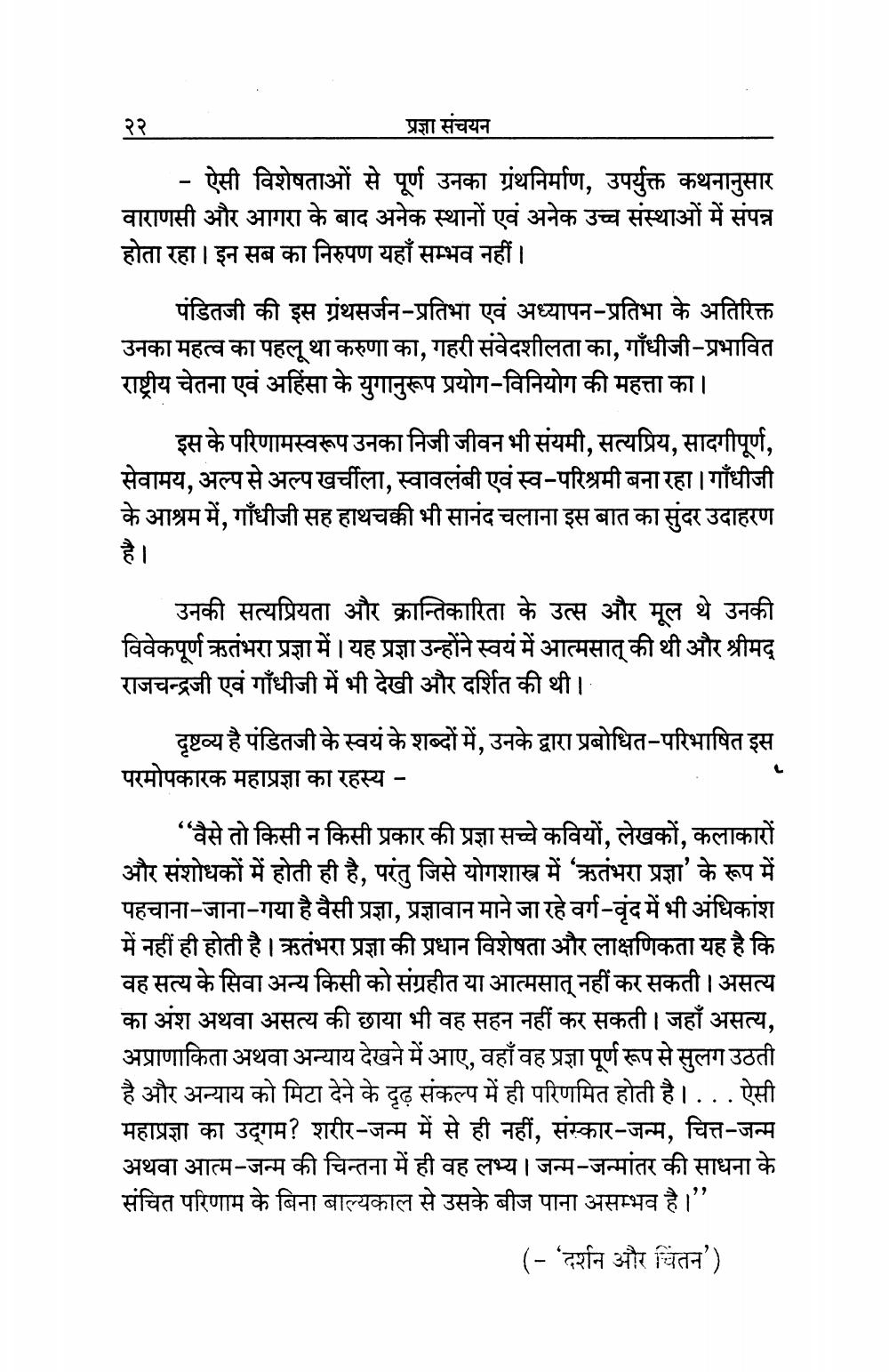________________
प्रज्ञा संचयन
- ऐसी विशेषताओं से पूर्ण उनका ग्रंथनिर्माण, उपर्युक्त कथनानुसार वाराणसी और आगरा के बाद अनेक स्थानों एवं अनेक उच्च संस्थाओं में संपन्न होता रहा। इन सब का निरुपण यहाँ सम्भव नहीं।
पंडितजी की इस ग्रंथसर्जन-प्रतिभा एवं अध्यापन-प्रतिभा के अतिरिक्त उनका महत्व का पहलू था करुणा का, गहरी संवेदशीलता का, गाँधीजी-प्रभावित राष्ट्रीय चेतना एवं अहिंसा के युगानुरूप प्रयोग-विनियोग की महत्ता का।
इस के परिणामस्वरूप उनका निजी जीवन भी संयमी, सत्यप्रिय, सादगीपूर्ण, सेवामय, अल्पसे अल्प खर्चीला, स्वावलंबी एवं स्व-परिश्रमी बना रहा । गाँधीजी के आश्रम में, गाँधीजी सह हाथचक्की भी सानंद चलाना इस बात का सुंदर उदाहरण
उनकी सत्यप्रियता और क्रान्तिकारिता के उत्स और मूल थे उनकी विवेकपूर्ण ऋतंभरा प्रज्ञा में । यह प्रज्ञा उन्होंने स्वयं में आत्मसात् की थी और श्रीमद् राजचन्द्रजी एवं गाँधीजी में भी देखी और दर्शित की थी।
दृष्टव्य है पंडितजी के स्वयं के शब्दों में, उनके द्वारा प्रबोधित-परिभाषित इस परमोपकारक महाप्रज्ञा का रहस्य -
“वैसे तो किसी न किसी प्रकार की प्रज्ञा सच्चे कवियों, लेखकों, कलाकारों और संशोधकों में होती ही है, परंतु जिसे योगशास्त्र में 'ऋतंभरा प्रज्ञा' के रूप में पहचाना-जाना-गया है वैसी प्रज्ञा, प्रज्ञावान माने जा रहे वर्ग-वृंद में भी अंधिकांश में नहीं ही होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा की प्रधान विशेषता और लाक्षणिकता यह है कि वह सत्य के सिवा अन्य किसी को संग्रहीत या आत्मसात् नहीं कर सकती। असत्य का अंश अथवा असत्य की छाया भी वह सहन नहीं कर सकती। जहाँ असत्य, अप्राणाकिता अथवा अन्याय देखने में आए, वहाँ वह प्रज्ञा पूर्ण रूप से सुलग उठती है और अन्याय को मिटा देने के दृढ़ संकल्प में ही परिणमित होती है। . . . ऐसी महाप्रज्ञा का उद्गम? शरीर-जन्म में से ही नहीं, संस्कार-जन्म, चित्त-जन्म अथवा आत्म-जन्म की चिन्तना में ही वह लभ्य । जन्म-जन्मांतर की साधना के संचित परिणाम के बिना बाल्यकाल से उसके बीज पाना असम्भव है।"
(- ‘दर्शन और चिंतन')