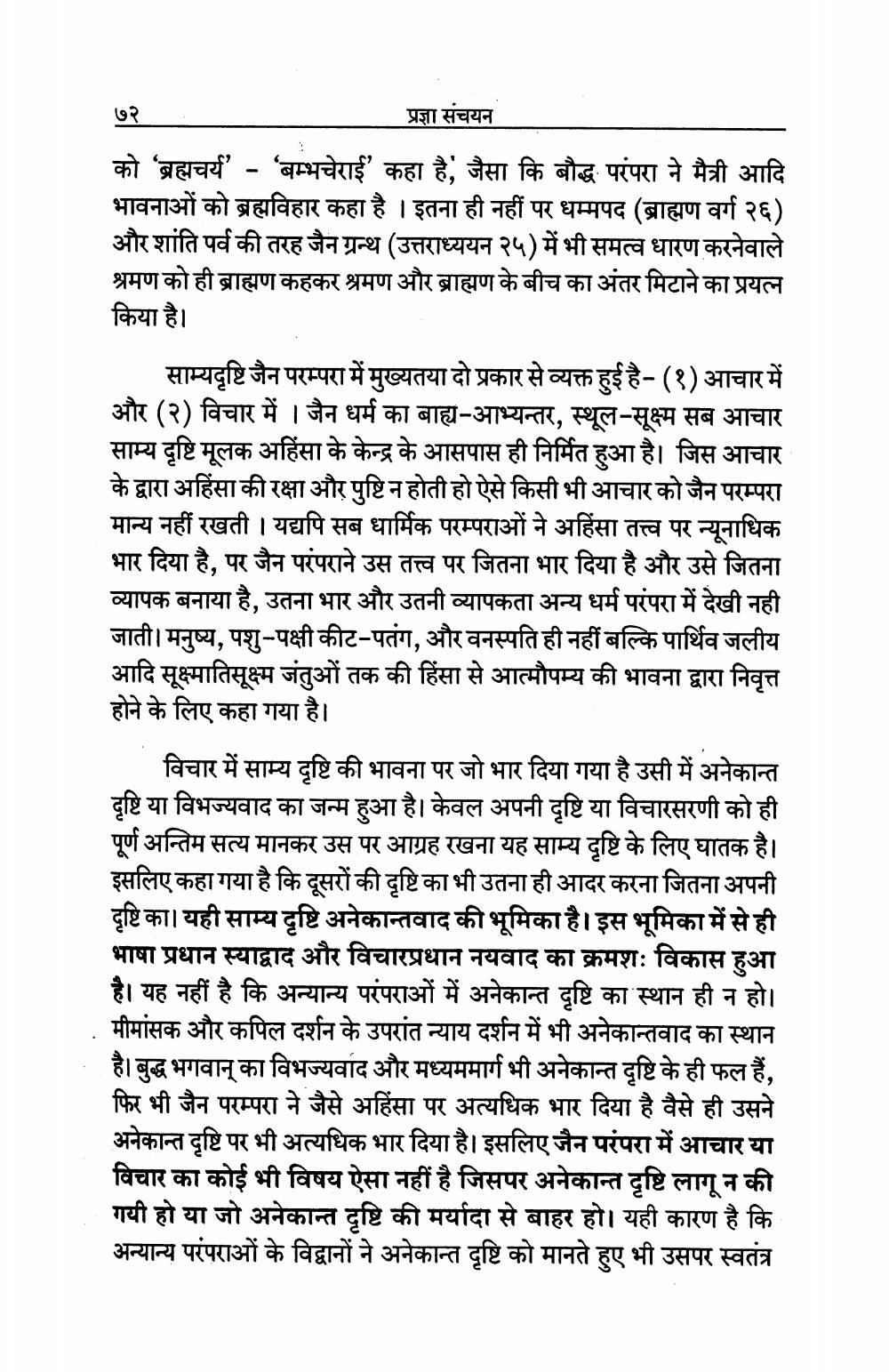________________
प्रज्ञा संचयन
को 'ब्रह्मचर्य' - 'बम्भचेराई' कहा है, जैसा कि बौद्ध परंपरा ने मैत्री आदि भावनाओं को ब्रह्मविहार कहा है । इतना ही नहीं पर धम्मपद (ब्राह्मण वर्ग २६)
और शांति पर्व की तरह जैन ग्रन्थ (उत्तराध्ययन २५) में भी समत्व धारण करनेवाले श्रमण को ही ब्राह्मण कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच का अंतर मिटाने का प्रयत्न किया है।
साम्यदृष्टि जैन परम्परा में मुख्यतया दो प्रकार से व्यक्त हुई है- (१) आचार में और (२) विचार में । जैन धर्म का बाह्य-आभ्यन्तर, स्थूल-सूक्ष्म सब आचार साम्य दृष्टि मूलक अहिंसा के केन्द्र के आसपास ही निर्मित हुआ है। जिस आचार के द्वारा अहिंसा की रक्षा और पुष्टि न होती हो ऐसे किसी भी आचार को जैन परम्परा मान्य नहीं रखती । यद्यपि सब धार्मिक परम्पराओं ने अहिंसा तत्त्व पर न्यूनाधिक भार दिया है, पर जैन परंपराने उस तत्त्व पर जितना भार दिया है और उसे जितना व्यापक बनाया है, उतना भार और उतनी व्यापकता अन्य धर्म परंपरा में देखी नही जाती। मनुष्य, पशु-पक्षी कीट-पतंग, और वनस्पति ही नहीं बल्कि पार्थिव जलीय आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म जंतुओं तक की हिंसा से आत्मौपम्य की भावना द्वारा निवृत्त होने के लिए कहा गया है। ___ विचार में साम्य दृष्टि की भावना पर जो भार दिया गया है उसी में अनेकान्त दृष्टि या विभज्यवाद का जन्म हुआ है। केवल अपनी दृष्टि या विचारसरणी को ही पूर्ण अन्तिम सत्य मानकर उस पर आग्रह रखना यह साम्य दृष्टि के लिए घातक है। इसलिए कहा गया है कि दूसरों की दृष्टि का भी उतना ही आदर करना जितना अपनी दृष्टि का। यही साम्य दृष्टि अनेकान्तवाद की भूमिका है। इस भूमिका में से ही भाषा प्रधान स्याद्वाद और विचारप्रधान नयवाद का क्रमशः विकास हुआ है। यह नहीं है कि अन्यान्य परंपराओं में अनेकान्त दृष्टि का स्थान ही न हो। मीमांसक और कपिल दर्शन के उपरांत न्याय दर्शन में भी अनेकान्तवाद का स्थान है। बुद्ध भगवान् का विभज्यवाद और मध्यममार्ग भी अनेकान्त दृष्टि के ही फल हैं, फिर भी जैन परम्परा ने जैसे अहिंसा पर अत्यधिक भार दिया है वैसे ही उसने अनेकान्त दृष्टि पर भी अत्यधिक भार दिया है। इसलिए जैन परंपरा में आचार या विचार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसपर अनेकान्त दृष्टि लागून की गयी हो या जो अनेकान्त दृष्टि की मर्यादा से बाहर हो। यही कारण है कि अन्यान्य परंपराओं के विद्वानों ने अनेकान्त दृष्टि को मानते हुए भी उसपर स्वतंत्र