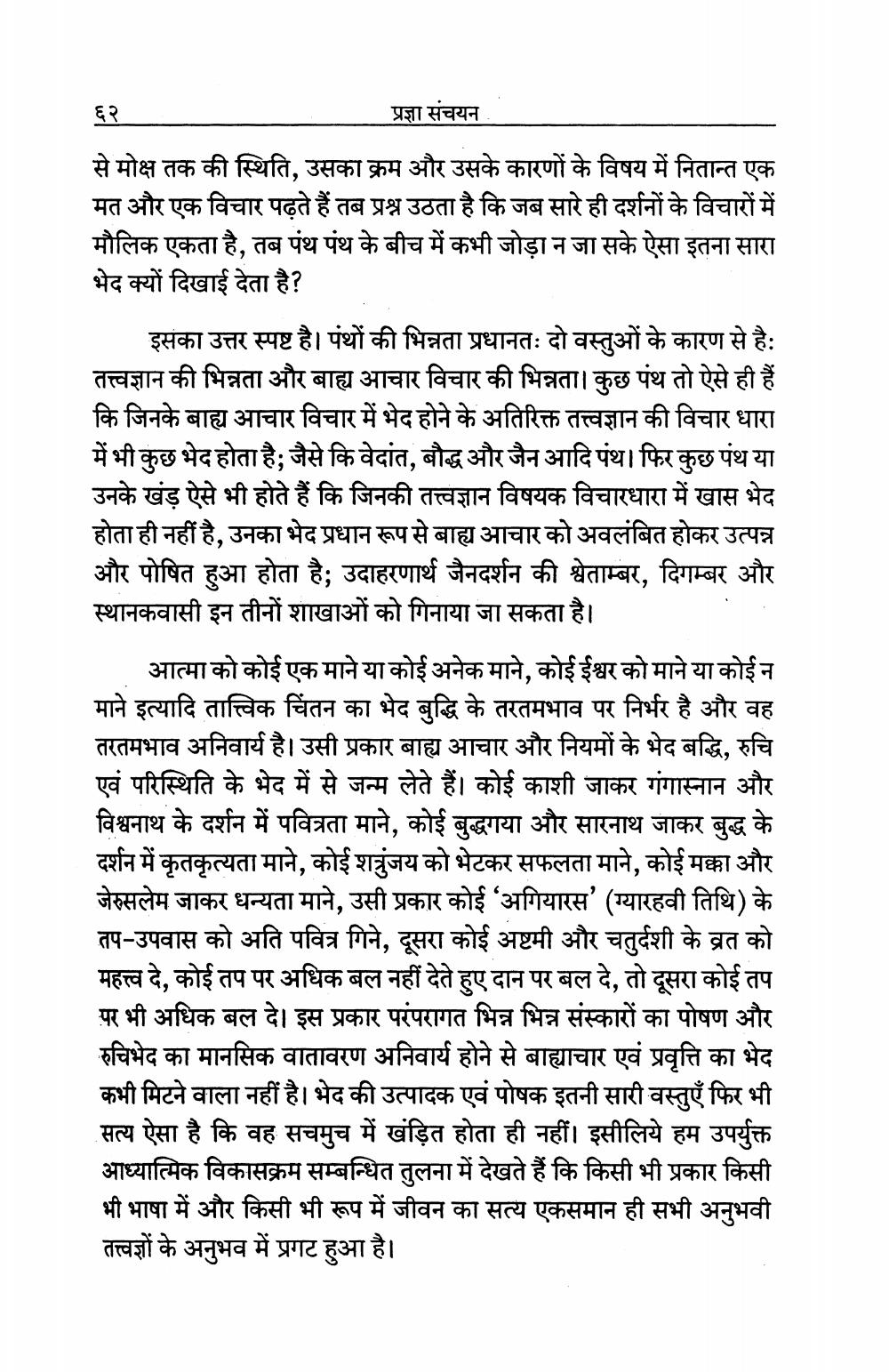________________
६२
प्रज्ञा संचयन
से मोक्ष तक की स्थिति, उसका क्रम और उसके कारणों के विषय में नितान्त एक मत और एक विचार पढ़ते हैं तब प्रश्न उठता है कि जब सारे ही दर्शनों के विचारों में मौलिक एकता है, तब पंथ पंथ के बीच में कभी जोड़ा न जा सके ऐसा इतना सारा भेद क्यों दिखाई देता है?
इसका उत्तर स्पष्ट है। पंथों की भिन्नता प्रधानतः दो वस्तुओं के कारण से है: तत्त्वज्ञान की भिन्नता और बाह्य आचार विचार की भिन्नता। कुछ पंथ तो ऐसे ही हैं कि जिनके बाह्य आचार विचार में भेद होने के अतिरिक्त तत्त्वज्ञान की विचार धारा में भी कुछ भेद होता है; जैसे कि वेदांत, बौद्ध और जैन आदि पंथ। फिर कुछ पंथ या उनके खंड़ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी तत्त्वज्ञान विषयक विचारधारा में खास भेद होता ही नहीं है, उनका भेद प्रधान रूप से बाह्य आचार को अवलंबित होकर उत्पन्न
और पोषित हआ होता है; उदाहरणार्थ जैनदर्शन की श्वेताम्बर, दिगम्बर और स्थानकवासी इन तीनों शाखाओं को गिनाया जा सकता है। ___ आत्मा को कोई एक माने या कोई अनेक माने, कोई ईश्वर को माने या कोई न माने इत्यादि तात्त्विक चिंतन का भेद बुद्धि के तरतमभाव पर निर्भर है और वह तरतमभाव अनिवार्य है। उसी प्रकार बाह्य आचार और नियमों के भेद बद्धि, रुचि एवं परिस्थिति के भेद में से जन्म लेते हैं। कोई काशी जाकर गंगास्नान और विश्वनाथ के दर्शन में पवित्रता माने, कोई बुद्धगया और सारनाथ जाकर बुद्ध के दर्शन में कृतकृत्यता माने, कोई शत्रुजय को भेटकर सफलता माने, कोई मक्का और जेरुसलेम जाकर धन्यता माने, उसी प्रकार कोई ‘अगियारस' (ग्यारहवी तिथि) के तप-उपवास को अति पवित्र गिने, दूसरा कोई अष्टमी और चतुर्दशी के व्रत को महत्त्व दे, कोई तप पर अधिक बल नहीं देते हुए दान पर बल दे, तो दूसरा कोई तप पर भी अधिक बल दे। इस प्रकार परंपरागत भिन्न भिन्न संस्कारों का पोषण और रुचिभेद का मानसिक वातावरण अनिवार्य होने से बाह्याचार एवं प्रवृत्ति का भेद कभी मिटने वाला नहीं है। भेद की उत्पादक एवं पोषक इतनी सारी वस्तुएँ फिर भी सत्य ऐसा है कि वह सचमुच में खंड़ित होता ही नहीं। इसीलिये हम उपर्युक्त आध्यात्मिक विकासक्रम सम्बन्धित तुलना में देखते हैं कि किसी भी प्रकार किसी भी भाषा में और किसी भी रूप में जीवन का सत्य एकसमान ही सभी अनुभवी तत्त्वज्ञों के अनुभव में प्रगट हुआ है।