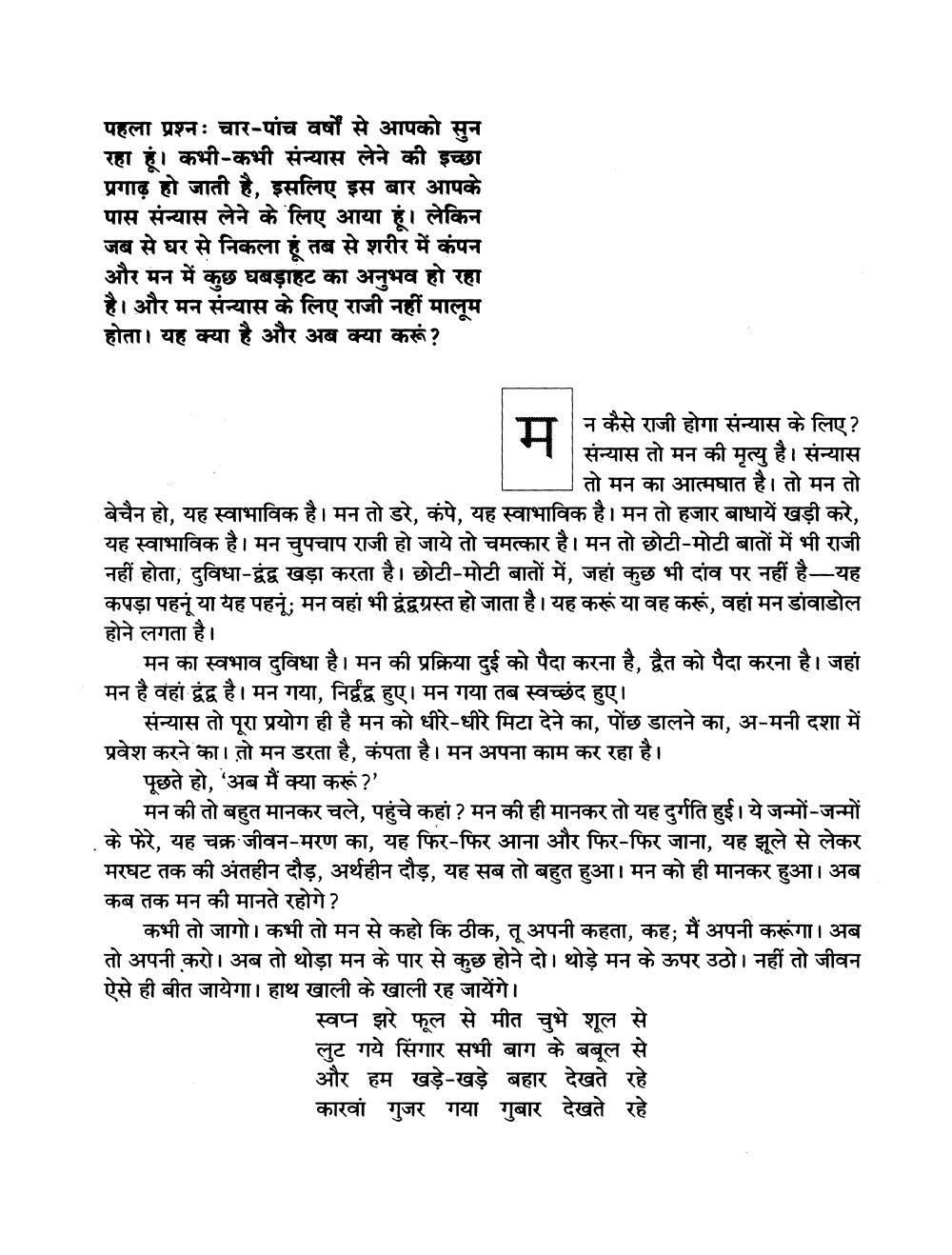________________
पहला प्रश्नः चार-पांच वर्षों से आपको सुन रहा हूं। कभी-कभी संन्यास लेने की इच्छा प्रगाढ़ हो जाती है, इसलिए इस बार आपके पास संन्यास लेने के लिए आया हूं। लेकिन जब से घर से निकला हूं तब से शरीर में कंपन
और मन में कुछ घबड़ाहट का अनुभव हो रहा है। और मन संन्यास के लिए राजी नहीं मालूम होता। यह क्या है और अब क्या करूं?
न कैसे राजी होगा संन्यास के लिए? संन्यास तो मन की मृत्यु है। संन्यास
तो मन का आत्मघात है। तो मन तो बेचैन हो, यह स्वाभाविक है। मन तो डरे, कंपे, यह स्वाभाविक है। मन तो हजार बाधायें खड़ी करे, यह स्वाभाविक है। मन चुपचाप राजी हो जाये तो चमत्कार है। मन तो छोटी-मोटी बातों में भी राजी नहीं होता, दुविधा-द्वंद्व खड़ा करता है। छोटी-मोटी बातों में, जहां कुछ भी दांव पर नहीं है—यह कपड़ा पहनूं या यह पहनूं; मन वहां भी द्वंद्वग्रस्त हो जाता है। यह करूं या वह करूं, वहां मन डांवाडोल होने लगता है।
मन का स्वभाव दुविधा है। मन की प्रक्रिया दुई को पैदा करना है, द्वैत को पैदा करना है। जहां मन है वहां द्वंद्व है। मन गया, निर्द्वद्व हुए। मन गया तब स्वच्छंद हुए। ___ संन्यास तो पूरा प्रयोग ही है मन को धीरे-धीरे मिटा देने का, पोंछ डालने का, अ-मनी दशा में प्रवेश करने का। तो मन डरता है, कंपता है। मन अपना काम कर रहा है।
पूछते हो, 'अब मैं क्या करूं?'
मन की तो बहुत मानकर चले, पहुंचे कहां? मन की ही मानकर तो यह दुर्गति हुई। ये जन्मों-जन्मों के फेरे, यह चक्र जीवन-मरण का, यह फिर-फिर आना और फिर-फिर जाना, यह झूले से लेकर मरघट तक की अंतहीन दौड़, अर्थहीन दौड़, यह सब तो बहुत हुआ। मन को ही मानकर हुआ। अब कब तक मन की मानते रहोगे?
कभी तो जागो। कभी तो मन से कहो कि ठीक, तू अपनी कहता, कह; मैं अपनी करूंगा। अब तो अपनी करो। अब तो थोड़ा मन के पार से कुछ होने दो। थोड़े मन के ऊपर उठो। नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत जायेगा। हाथ खाली के खाली रह जायेंगे।
स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गये सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे