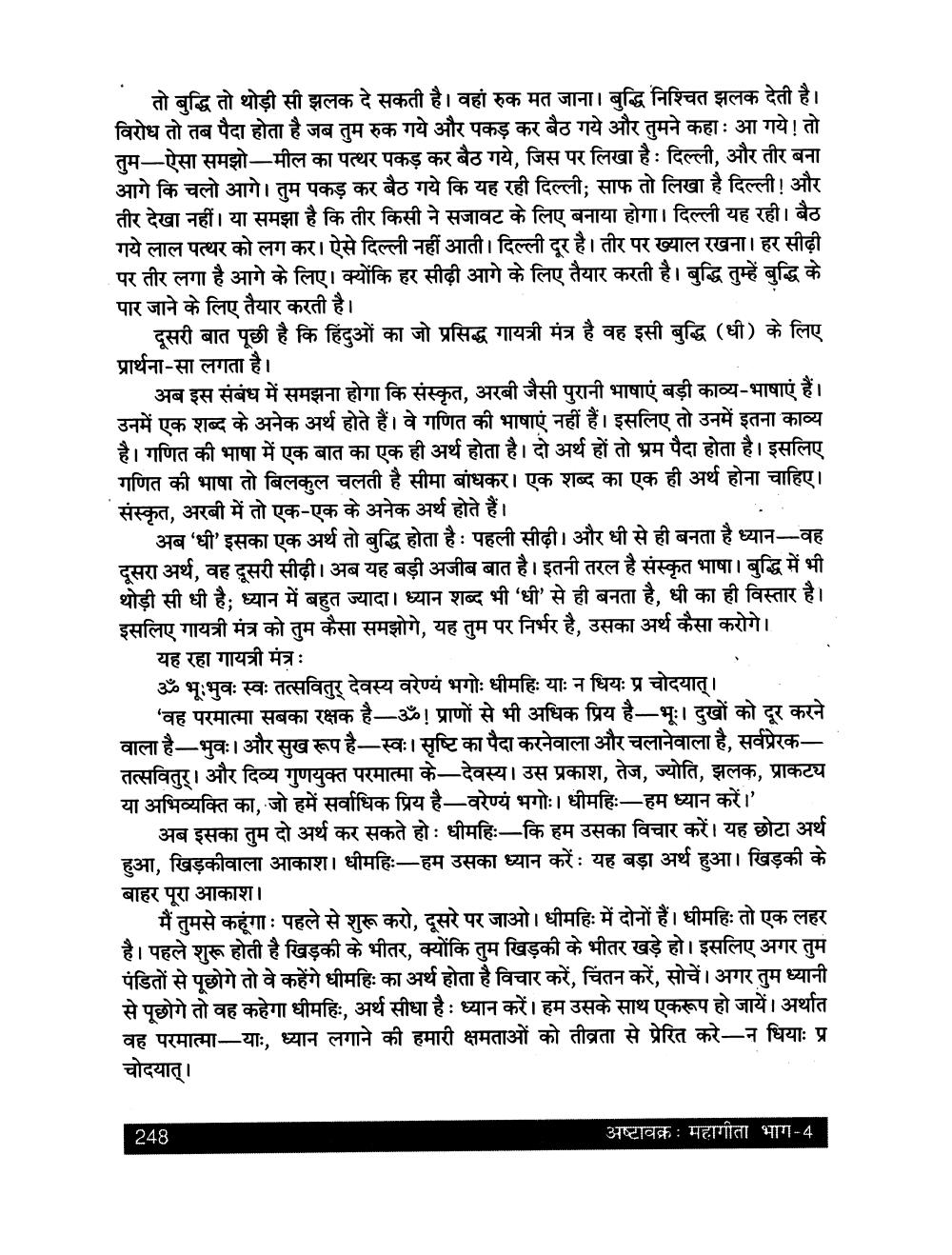________________
तो बुद्धि तो थोड़ी सी झलक दे सकती है। वहां रुक मत जाना । बुद्धि निश्चित झलक देती है। विरोध तो तब पैदा होता है जब तुम रुक गये और पकड़ कर बैठ गये और तुमने कहा आ गये ! तो तुम — ऐसा समझो - मील का पत्थर पकड़ कर बैठ गये, जिस पर लिखा है: दिल्ली, और तीर बना आगे कि चलो आगे। तुम पकड़ कर बैठ गये कि यह रही दिल्ली; साफ तो लिखा है दिल्ली ! और तीर देखा नहीं । या समझा है कि तीर किसी ने सजावट के लिए बनाया होगा। दिल्ली यह रही । बैठ गये लाल पत्थर को लग कर ऐसे दिल्ली नहीं आती। दिल्ली दूर है। तीर पर ख्याल रखना। हर सीढ़ी पर तीर लगा है आगे के लिए। क्योंकि हर सीढ़ी आगे के लिए तैयार करती है । बुद्धि तुम्हें बुद्धि के पार जाने के लिए तैयार करती है।
I
दूसरी बात पूछी है कि हिंदुओं का जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह इसी बुद्धि (धी) के लिए प्रार्थना-सा लगता है।
अब इस संबंध में समझना होगा कि संस्कृत, अरबी जैसी पुरानी भाषाएं बड़ी काव्य- भाषाएं हैं। उनमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । वे गणित की भाषाएं नहीं हैं। इसलिए तो उनमें इतना काव्य
गणित की भाषा में एक बात का एक ही अर्थ होता है। दो अर्थ हों तो भ्रम पैदा होता है। इसलिए गणित की भाषा तो बिलकुल चलती है सीमा बांधकर । एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए । संस्कृत, अरबी में तो एक-एक के अनेक अर्थ होते हैं।
अब 'धी' इसका एक अर्थ तो बुद्धि होता है : पहली सीढ़ी। और धी से ही बनता है ध्यान – वह दूसरा अर्थ, वह दूसरी सीढ़ी। अब यह बड़ी अजीब बात है । इतनी तरल है संस्कृत भाषा । बुद्धि में भी थोड़ी सी धी है; ध्यान में बहुत ज्यादा । ध्यान शब्द भी 'धी' से ही बनता है, धी का ही विस्तार है । इसलिए गायत्री मंत्र को तुम कैसा समझोगे, यह तुम पर निर्भर है, उसका अर्थ कैसा करोगे।
यह रहा गायत्री मंत्र :
ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुर् देवस्य वरेण्यं भगोः धीमहिः याः न धियः प्रचोदयात् ।
‘वह परमात्मा सबका रक्षक है - ॐ ! प्राणों से भी अधिक प्रिय है- भूः । दुखों को दूर करने वाला है — भुवः । और सुख रूप है— स्वः । सृष्टि का पैदा करनेवाला और चलानेवाला है, सर्वप्रेरक— तत्सवितुर्| और दिव्य गुणयुक्त परमात्मा के — देवस्य । उस प्रकाश, तेज, ज्योति, झलक, प्राकट्य या अभिव्यक्ति का, जो हमें सर्वाधिक प्रिय है— वरेण्यं भगोः । धीमहि: - हम ध्यान करें ।'
अब इसका तुम दो अर्थ कर सकते हो : धीमहि: - कि हम उसका विचार करें। यह छोटा अर्थ हुआ, खिड़कीवाला आकाश । धीमहि:- हम उसका ध्यान करें: यह बड़ा अर्थ हुआ । खिड़की के बाहर पूरा आकाश ।
मैं तुमसे कहूंगा : पहले से शुरू करो, दूसरे पर जाओ। धीमहि: में दोनों हैं। धीमहि: तो एक लहर है। पहले शुरू होती है खिड़की के भीतर, क्योंकि तुम खिड़की के भीतर खड़े हो । इसलिए अगर तुम पंडितों से पूछोगे तो वे कहेंगे धीमहि: का अर्थ होता है विचार करें, चिंतन करें, सोचें। अगर तुम ध्यानी से पूछोगे तो वह कहेगा धीमहि:, अर्थ सीधा है: ध्यान करें। हम उसके साथ एकरूप हो जायें । अर्थात वह परमात्मा — याः, ध्यान लगाने की हमारी क्षमताओं को तीव्रता से प्रेरित करे-न धियाः प्र चोदयात्।
248
अष्टावक्र: महागीता भाग-4