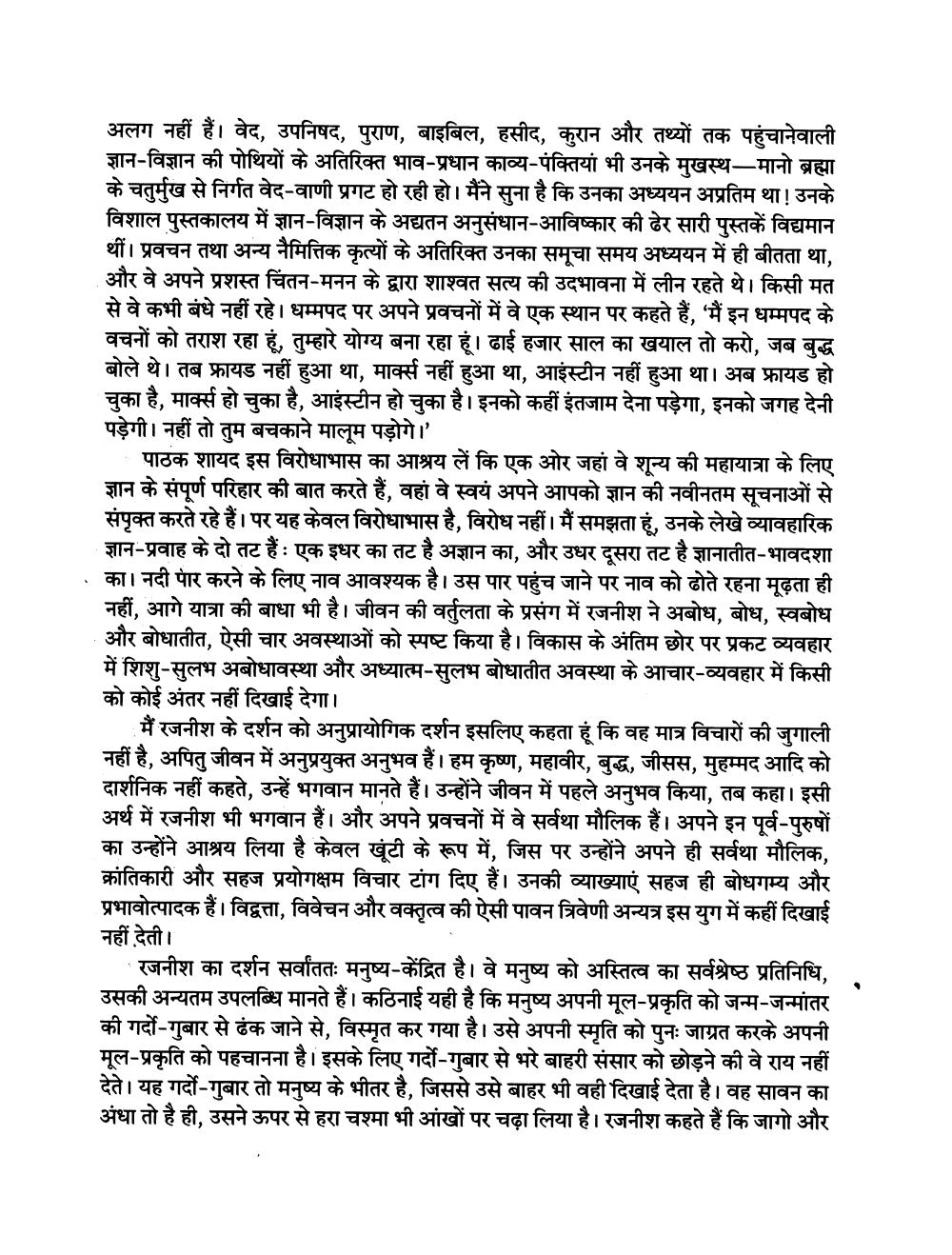________________
अलग नहीं हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, बाइबिल, हसीद, कुरान और तथ्यों तक पहुंचानेवाली ज्ञान-विज्ञान की पोथियों के अतिरिक्त भाव-प्रधान काव्य-पंक्तियां भी उनके मुखस्थ–मानो ब्रह्मा के चतुर्मुख से निर्गत वेद-वाणी प्रगट हो रही हो। मैंने सुना है कि उनका अध्ययन अप्रतिम था! उनके विशाल पुस्तकालय में ज्ञान-विज्ञान के अद्यतन अनुसंधान-आविष्कार की ढेर सारी पुस्तकें विद्यमान थीं। प्रवचन तथा अन्य नैमित्तिक कृत्यों के अतिरिक्त उनका समूचा समय अध्ययन में ही बीतता था, और वे अपने प्रशस्त चिंतन-मनन के द्वारा शाश्वत सत्य की उदभावना में लीन रहते थे। किसी मत से वे कभी बंधे नहीं रहे। धम्मपद पर अपने प्रवचनों में वे एक स्थान पर कहते हैं, 'मैं इन धम्मपद के वचनों को तराश रहा है, तम्हारे योग्य बना रहा है। ढाई हजार साल का खयाल तो करो,
बुद्ध बोले थे। तब फ्रायड नहीं हुआ था, मार्क्स नहीं हुआ था, आइंस्टीन नहीं हुआ था। अब फ्रायड हो चुका है, मार्क्स हो चुका है, आइंस्टीन हो चुका है। इनको कहीं इंतजाम देना पड़ेगा, इनको जगह देनी पड़ेगी। नहीं तो तुम बचकाने मालूम पड़ोगे।'
पाठक शायद इस विरोधाभास का आश्रय लें कि एक ओर जहां वे शून्य की महायात्रा के लिए ज्ञान के संपूर्ण परिहार की बात करते हैं, वहां वे स्वयं अपने आपको ज्ञान की नवीनतम सूचनाओं से संपृक्त करते रहे हैं। पर यह केवल विरोधाभास है, विरोध नहीं। मैं समझता हूं, उनके लेखे व्यावहारिक
ज्ञान-प्रवाह के दो तट हैं : एक इधर का तट है अज्ञान का, और उधर दूसरा तट है ज्ञानातीत-भावदशा . का। नदी पार करने के लिए नाव आवश्यक है। उस पार पहुंच जाने पर नाव को ढोते रहना मूढ़ता ही नहीं, आगे यात्रा की बाधा भी है। जीवन की वर्तुलता के प्रसंग में रजनीश ने अबोध, बोध, स्वबोध
और बोधातीत, ऐसी चार अवस्थाओं को स्पष्ट किया है। विकास के अंतिम छोर पर प्रकट व्यवहार में शिशु-सुलभ अबोधावस्था और अध्यात्म-सुलभ बोधातीत अवस्था के आचार-व्यवहार में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। ___ मैं रजनीश के दर्शन को अनुप्रायोगिक दर्शन इसलिए कहता हूं कि वह मात्र विचारों की जुगाली नहीं है, अपितु जीवन में अनुप्रयुक्त अनुभव हैं। हम कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जीसस, मुहम्मद आदि को दार्शनिक नहीं कहते, उन्हें भगवान मानते हैं। उन्होंने जीवन में पहले अनुभव किया, तब कहा। इसी अर्थ में रजनीश भी भगवान हैं। और अपने प्रवचनों में वे सर्वथा मौलिक हैं। अपने इन पूर्व-पुरुषों का उन्होंने आश्रय लिया है केवल खूटी के रूप में, जिस पर उन्होंने अपने ही सर्वथा मौलिक, क्रांतिकारी और सहज प्रयोगक्षम विचार टांग दिए हैं। उनकी व्याख्याएं सहज ही बोधगम्य और प्रभावोत्पादक हैं। विद्वत्ता, विवेचन और वक्तृत्व की ऐसी पावन त्रिवेणी अन्यत्र इस युग में कहीं दिखाई नहीं देती।
रजनीश का दर्शन सर्वांततः मनुष्य-केंद्रित है। वे मनुष्य को अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, उसकी अन्यतम उपलब्धि मानते हैं। कठिनाई यही है कि मनुष्य अपनी मूल-प्रकृति को जन्म-जन्मांतर की गर्दो-गुबार से ढंक जाने से, विस्मृत कर गया है। उसे अपनी स्मृति को पुनः जाग्रत करके अपनी मूल-प्रकृति को पहचानना है। इसके लिए गर्दो-गुबार से भरे बाहरी संसार को छोड़ने की वे राय नहीं देते। यह गर्दो-गुबार तो मनुष्य के भीतर है, जिससे उसे बाहर भी वही दिखाई देता है। वह सावन का अंधा तो है ही, उसने ऊपर से हरा चश्मा भी आंखों पर चढ़ा लिया है। रजनीश कहते हैं कि जागो और