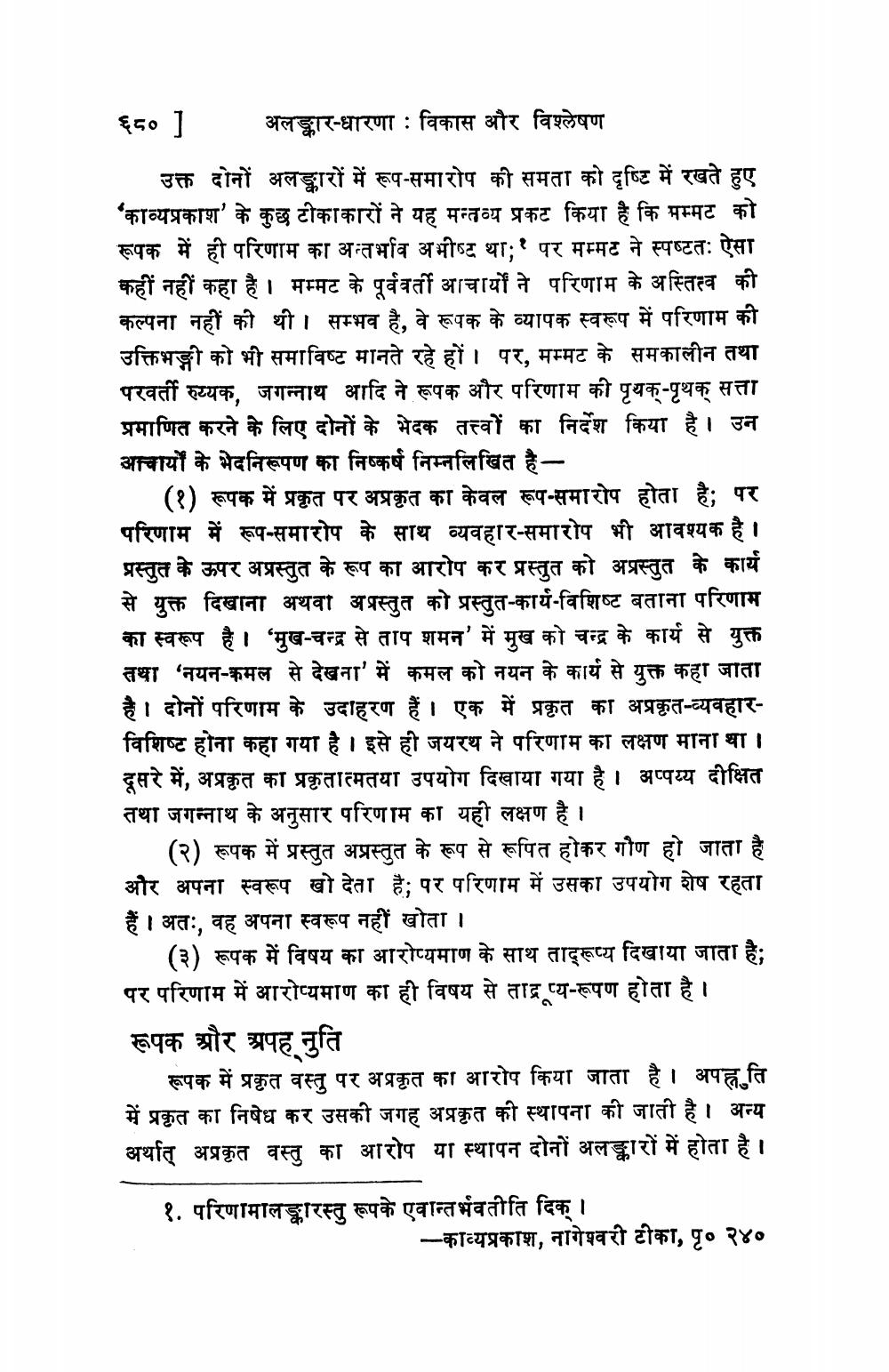________________
६८० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उक्त दोनों अलङ्कारों में रूप-समारोप की समता को दृष्टि में रखते हुए 'काव्यप्रकाश' के कुछ टीकाकारों ने यह मन्तव्य प्रकट किया है कि मम्मट को रूपक में ही परिणाम का अन्तर्भाव अभीष्ट था;' पर मम्मट ने स्पष्टतः ऐसा कहीं नहीं कहा है। मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों ने परिणाम के अस्तित्व की कल्पना नहीं की थी। सम्भव है, वे रूपक के व्यापक स्वरूप में परिणाम की उक्तिभङ्गी को भी समाविष्ट मानते रहे हों। पर, मम्मट के समकालीन तथा परवर्ती रुय्यक, जगन्नाथ आदि ने रूपक और परिणाम की पृथक्-पृथक् सत्ता प्रमाणित करने के लिए दोनों के भेदक तत्त्वों का निर्देश किया है। उन आचार्यों के भेदनिरूपण का निष्कर्ष निम्नलिखित है
(१) रूपक में प्रकृत पर अप्रकृत का केवल रूप-समारोप होता है; पर परिणाम में रूप-समारोप के साथ व्यवहार-समारोप भी आवश्यक है। प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत के रूप का आरोप कर प्रस्तुत को अप्रस्तुत के कार्य से युक्त दिखाना अथवा अप्रस्तुत को प्रस्तुत-कार्य-विशिष्ट बताना परिणाम का स्वरूप है। 'मुख-चन्द्र से ताप शमन' में मुख को चन्द्र के कार्य से युक्त तथा 'नयन-कमल से देखना' में कमल को नयन के कार्य से युक्त कहा जाता है। दोनों परिणाम के उदाहरण हैं। एक में प्रकृत का अप्रकृत-व्यवहारविशिष्ट होना कहा गया है । इसे ही जयरथ ने परिणाम का लक्षण माना था। दूसरे में, अप्रकृत का प्रकृतात्मतया उपयोग दिखाया गया है। अप्पय्य दीक्षित तथा जगन्नाथ के अनुसार परिणाम का यही लक्षण है।
(२) रूपक में प्रस्तुत अप्रस्तुत के रूप से रूपित होकर गौण हो जाता है और अपना स्वरूप खो देता है; पर परिणाम में उसका उपयोग शेष रहता हैं । अतः, वह अपना स्वरूप नहीं खोता ।
(३) रूपक में विषय का आरोप्यमाण के साथ ताप्य दिखाया जाता है; पर परिणाम में आरोप्यमाण का ही विषय से ताद्र प्य-रूपण होता है। रूपक और अपह नुति
रूपक में प्रकृत वस्तु पर अप्रकृत का आरोप किया जाता है। अपह्न ति में प्रकृत का निषेध कर उसकी जगह अप्रकृत की स्थापना की जाती है। अन्य अर्थात् अप्रकृत वस्तु का आरोप या स्थापन दोनों अलङ्कारों में होता है।
१. परिणामालङ्कारस्तु रूपके एवान्तर्भवतीति दिक् ।
-काव्यप्रकाश, नागेश्वरी टीका, पृ० २४०