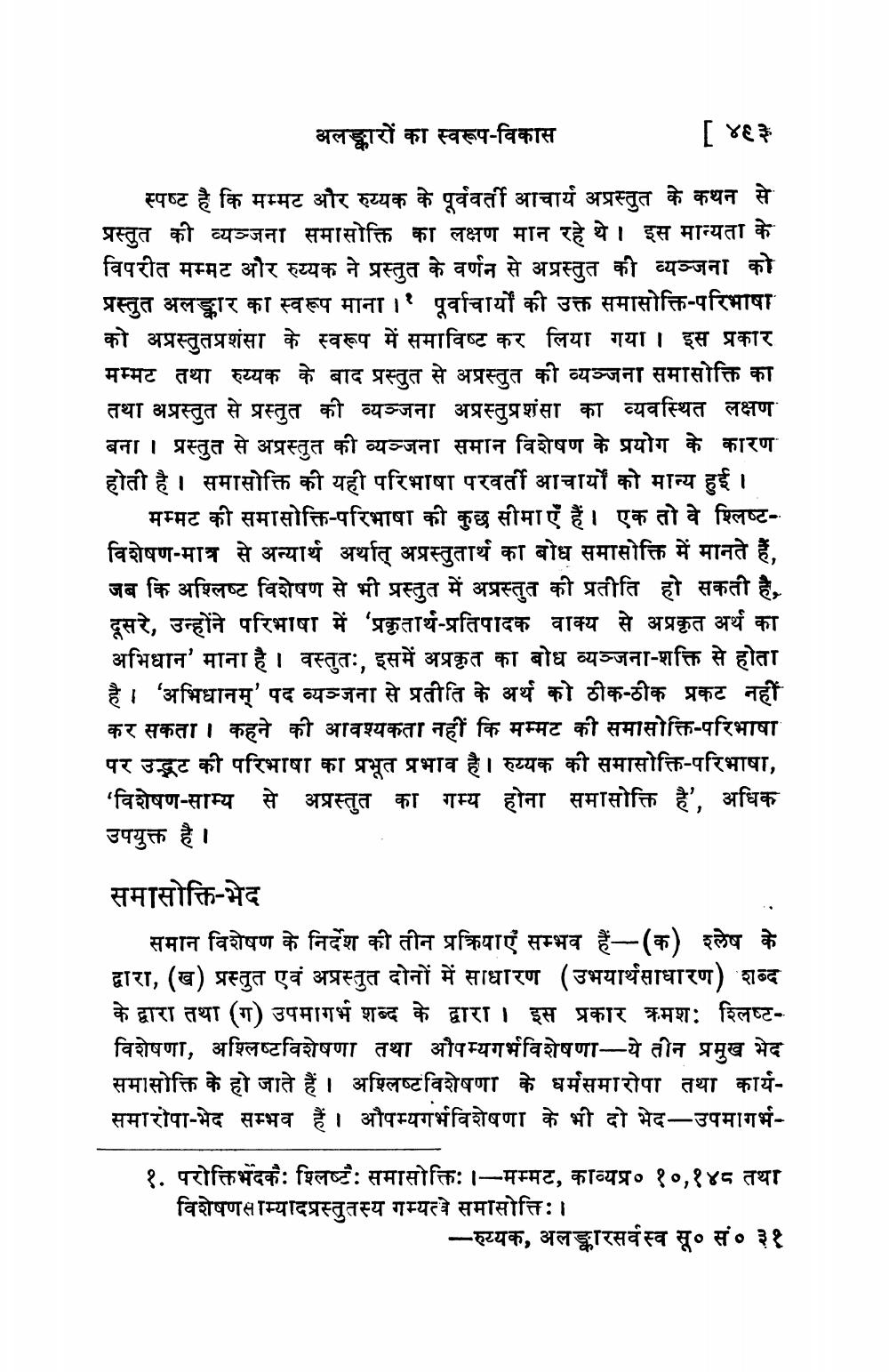________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[४६३
स्पष्ट है कि मम्मट और रुय्यक के पूर्ववर्ती आचार्य अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत की व्यञ्जना समासोक्ति का लक्षण मान रहे थे। इस मान्यता के विपरीत मम्मट और रुय्यक ने प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत की व्यञ्जना को प्रस्तुत अलङ्कार का स्वरूप माना।' पूर्वाचार्यों की उक्त समासोक्ति-परिभाषा को अप्रस्तुतप्रशंसा के स्वरूप में समाविष्ट कर लिया गया। इस प्रकार मम्मट तथा रुय्यक के बाद प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यञ्जना समासोक्ति का तथा अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यञ्जना अप्रस्तुप्रशंसा का व्यवस्थित लक्षण बना । प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यञ्जना समान विशेषण के प्रयोग के कारण होती है। समासोक्ति की यही परिभाषा परवर्ती आचार्यों को मान्य हुई।
मम्मट की समासोक्ति-परिभाषा की कुछ सीमाएँ हैं। एक तो वे श्लिष्टविशेषण-मात्र से अन्यार्थ अर्थात् अप्रस्तुतार्थ का बोध समासोक्ति में मानते हैं, जब कि अश्लिष्ट विशेषण से भी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की प्रतीति हो सकती है, दूसरे, उन्होंने परिभाषा में 'प्रकृतार्थ-प्रतिपादक वाक्य से अप्रकृत अर्थ का अभिधान' माना है। वस्तुतः, इसमें अप्रकृत का बोध व्यञ्जना-शक्ति से होता है। 'अभिधानम्' पद व्यञ्जना से प्रतीति के अर्थ को ठीक-ठीक प्रकट नहीं कर सकता। कहने की आवश्यकता नहीं कि मम्मट की समासोक्ति-परिभाषा पर उद्भट की परिभाषा का प्रभूत प्रभाव है। रुय्यक की समासोक्ति-परिभाषा, 'विशेषण-साम्य से अप्रस्तुत का गम्य होना समासोक्ति है', अधिक उपयुक्त है।
समासोक्ति-भेद
समान विशेषण के निर्देश की तीन प्रक्रियाएं सम्भव हैं-(क) श्लेष के द्वारा, (ख) प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों में साधारण (उभयार्थसाधारण) शब्द के द्वारा तथा (ग) उपमागर्भ शब्द के द्वारा। इस प्रकार क्रमश: श्लिष्टविशेषणा, अश्लिष्टविशेषणा तथा औपम्यगर्भविशेषणा-ये तीन प्रमुख भेद समासोक्ति के हो जाते हैं। अश्लिष्ट विशेषणा के धर्मसमारोपा तथा कार्यसमारोपा-भेद सम्भव हैं। औपम्यगर्भविशेषणा के भी दो भेद-उपमागर्भ
१. परोक्तिभदकैः श्लिष्टः समासोक्तिः।-मम्मट, काव्यप्र० १०,१४८ तथा विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोत्तिः।
-रुय्यक, अलङ्कारसर्वस्व सू० सं० ३१