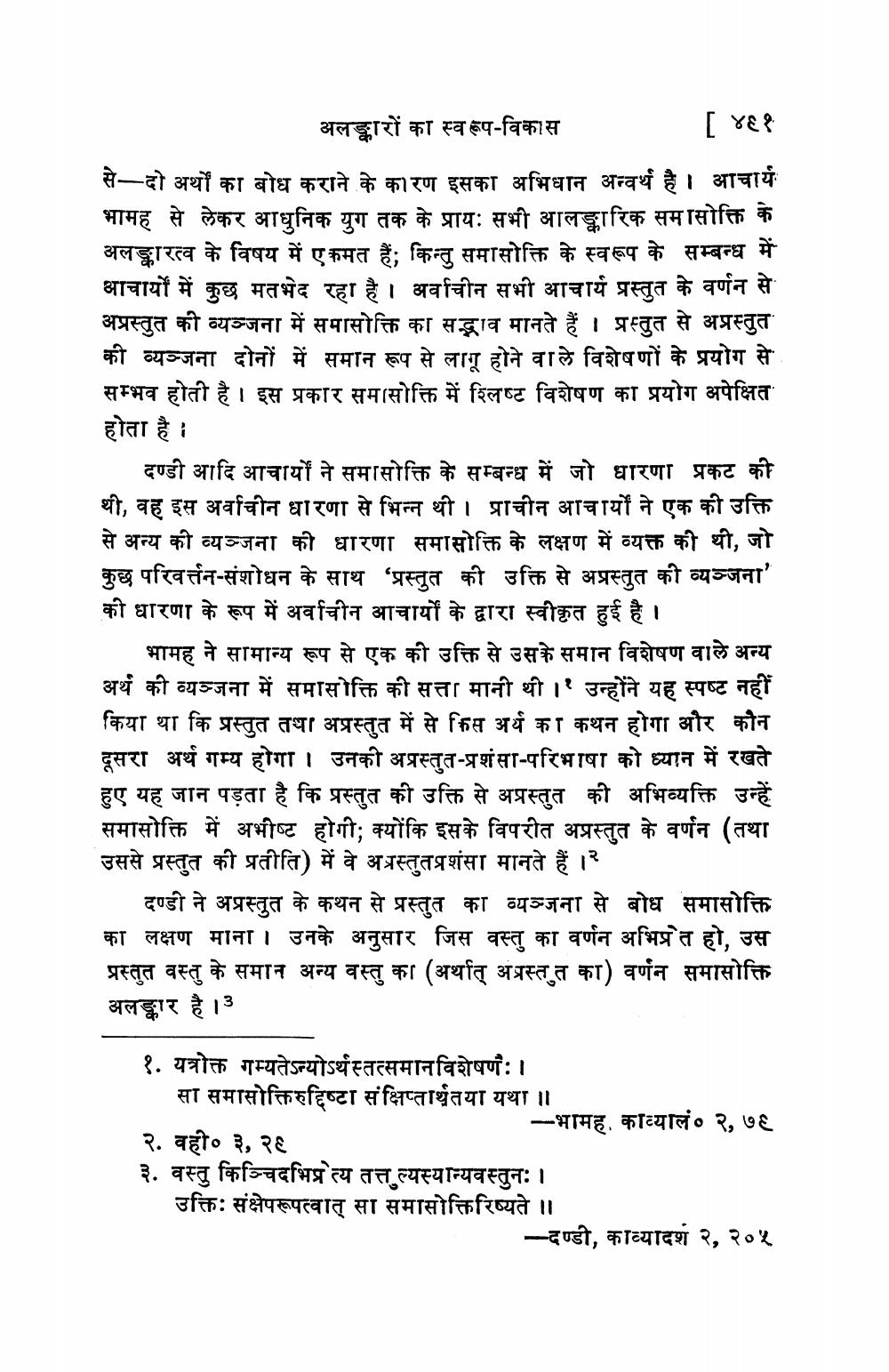________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४६१
से-दो अर्थों का बोध कराने के कारण इसका अभिधान अन्वर्थ है। आचार्य भामह से लेकर आधुनिक युग तक के प्रायः सभी आलङ्कारिक समासोक्ति के अलङ्कारत्व के विषय में एकमत हैं; किन्तु समासोक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्यों में कुछ मतभेद रहा है। अर्वाचीन सभी आचार्य प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत की व्यञ्जना में समासोक्ति का सद्भाव मानते हैं । प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यञ्जना दोनों में समान रूप से लागू होने वाले विशेषणों के प्रयोग से सम्भव होती है। इस प्रकार समासोक्ति में श्लिष्ट विशेषण का प्रयोग अपेक्षित होता है।
दण्डी आदि आचार्यों ने समासोक्ति के सम्बन्ध में जो धारणा प्रकट की थी, वह इस अर्वाचीन धारणा से भिन्न थी। प्राचीन आचार्यों ने एक की उक्ति से अन्य की व्यञ्जना की धारणा समासोक्ति के लक्षण में व्यक्त की थी, जो कुछ परिवर्तन-संशोधन के साथ 'प्रस्तुत की उक्ति से अप्रस्तुत की व्यञ्जना' की धारणा के रूप में अर्वाचीन आचार्यों के द्वारा स्वीकृत हुई है। __ भामह ने सामान्य रूप से एक की उक्ति से उसके समान विशेषण वाले अन्य अर्थ की व्यञ्जना में समासोक्ति की सत्ता मानी थी। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में से किस अर्थ का कथन होगा और कौन दूसरा अर्थ गम्य होगा। उनकी अप्रस्तुत-प्रशंसा-परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत की उक्ति से अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति उन्हें समासोक्ति में अभीष्ट होगी; क्योंकि इसके विपरीत अप्रस्तुत के वर्णन (तथा उससे प्रस्तुत की प्रतीति) में वे अप्रस्तुतप्रशंसा मानते हैं ।
दण्डी ने अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत का व्यञ्जना से बोध समासोक्ति का लक्षण माना। उनके अनुसार जिस वस्तु का वर्णन अभिप्रेत हो, उस प्रस्तुत वस्तु के समान अन्य वस्तु का (अर्थात् अप्रस्त त का) वर्णन समासोक्ति अलङ्कार है।
१. यत्रोक्त गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणः । ___ सा समासोक्तिरुद्दिष्टा संक्षिप्तार्थतया यथा ॥
-भामह. काव्यालं० २, ७६ २. वही० ३, २६ ३. वस्तु किञ्चिदभिप्रेत्य तत्त ल्यस्यान्यवस्तुनः। उक्तिः संक्षेपरूपत्वात् सा समासोक्तिरिष्यते ॥
-दण्डी, काव्यादर्श २, २०५