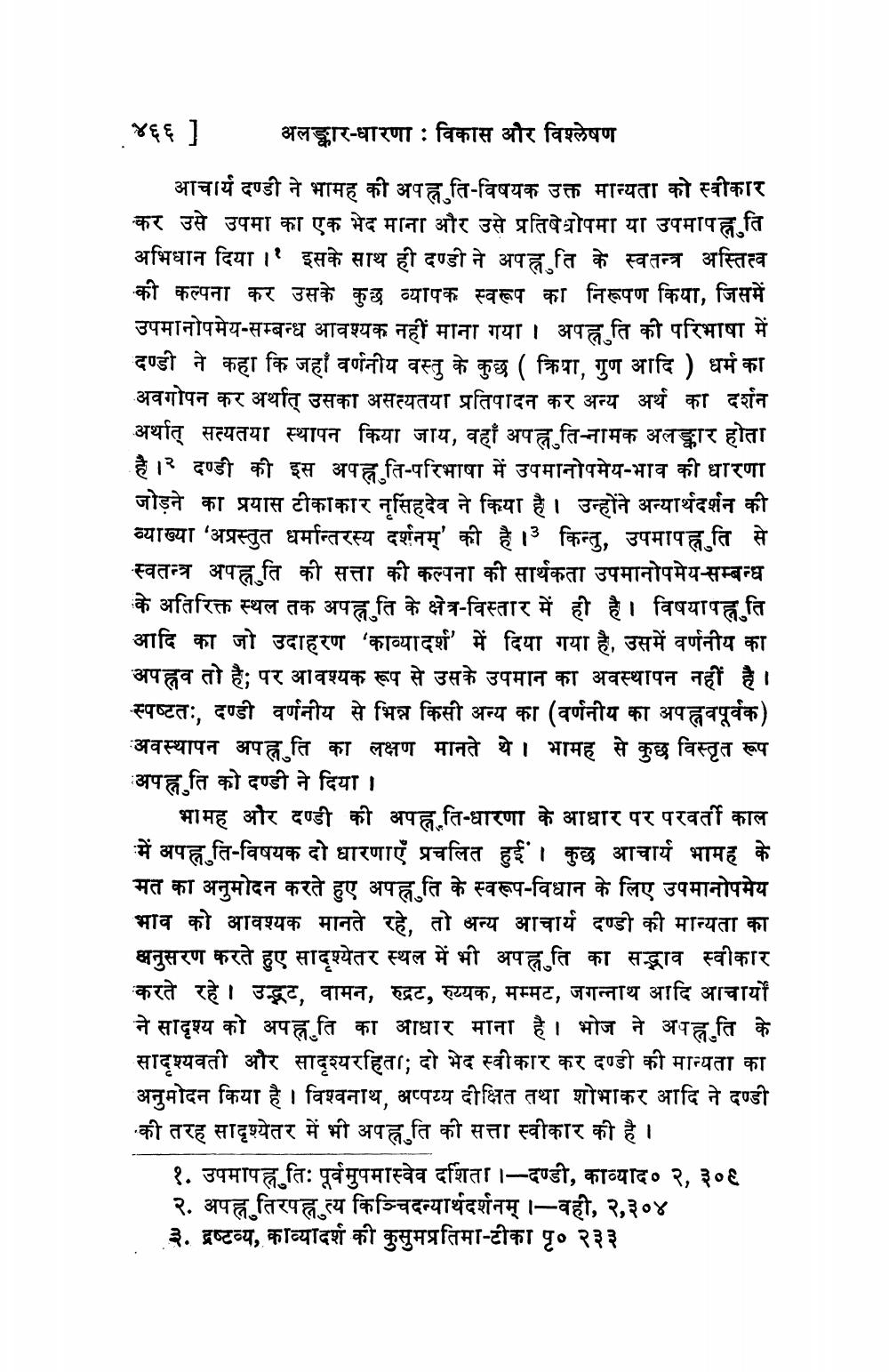________________
४६६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
आचार्य दण्डी ने भामह की अपह्नति-विषयक उक्त मान्यता को स्वीकार कर उसे उपमा का एक भेद माना और उसे प्रतिषेधोपमा या उपमापह्नति अभिधान दिया। इसके साथ ही दण्डी ने अपह्न ति के स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना कर उसके कुछ व्यापक स्वरूप का निरूपण किया, जिसमें उपमानोपमेय-सम्बन्ध आवश्यक नहीं माना गया। अपह्न ति की परिभाषा में दण्डी ने कहा कि जहाँ वर्णनीय वस्तु के कुछ ( क्रिया, गुण आदि ) धर्म का अवगोपन कर अर्थात् उसका असत्यतया प्रतिपादन कर अन्य अर्थ का दर्शन अर्थात् सत्यतया स्थापन किया जाय, वहाँ अपह्न ति-नामक अलङ्कार होता है ।२ दण्डी की इस अपह्न,ति-परिभाषा में उपमानोपमेय-भाव की धारणा जोड़ने का प्रयास टीकाकार नसिंहदेव ने किया है। उन्होंने अन्यार्थदर्शन की व्याख्या 'अप्रस्तुत धर्मान्तरस्य दर्शनम्' की है। किन्तु, उपमापह्न ति से स्वतन्त्र अपह्न ति की सत्ता की कल्पना की सार्थकता उपमानोपमेय-सम्बन्ध के अतिरिक्त स्थल तक अपह्नति के क्षेत्र-विस्तार में ही है। विषयापह्नति आदि का जो उदाहरण 'काव्यादर्श' में दिया गया है, उसमें वर्णनीय का अपह्नव तो है; पर आवश्यक रूप से उसके उपमान का अवस्थापन नहीं है। स्पष्टतः, दण्डी वर्णनीय से भिन्न किसी अन्य का (वर्णनीय का अपह्नवपूर्वक) अवस्थापन अपह्न ति का लक्षण मानते थे। भामह से कुछ विस्तृत रूप अपह्न ति को दण्डी ने दिया।
भामह और दण्डी की अपह्न.ति-धारणा के आधार पर परवर्ती काल में अपह्नति-विषयक दो धारणाएँ प्रचलित हुई। कुछ आचार्य भामह के मत का अनुमोदन करते हुए अपह्नति के स्वरूप-विधान के लिए उपमानोपमेय भाव को आवश्यक मानते रहे, तो अन्य आचार्य दण्डी की मान्यता का अनुसरण करते हुए सादृश्येतर स्थल में भी अपह्नति का सद्भाव स्वीकार करते रहे। उद्भट, वामन, रुद्रट, रुय्यक, मम्मट, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने सादृश्य को अपह्नति का आधार माना है। भोज ने अपह्नति के सादृश्यवती और सादृश्यरहिता; दो भेद स्वीकार कर दण्डी की मान्यता का अनुमोदन किया है । विश्वनाथ, अप्पय्य दीक्षित तथा शोभाकर आदि ने दण्डी की तरह सादृश्येतर में भी अपह्न ति की सत्ता स्वीकार की है ।
१. उपमापह्न तिः पूर्वमुपमास्वेव दर्शिता।-दण्डी, काव्याद० २, ३०६ २. अपह्न तिरपह्नत्य किञ्चिदन्यार्थदर्शनम् ।-वही, २,३०४ ३. द्रष्टव्य, काव्यादर्श की कुसुमप्रतिमा-टीका पृ० २३३