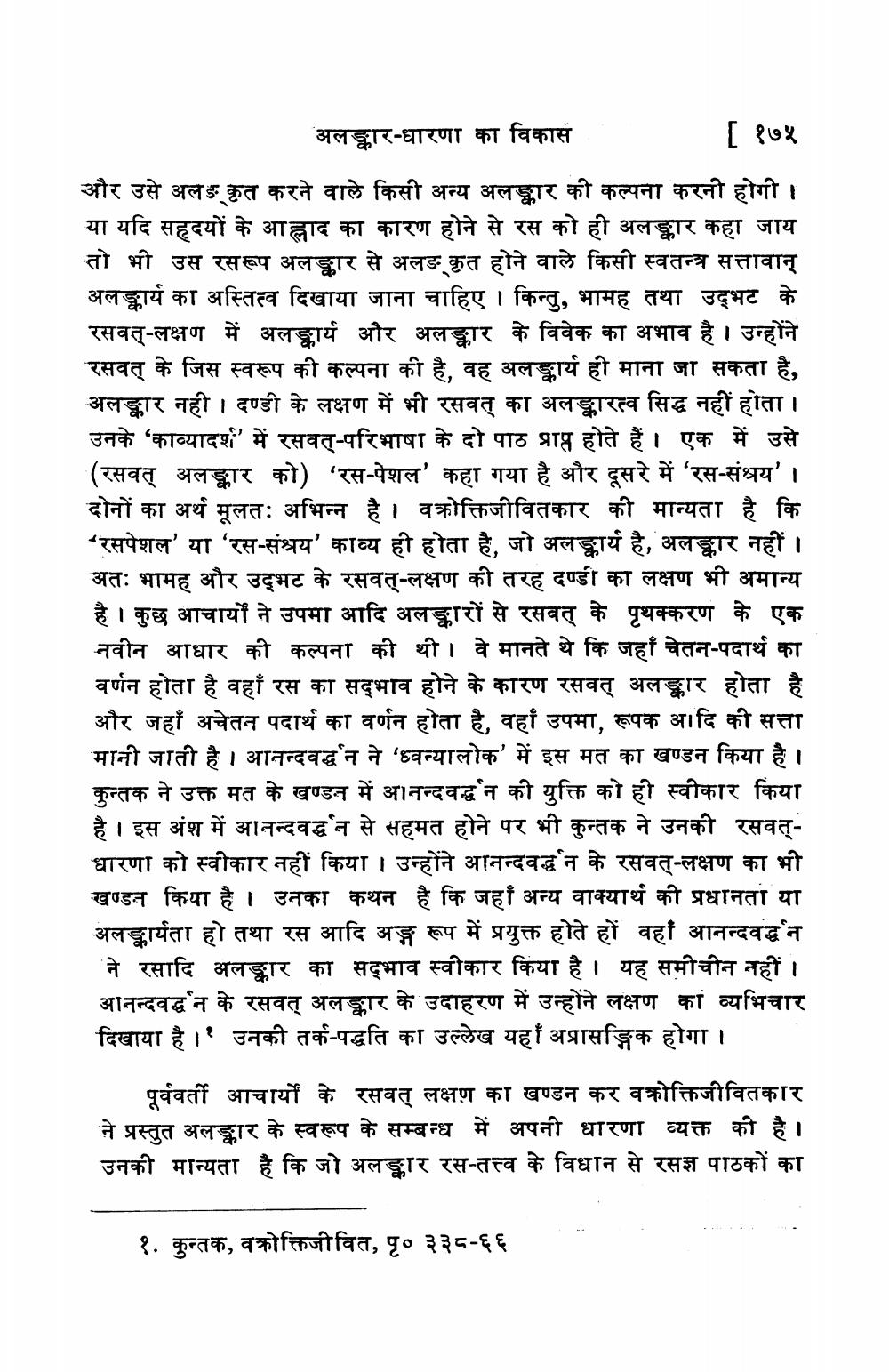________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १७५ और उसे अलंकृत करने वाले किसी अन्य अलङ्कार की कल्पना करनी होगी । या यदि सहृदयों के आह्लाद का कारण होने से रस को ही अलङ्कार कहा जाय तो भी उस रसरूप अलङ्कार से अलङ्कृत होने वाले किसी स्वतन्त्र सत्तावान् अलङ्कार्य का अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए । किन्तु, भामह तथा उद्भट के रसवत्-लक्षण में अलङ्कार्य और अलङ्कार के विवेक का अभाव है । उन्होंने रसवत् के जिस स्वरूप की कल्पना की है, वह अलङ्कार्य ही माना जा सकता है, अलङ्कार नही । दण्डी के लक्षण में भी रसवत् का अलङ्कारत्व सिद्ध नहीं होता । उनके ‘काव्यादर्श' में रसवत् - परिभाषा के दो पाठ प्राप्त होते हैं । एक में उसे ( रसवत् अलङ्कार को) 'रस-पेशल' कहा गया है और दूसरे में 'रस-संश्रय' । दोनों का अर्थ मूलतः अभिन्न है । वक्रोक्तिजीवितकार की मान्यता है कि ‘रसपेशल' या 'रस-संश्रय' काव्य ही होता है, जो अलङ्कार्य है, अलङ्कार नहीं । अतः भामह और उद्भट के रसवत्-लक्षण की तरह दण्डी का लक्षण भी अमान्य है । कुछ आचार्यों ने उपमा आदि अलङ्कारों से रसवत् के पृथक्करण के एक नवीन आधार की कल्पना की थी । वे मानते थे कि जहाँ चेतन पदार्थ का वर्णन होता है वहाँ रस का सद्भाव होने के कारण रसवत् अलङ्कार होता है और जहाँ अचेतन पदार्थ का वर्णन होता है, वहाँ उपमा, रूपक आदि की सत्ता मानी जाती है | आनन्दवर्द्धन ने 'ध्वन्यालोक' में इस मत का खण्डन किया है । कुन्तक ने उक्त मत के खण्डन में आनन्दवर्द्धन की युक्ति को ही स्वीकार किया है । इस अंश में आनन्दवर्द्धन से सहमत होने पर भी कुन्तक ने उनकी रसवत्धारणा को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने आनन्दवर्द्धन के रसवत्-लक्षण का भी खण्डन किया है | उनका कथन है कि जहाँ अन्य वाक्यार्थ की प्रधानता या अलङ्कार्यता हो तथा रस आदि अङ्ग रूप में प्रयुक्त होते हों वहाँ आनन्दवर्द्धन ने रसादि अलङ्कार का सद्भाव स्वीकार किया है । यह समीचीन नहीं । आनन्दवर्द्धन के रसवत् अलङ्कार के उदाहरण में उन्होंने लक्षण का व्यभिचार दिखाया है । उनकी तर्क-पद्धति का उल्लेख यहाँ अप्रासङ्गिक होगा ।
पूर्ववर्ती आचार्यों के रसवत् लक्षण का खण्डन कर वक्रोक्तिजीवितकार ने प्रस्तुत अलङ्कार के स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी धारणा व्यक्त की है । उनकी मान्यता है कि जो अलङ्कार रस तत्त्व के विधान से रसज्ञ पाठकों का
१. कुन्तक, वक्रोक्तिजीवित, पृ० ३३८- ६६