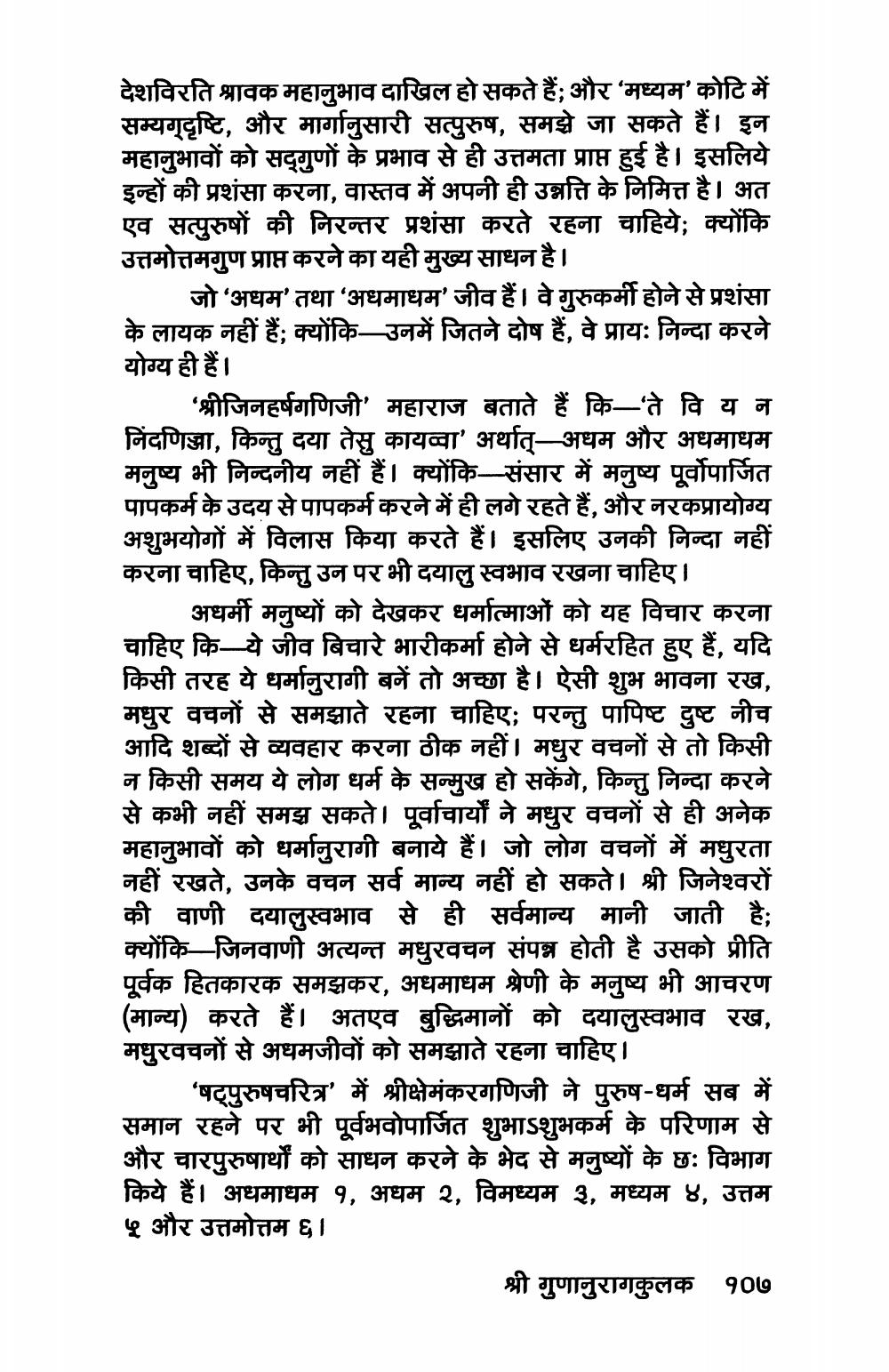________________
देशविरति श्रावक महानुभाव दाखिल हो सकते हैं;और 'मध्यम' कोटि में सम्यग्दृष्टि, और मार्गानुसारी सत्पुरुष, समझे जा सकते हैं। इन महानुभावों को सद्गुणों के प्रभाव से ही उत्तमता प्राप्त हुई है। इसलिये इन्हों की प्रशंसा करना, वास्तव में अपनी ही उन्नत्ति के निमित्त है। अत एव सत्पुरुषों की निरन्तर प्रशंसा करते रहना चाहिये; क्योंकि उत्तमोत्तमगुण प्राप्त करने का यही मुख्य साधन है।
जो 'अधम' तथा 'अधमाधम' जीव हैं। वे गुरुकर्मी होने से प्रशंसा के लायक नहीं हैं; क्योंकि उनमें जितने दोष हैं, वे प्रायः निन्दा करने योग्य ही हैं।
'श्रीजिनहर्षगणिजी' महाराज बताते हैं कि-'ते वि य न निंदणिज्जा, किन्तु दया तेसु कायव्वा' अर्थात्-अधम और अधमाधम मनुष्य भी निन्दनीय नहीं हैं। क्योंकि संसार में मनुष्य पूर्वोपार्जित पापकर्म के उदय से पापकर्म करने में ही लगे रहते हैं, और नरकप्रायोग्य अशुभयोगों में विलास किया करते हैं। इसलिए उनकी निन्दा नहीं करना चाहिए, किन्तु उन पर भी दयालु स्वभाव रखना चाहिए।
अधर्मी मनुष्यों को देखकर धर्मात्माओं को यह विचार करना चाहिए कि ये जीव बिचारे भारीकर्मा होने से धर्मरहित हुए हैं, यदि किसी तरह ये धर्मानुरागी बनें तो अच्छा है। ऐसी शुभ भावना रख, मधुर वचनों से समझाते रहना चाहिए; परन्तु पापिष्ट दुष्ट नीच आदि शब्दों से व्यवहार करना ठीक नहीं। मधुर वचनों से तो किसी न किसी समय ये लोग धर्म के सन्मुख हो सकेंगे, किन्तु निन्दा करने से कभी नहीं समझ सकते। पूर्वाचार्यों ने मधुर वचनों से ही अनेक महानुभावों को धर्मानुरागी बनाये हैं। जो लोग वचनों में मधुरता नहीं रखते, उनके वचन सर्व मान्य नहीं हो सकते। श्री जिनेश्वरों की वाणी दयालुस्वभाव से ही सर्वमान्य मानी जाती है; क्योंकि जिनवाणी अत्यन्त मधुरवचन संपन्न होती है उसको प्रीति पूर्वक हितकारक समझकर, अधमाधम श्रेणी के मनुष्य भी आचरण (मान्य) करते हैं। अतएव बुद्धिमानों को दयालुस्वभाव रख, मधुरवचनों से अधमजीवों को समझाते रहना चाहिए।
'षट्पुरुषचरित्र' में श्रीक्षेमंकरगणिजी ने पुरुष-धर्म सब में समान रहने पर भी पूर्वभवोपार्जित शुभाऽशुभकर्म के परिणाम से
और चारपुरुषार्थों को साधन करने के भेद से मनुष्यों के छः विभाग किये हैं। अधमाधम १, अधम २, विमध्यम ३, मध्यम ४, उत्तम ५और उत्तमोत्तम ६)
श्री गुणानुरागकुलक १०७