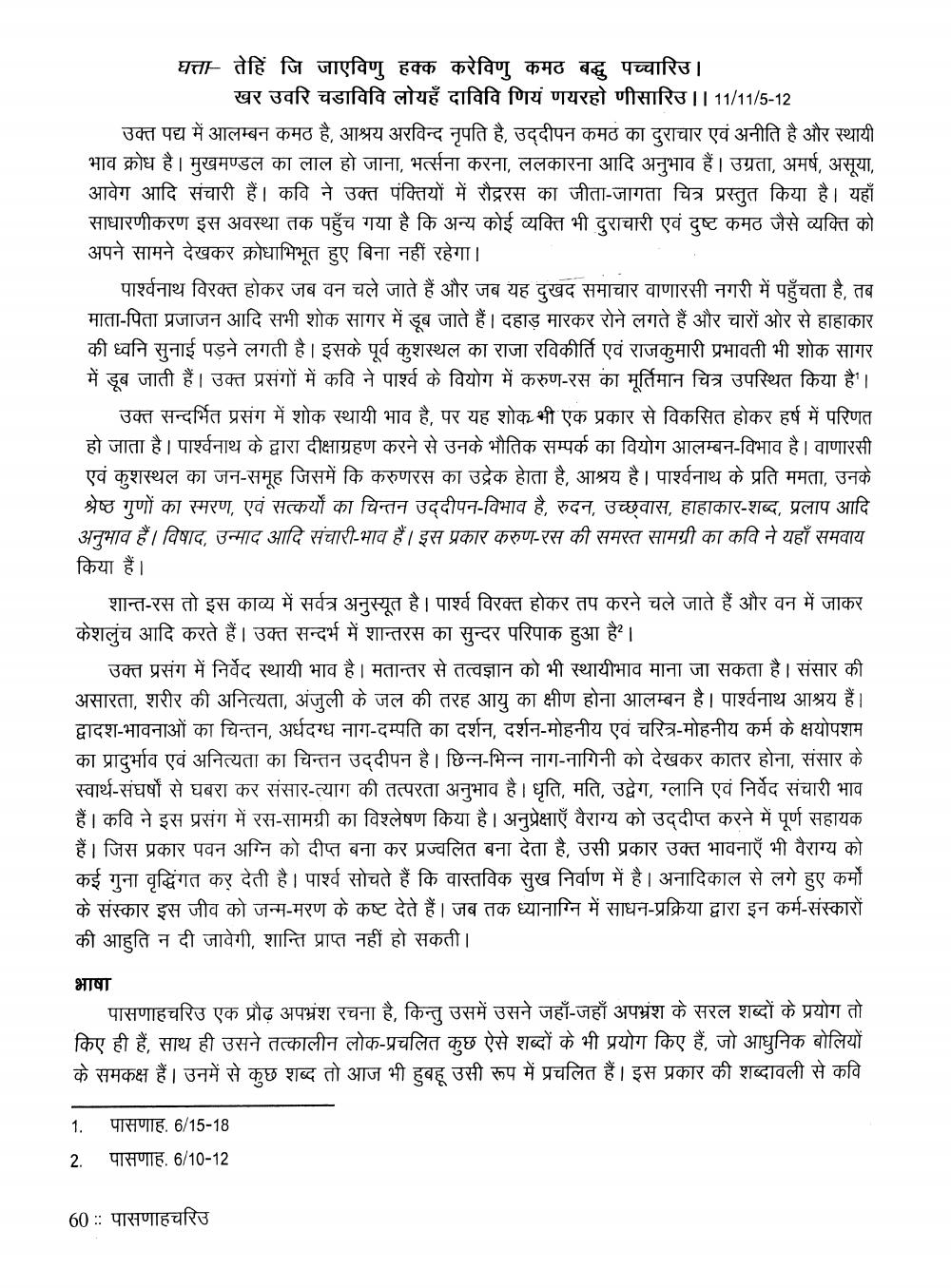________________
घत्ता- तेहिं जि जाएविण हक्क करेविणु कमठ बद्ध पच्चारिउ।
खर उवरि चडाविवि लोयहँ दाविवि णियं णयरहो णीसारिउ ।। 11/11/5-12 उक्त पद्य में आलम्बन कमठ है, आश्रय अरविन्द नृपति है, उद्दीपन कमठ का दुराचार एवं अनीति है और स्थायी भाव क्रोध है। मुखमण्डल का लाल हो जाना, भर्त्सना करना, ललकारना आदि अनुभाव हैं। उग्रता, अमर्ष, असूया, आवेग आदि संचारी हैं। कवि ने उक्त पंक्तियों में रौद्ररस का जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ साधारणीकरण इस अवस्था तक पहुंच गया है कि अन्य कोई व्यक्ति भी दुराचारी एवं दुष्ट कमठ जैसे व्यक्ति को अपने सामने देखकर क्रोधाभिभूत हुए बिना नहीं रहेगा।
पार्श्वनाथ विरक्त होकर जब वन चले जाते हैं और जब यह दुखद समाचार वाणारसी नगरी में पहुँचता है, तब माता-पिता प्रजाजन आदि सभी शोक सागर में डूब जाते हैं। दहाड़ मारकर रोने लगते हैं और चारों ओर से हाहाकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। इसके पूर्व कुशस्थल का राजा रविकीर्ति एवं राजकुमारी प्रभावती भी शोक सागर में डूब जाती हैं। उक्त प्रसंगों में कवि ने पार्श्व के वियोग में करुण-रस का मूर्तिमान चित्र उपस्थित किया है।
उक्त सन्दर्भित प्रसंग में शोक स्थायी भाव है, पर यह शोक भी एक प्रकार से विकसित होकर हर्ष में परिणत हो जाता है। पार्श्वनाथ के द्वारा दीक्षाग्रहण करने से उनके भौतिक सम्पर्क का वियोग आलम्बन-विभाव है। वाणारसी एवं कुशस्थल का जन-समूह जिसमें कि करुणरस का उद्रेक होता है, आश्रय है। पार्श्वनाथ के प्रति ममता, उनके
गों का स्मरण, एवं सत्कर्यों का चिन्तन उद्दीपन-विभाव है, रुदन, उच्छवास, हाहाकार-शब्द, प्रलाप आदि अनुभाव हैं। विषाद, उन्माद आदि संचारी-भाव हैं। इस प्रकार करुण-रस की समस्त सामग्री का कवि ने यहाँ समवाय किया हैं।
शान्त-रस तो इस काव्य में सर्वत्र अनुस्यूत है। पार्श्व विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं और वन में जाकर केशलुंच आदि करते हैं। उक्त सन्दर्भ में शान्तरस का सुन्दर परिपाक हुआ है।
उक्त प्रसंग में निर्वेद स्थायी भाव है। मतान्तर से तत्वज्ञान को भी स्थायीभाव माना जा सकता है। संसार की असारता, शरीर की अनित्यता, अंजुली के जल की तरह आयु का क्षीण होना आलम्बन है। पार्श्वनाथ आश्रय हैं। द्वादश-भावनाओं का चिन्तन, अर्धदग्ध नाग-दम्पति का दर्शन, दर्शन-मोहनीय एवं चरित्र-मोहनीय कर्म के क्षयोपशम का प्रादुर्भाव एवं अनित्यता का चिन्तन उद्दीपन है। छिन्न-भिन्न नाग-नागिनी को देखकर कातर होना, संसार के स्वार्थ-संघर्षों से घबरा कर संसार-त्याग की तत्परता अनुभाव है। धृति, मति, उद्वेग, ग्लानि एवं निर्वेद संचारी भाव हैं। कवि ने इस प्रसंग में रस-सामग्री का विश्लेषण किया है। अनुप्रेक्षाएँ वैराग्य को उद्दीप्त करने में पूर्ण सहायक हैं। जिस प्रकार पवन अग्नि को दीप्त बना कर प्रज्वलित बना देता है, उसी प्रकार उक्त भावनाएँ भी वैराग्य को कई गुना वृद्धिंगत कर देती है। पार्श्व सोचते हैं कि वास्तविक सुख निर्वाण में है। अनादिकाल से लगे हुए कर्मों के संस्कार इस जीव को जन्म-मरण के कष्ट देते हैं। जब तक ध्यानाग्नि में साधन-प्रक्रिया द्वारा इन कर्म-संस्कारों की आहुति न दी जावेगी, शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
भाषा
पासणाहचरिउ एक प्रौढ़ अपभ्रंश रचना है, किन्तु उसमें उसने जहाँ-जहाँ अपभ्रंश के सरल शब्दों के प्रयोग तो किए ही हैं, साथ ही उसने तत्कालीन लोक-प्रचलित कुछ ऐसे शब्दों के भी प्रयोग किए हैं, जो आधुनिक बोलियों के समकक्ष हैं। उनमें से कुछ शब्द तो आज भी हुबहू उसी रूप में प्रचलित हैं। इस प्रकार की शब्दावली से कवि
1. 2.
पासणाह. 6/15-18 पासणाह. 6/10-12
60 :: पासणाहचरिउ