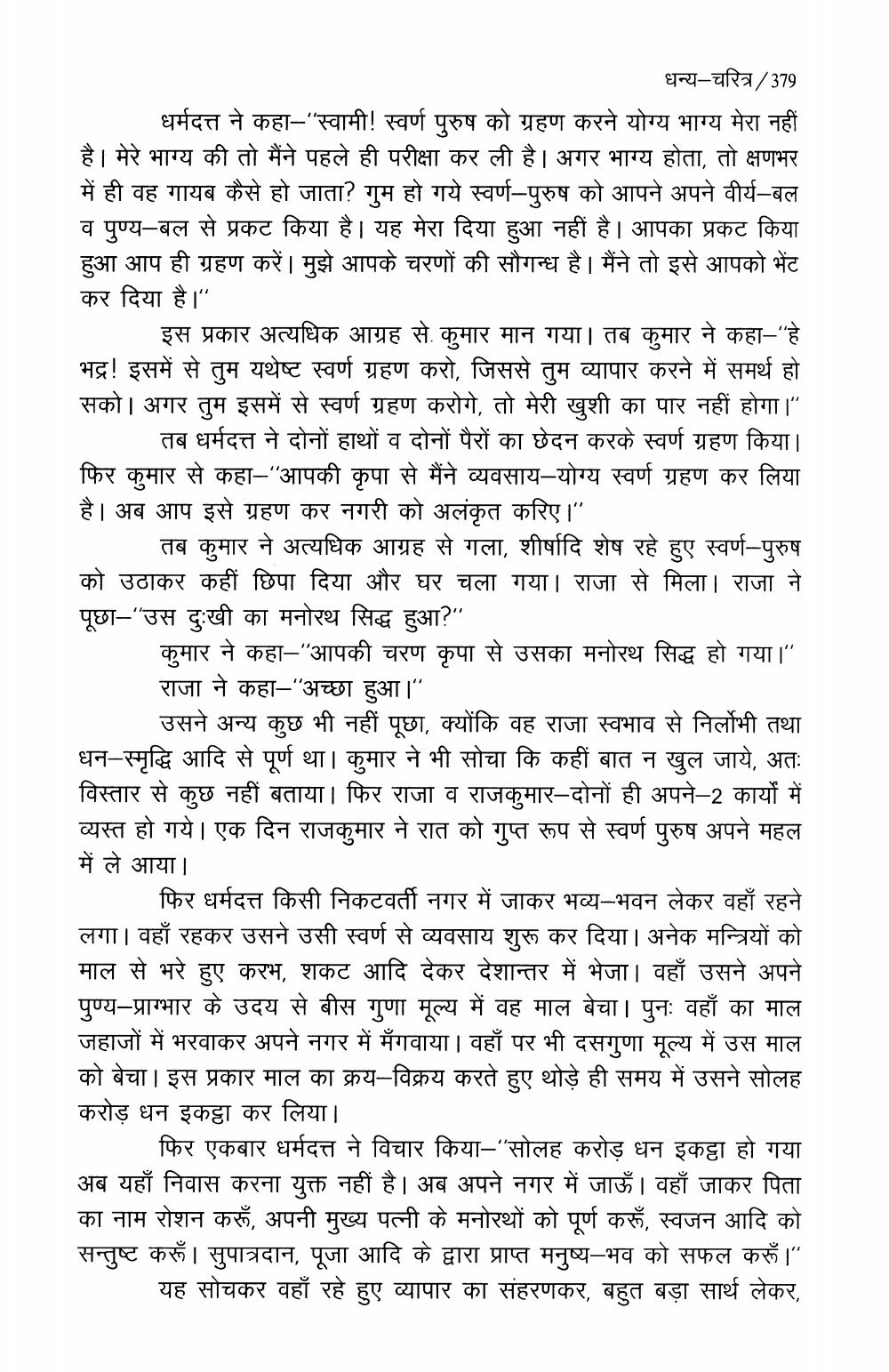________________
धन्य - चरित्र / 379
धर्मदत्त ने कहा—“स्वामी! स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने योग्य भाग्य मेरा नहीं है। मेरे भाग्य की तो मैंने पहले ही परीक्षा कर ली है। अगर भाग्य होता, तो क्षणभर में ही वह गायब कैसे हो जाता? गुम हो गये स्वर्ण - पुरुष को आपने अपने वीर्य-बल व पुण्य-बल से प्रकट किया है। यह मेरा दिया हुआ नहीं है । आपका प्रकट किया हुआ आप ही ग्रहण करें। मुझे आपके चरणों की सौगन्ध है । मैंने तो इसे आपको भेंट कर दिया है। "
इस प्रकार अत्यधिक आग्रह से कुमार मान गया। तब कुमार ने कहा- "हे भद्र! इसमें से तुम यथेष्ट स्वर्ण ग्रहण करो, जिससे तुम व्यापार करने में समर्थ हो सको। अगर तुम इसमें से स्वर्ण ग्रहण करोगे, तो मेरी खुशी का पार नहीं होगा ।" तब धर्मदत्त ने दोनों हाथों व दोनों पैरों का छेदन करके स्वर्ण ग्रहण किया। फिर कुमार से कहा - " आपकी कृपा से मैंने व्यवसाय - योग्य स्वर्ण ग्रहण कर लिया है। अब आप इसे ग्रहण कर नगरी को अलंकृत करिए । "
तब कुमार ने अत्यधिक आग्रह से गला, शीर्षादि शेष रहे हुए स्वर्ण - पुरुष को उठाकर कहीं छिपा दिया और घर चला गया। राजा से मिला। राजा ने पूछा - "उस दुःखी का मनोरथ सिद्ध हुआ ?”
कुमार ने कहा - " आपकी चरण कृपा से उसका मनोरथ सिद्ध हो गया ।" राजा ने कहा- "अच्छा हुआ ।"
उसने अन्य कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वह राजा स्वभाव से निर्लोभी तथा धन-समृद्धि आदि से पूर्ण था । कुमार ने भी सोचा कि कहीं बात न खुल जाये, अतः विस्तार से कुछ नहीं बताया। फिर राजा व राजकुमार - दोनों ही अपने -2 कार्यों में व्यस्त हो गये। एक दिन राजकुमार ने रात को गुप्त रूप से स्वर्ण पुरुष अपने महल में ले आया ।
फिर धर्मदत्त किसी निकटवर्ती नगर में जाकर भव्य भवन लेकर वहाँ रहने लगा। वहाँ रहकर उसने उसी स्वर्ण से व्यवसाय शुरू कर दिया। अनेक मन्त्रियों को माल से भरे हुए करभ, शकट आदि देकर देशान्तर में भेजा । वहाँ उसने अपने पुण्य-प्राग्भार के उदय से बीस गुणा मूल्य में वह माल बेचा। पुनः वहाँ का माल जहाजों में भरवाकर अपने नगर में मँगवाया । वहाँ पर भी दसगुणा मूल्य में उस माल को बेचा। इस प्रकार माल का क्रय-विक्रय करते हुए थोड़े ही समय में उसने सोलह करोड़ धन इकट्ठा कर लिया ।
फिर एकबार धर्मदत्त ने विचार किया - "सोलह करोड़ धन इकट्ठा हो गया अब यहाँ निवास करना युक्त नहीं है। अब अपने नगर में जाऊँ। वहाँ जाकर पिता का नाम रोशन करूँ, अपनी मुख्य पत्नी के मनोरथों को पूर्ण करूँ, स्वजन आदि को सन्तुष्ट करूँ। सुपात्रदान, पूजा आदि के द्वारा प्राप्त मनुष्य-भव को सफल करूँ ।" यह सोचकर वहाँ रहे हुए व्यापार का संहरणकर, बहुत बड़ा सार्थ लेकर,