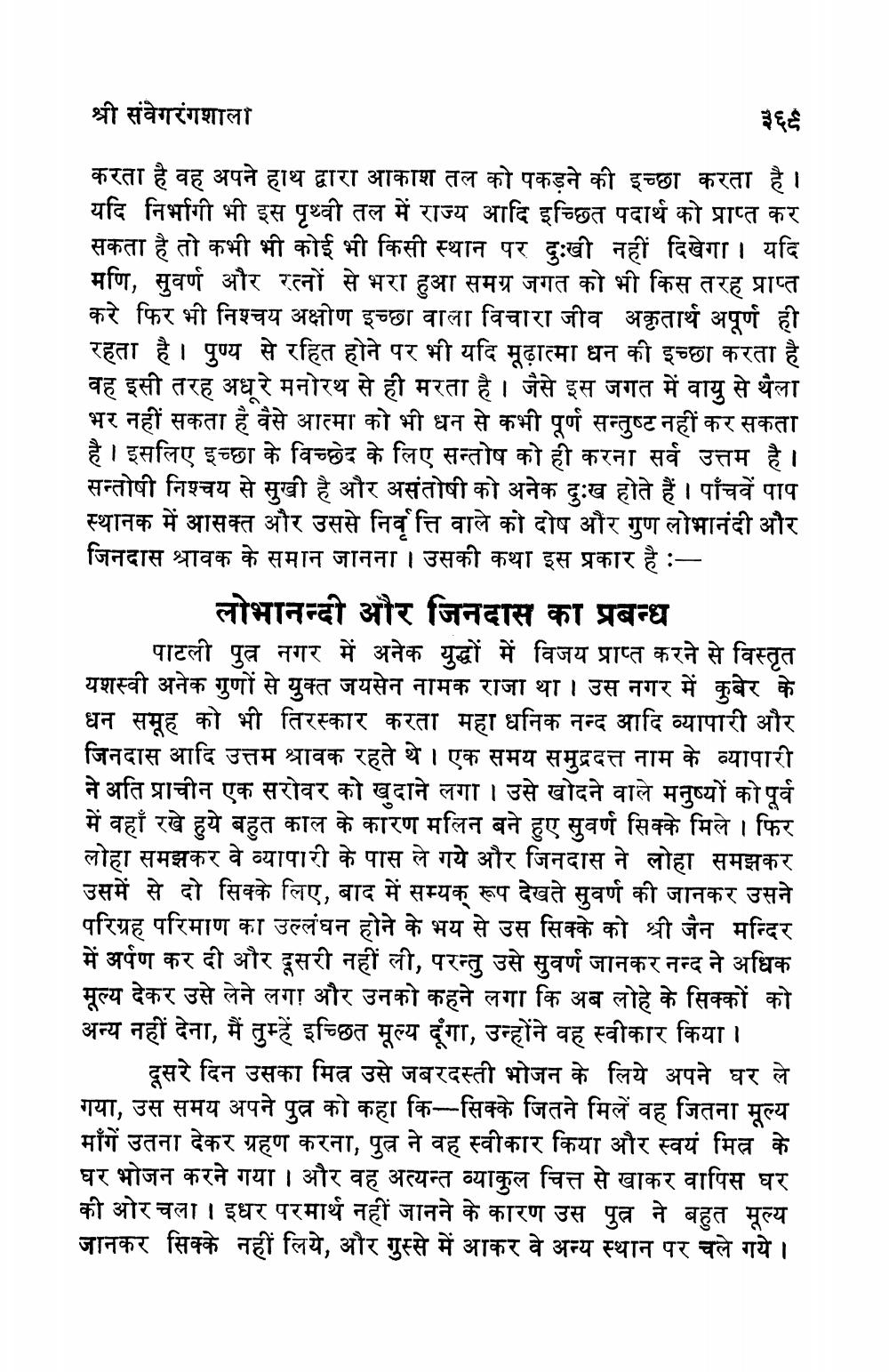________________
श्री संवेगरंगशाला
३६६
करता है वह अपने हाथ द्वारा आकाश तल को पकड़ने की इच्छा करता है । यदि निर्भागी भी इस पृथ्वी तल में राज्य आदि इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकता है तो कभी भी कोई भी किसी स्थान पर दुःखी नहीं दिखेगा । यदि मणि, सुवर्ण और रत्नों से भरा हुआ समग्र जगत को भी किस तरह प्राप्त करे फिर भी निश्चय अक्षीण इच्छा वाला विचारा जीव अकृतार्थ अपूर्ण ही रहता है । पुण्य से रहित होने पर भी यदि मूढात्मा धन की इच्छा करता है वह इसी तरह अधूरे मनोरथ से ही मरता है । जैसे इस जगत में वायु से थैला भर नहीं सकता है वैसे आत्मा को भी धन से कभी पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकता है । इसलिए इच्छा के विच्छेद के लिए सन्तोष को ही करना सर्व उत्तम है । सन्तोषी निश्चय से सुखी है और असंतोषी को अनेक दुःख होते हैं । पाँचवें पाप स्थानक में आसक्त और उससे निर्वृत्ति वाले को दोष और गुण लोभानंदी और जिनदास श्रावक के समान जानना । उसकी कथा इस प्रकार है :
लोभानन्दी और जिनदास का प्रबन्ध
पाटली पुत्र नगर में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने से विस्तृत यशस्वी अनेक गुणों से युक्त जयसेन नामक राजा था । उस नगर में कुबेर के धन समूह को भी तिरस्कार करता महा धनिक नन्द आदि व्यापारी और जिनदास आदि उत्तम श्रावक रहते थे । एक समय समुद्रदत्त नाम के व्यापारी
1
अति प्राचीन एक सरोवर को खुदाने लगा । उसे खोदने वाले मनुष्यों को पूर्व में वहाँ रखे हुये बहुत काल के कारण मलिन बने हुए सुवर्ण सिक्के मिले । फिर लोहा समझकर वे व्यापारी के पास ले गये और जिनदास ने लोहा समझकर उसमें से दो सिक्के लिए, बाद में सम्यक् रूप देखते सुवर्ण की जानकर उसने परिग्रह परिमाण का उल्लंघन होने के भय से उस सिक्के को श्री जैन मन्दिर में अर्पण कर दी और दूसरी नहीं ली, परन्तु उसे सुवर्णं जानकर नन्द ने अधिक मूल्य देकर उसे लेने लगा और उनको कहने लगा कि अब लोहे के सिक्कों को अन्य नहीं देना, मैं तुम्हें इच्छित मूल्य दूंगा, उन्होंने वह स्वीकार किया ।
दूसरे दिन उसका मित्र उसे जबरदस्ती भोजन के लिये अपने घर ले गया, उस समय अपने पुत्र को कहा कि - सिक्के जितने मिलें वह जितना मूल्य माँगें उतना देकर ग्रहण करना, पुत्र ने वह स्वीकार किया और स्वयं मित्र के घर भोजन करने गया । और वह अत्यन्त व्याकुल चित्त से खाकर वापिस घर की ओर चला । इधर परमार्थ नहीं जानने के कारण उस पुत्र ने बहुत मूल्य जानकर सिक्के नहीं लिये, और गुस्से में आकर वे अन्य स्थान पर चले गये ।