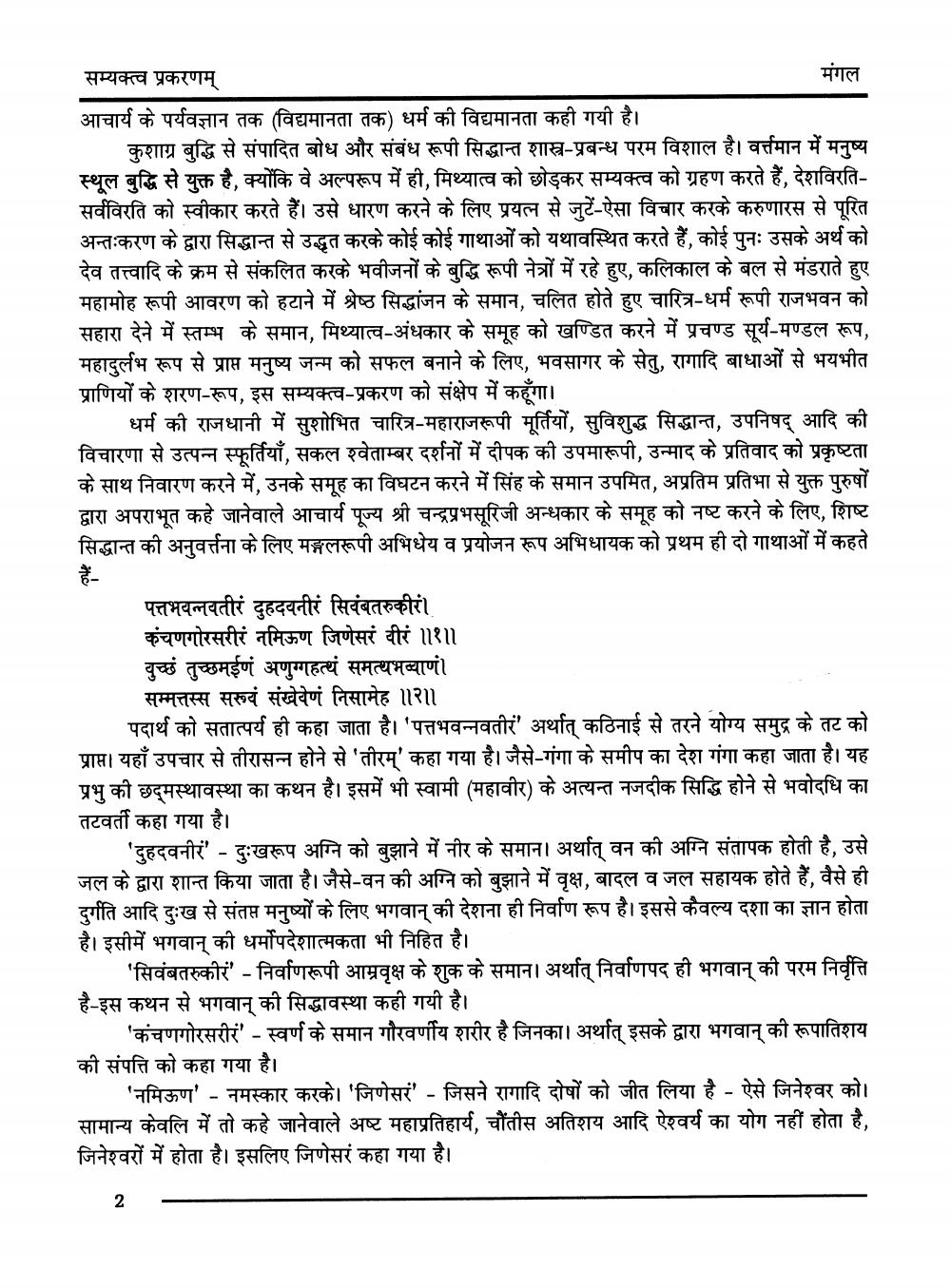________________
सम्यक्त्व प्रकरणम्
मंगल
आचार्य के पर्यवज्ञान तक (विद्यमानता तक) धर्म की विद्यमानता कही गयी है।
___ कुशाग्र बुद्धि से संपादित बोध और संबंध रूपी सिद्धान्त शास्त्र-प्रबन्ध परम विशाल है। वर्तमान में मनुष्य स्थूल बुद्धि से युक्त है, क्योंकि वे अल्परूप में ही, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं, देशविरतिसर्वविरति को स्वीकार करते हैं। उसे धारण करने के लिए प्रयत्न से जुटें-ऐसा विचार करके करुणारस से पूरित अन्तःकरण के द्वारा सिद्धान्त से उद्धृत करके कोई कोई गाथाओं को यथावस्थित करते हैं, कोई पुनः उसके अर्थ को देव तत्त्वादि के क्रम से संकलित करके भवीजनों के बुद्धि रूपी नेत्रों में रहे हुए, कलिकाल के बल से मंडराते हुए महामोह रूपी आवरण को हटाने में श्रेष्ठ सिद्धांजन के समान, चलित होते हुए चारित्र-धर्म रूपी राजभवन को सहारा देने में स्तम्भ के समान, मिथ्यात्व-अंधकार के समूह को खण्डित करने में प्रचण्ड सूर्य-मण्डल रूप, महादुर्लभ रूप से प्राप्त मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए, भवसागर के सेतु, रागादि बाधाओं से भयभीत प्राणियों के शरण-रूप, इस सम्यक्त्व-प्रकरण को संक्षेप में कहूँगा।
धर्म की राजधानी में सुशोभित चारित्र-महाराजरूपी मूर्तियों, सुविशुद्ध सिद्धान्त, उपनिषद् आदि की विचारणा से उत्पन्न स्फूर्तियाँ, सकल श्वेताम्बर दर्शनों में दीपक की उपमारूपी, उन्माद के प्रतिवाद को प्रकृष्टता के साथ निवारण करने में, उनके समूह का विघटन करने में सिंह के समान उपमित, अप्रतिम प्रतिभा से युक्त पुरुषों द्वारा अपराभूत कहे जानेवाले आचार्य पूज्य श्री चन्द्रप्रभसूरिजी अन्धकार के समूह को नष्ट करने के लिए, शिष्ट सिद्धान्त की अनुवर्त्तना के लिए मङ्गलरूपी अभिधेय व प्रयोजन रूप अभिधायक को प्रथम ही दो गाथाओं में कहते
पत्तभवन्नवतीरं दुहदयनीरं सिवंबतरुकी। कंचणगोरसरीरं नमिऊण जिणेसरं वीरं ॥१॥ युच्छं तुच्छमईणं अणुग्गहत्थं समत्थभव्याणं।
सम्मत्तस्स सरुवं संखेवेणं निसामेह ॥२॥
पदार्थ को सतात्पर्य ही कहा जाता है। 'पत्तभवन्नवतीरं' अर्थात् कठिनाई से तरने योग्य समुद्र के तट को प्राप्त। यहाँ उपचार से तीरासन्न होने से 'तीरम्' कहा गया है। जैसे-गंगा के समीप का देश गंगा कहा जाता है। यह प्रभु की छद्मस्थावस्था का कथन है। इसमें भी स्वामी (महावीर) के अत्यन्त नजदीक सिद्धि होने से भवोदधि का तटवर्ती कहा गया है।
'दुहदवनीरं' - दुःखरूप अग्नि को बुझाने में नीर के समान। अर्थात् वन की अग्नि संतापक होती है, उसे जल के द्वारा शान्त किया जाता है। जैसे-वन की अग्नि को बुझाने में वृक्ष, बादल व जल सहायक होते हैं, वैसे ही दुर्गति आदि दुःख से संतप्त मनुष्यों के लिए भगवान् की देशना ही निर्वाण रूप है। इससे कैवल्य दशा का ज्ञान होता है। इसीमें भगवान् की धर्मोपदेशात्मकता भी निहित है। _ सिवंबतरुकीरं' - निर्वाणरूपी आम्रवृक्ष के शुक के समान। अर्थात् निर्वाणपद ही भगवान् की परम निर्वृत्ति है-इस कथन से भगवान् की सिद्धावस्था कही गयी है।
'कंचणगोरसरीरं' - स्वर्ण के समान गौरवर्णीय शरीर है जिनका। अर्थात् इसके द्वारा भगवान् की रूपातिशय की संपत्ति को कहा गया है।
'नमिऊण' - नमस्कार करके। 'जिणेसरं' - जिसने रागादि दोषों को जीत लिया है - ऐसे जिनेश्वर को। सामान्य केवलि में तो कहे जानेवाले अष्ट महाप्रतिहार्य, चौंतीस अतिशय आदि ऐश्वर्य का योग नहीं होता है, जिनेश्वरों में होता है। इसलिए जिणेसरं कहा गया है।