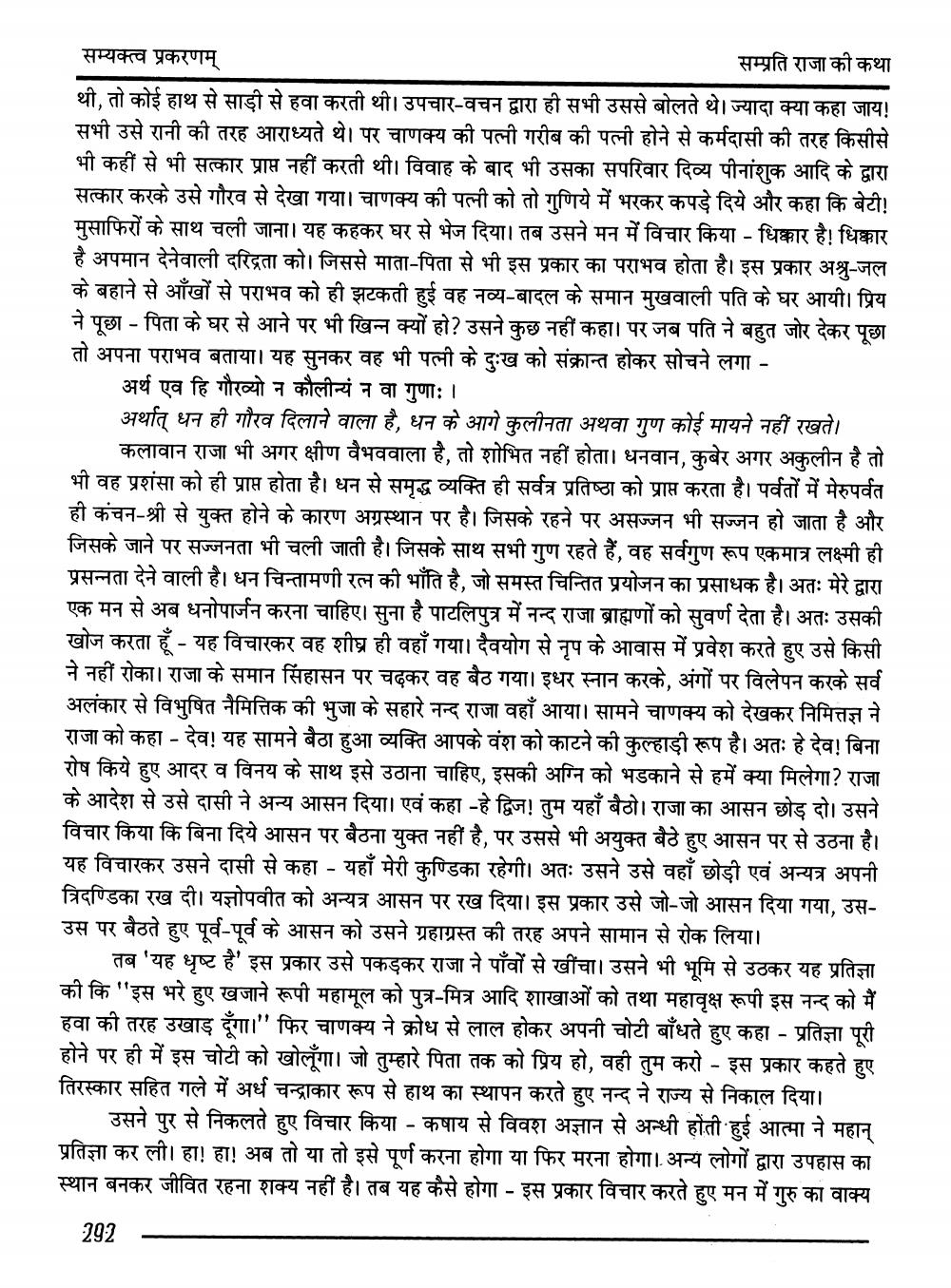________________
सम्यक्त्व प्रकरणम्
सम्प्रति राजा की कथा
थी, तो कोई हाथ से साड़ी से हवा करती थी । उपचार - वचन द्वारा ही सभी उससे बोलते थे। ज्यादा क्या कहा जाय ! सभी उसे रानी की तरह आराध्यते थे। पर चाणक्य की पत्नी गरीब की पत्नी होने से कर्मदासी की तरह किसीसे भी कहीं से भी सत्कार प्राप्त नहीं करती थी । विवाह के बाद भी उसका सपरिवार दिव्य पीनांशुक आदि के द्वारा सत्कार करके उसे गौरव से देखा गया । चाणक्य की पत्नी को तो गुणिये में भरकर कपड़े दिये और कहा कि बेटी ! मुसाफिरों के साथ चली जाना। यह कहकर घर से भेज दिया। तब उसने मन में विचार किया - धिक्कार है! धिक्कार है अपमान देनेवाली दरिद्रता को । जिससे माता-पिता से भी इस प्रकार का पराभव होता है। इस प्रकार अश्रु-जल के बहाने से आँखों से पराभव को ही झटकती हुई वह नव्य- बादल के समान मुखवाली पति के घर आयी । प्रिय ने पूछा - पिता के घर से आने पर भी खिन्न क्यों हो? उसने कुछ नहीं कहा। पर जब पति ने बहुत जोर देकर पूछा तो अपना पराभव बताया । यह सुनकर वह भी पत्नी के दुःख को संक्रान्त होकर सोचने लगा -
अर्थ एव हि गौरव्यो न कौलीन्यं न वा गुणाः ।
अर्थात् धन ही गौरव दिलाने वाला है, धन के आगे कुलीनता अथवा गुण कोई मायने नहीं रखते।
कलावान राजा भी अगर क्षीण वैभववाला है, तो शोभित नहीं होता । धनवान, कुबेर अगर अकुलीन है तो भी वह प्रशंसा को ही प्राप्त होता है। धन से समृद्ध व्यक्ति ही सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है । पर्वतों में मेरुपर्वत ही कंचन - श्री से युक्त होने के कारण अग्रस्थान पर है। जिसके रहने पर असज्जन भी सज्जन हो जाता है और जिसके जाने पर सज्जनता भी चली जाती है। जिसके साथ सभी गुण रहते हैं, वह सर्वगुण रूप एकमात्र लक्ष्मी ही प्रसन्नता देने वाली है। धन चिन्तामणी रत्न की भाँति है, जो समस्त चिन्तित प्रयोजन का प्रसाधक है। अतः मेरे द्वारा एक मन से अब धनोपार्जन करना चाहिए। सुना है पाटलिपुत्र में नन्द राजा ब्राह्मणों को सुवर्ण देता है। अतः उसकी खोज करता हूँ - यह विचारकर वह शीघ्र ही वहाँ गया। दैवयोग से नृप के आवास में प्रवेश करते हुए उसे किसी ने नहीं रोका। राजा के समान सिंहासन पर चढ़कर वह बैठ गया। इधर स्नान करके, अंगों पर विलेपन करके सर्व अलंकार से विभुषित नैमित्तिक की भुजा के सहारे नन्द राजा वहाँ आया। सामने चाणक्य को देखकर निमित्तज्ञ ने राजा को कहा - देव! यह सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपके वंश को काटने की कुल्हाड़ी रूप है। अतः हे देव! बिना रोष किये हुए आदर व विनय के साथ इसे उठाना चाहिए, इसकी अग्नि को भडकाने से हमें क्या मिलेगा? राजा के आदेश से उसे दासी ने अन्य आसन दिया। एवं कहा - हे द्विज ! तुम यहाँ बैठो। राजा का आसन छोड़ दो। उसने विचार किया कि बिना दिये आसन पर बैठना युक्त नहीं है, पर उससे भी अयुक्त बैठे हुए आसन पर से उठना है। यह विचारकर उसने दासी से कहा- यहाँ मेरी कुण्डिका रहेगी। अतः उसने उसे वहाँ छोड़ी एवं अन्यत्र अपनी त्रिदण्डिका रख दी। यज्ञोपवीत को अन्यत्र आसन पर रख दिया। इस प्रकार उसे जो-जो आसन दिया गया, उसउस पर बैठते हुए पूर्व-पूर्व के आसन को उसने ग्रहाग्रस्त की तरह अपने सामान से रोक लिया ।
तब 'यह धृष्ट है' इस प्रकार उसे पकड़कर राजा ने पाँवों से खींचा। उसने भी भूमि से उठकर यह प्रतिज्ञा की कि "इस भरे हुए खजाने रूपी महामूल को पुत्र - मित्र आदि शाखाओं को तथा महावृक्ष रूपी इस नन्द को मैं हवा की तरह उखाड़ दूँगा।" फिर चाणक्य ने क्रोध से लाल होकर अपनी चोटी बाँधते हुए कहा - प्रतिज्ञा पूरी होने पर ही में इस चोटी को खोलूँगा । जो तुम्हारे पिता तक को प्रिय हो, वही तुम करो इस प्रकार कहते हुए तिरस्कार सहित गले में अर्ध चन्द्राकार रूप से हाथ का स्थापन करते हुए नन्द ने राज्य से निकाल दिया।
उसने पुर से निकलते हुए विचार किया - कषाय से विवश अज्ञान से अन्धी होती हुई आत्मा ने महान् प्रतिज्ञा कर ली। हा! हा! अब तो या तो इसे पूर्ण करना होगा या फिर मरना होगा। अन्य लोगों द्वारा उपहास का स्थान बनकर जीवित रहना शक्य नहीं है। तब यह कैसे होगा - इस प्रकार विचार करते हुए मन में गुरु का वाक्य
292
-