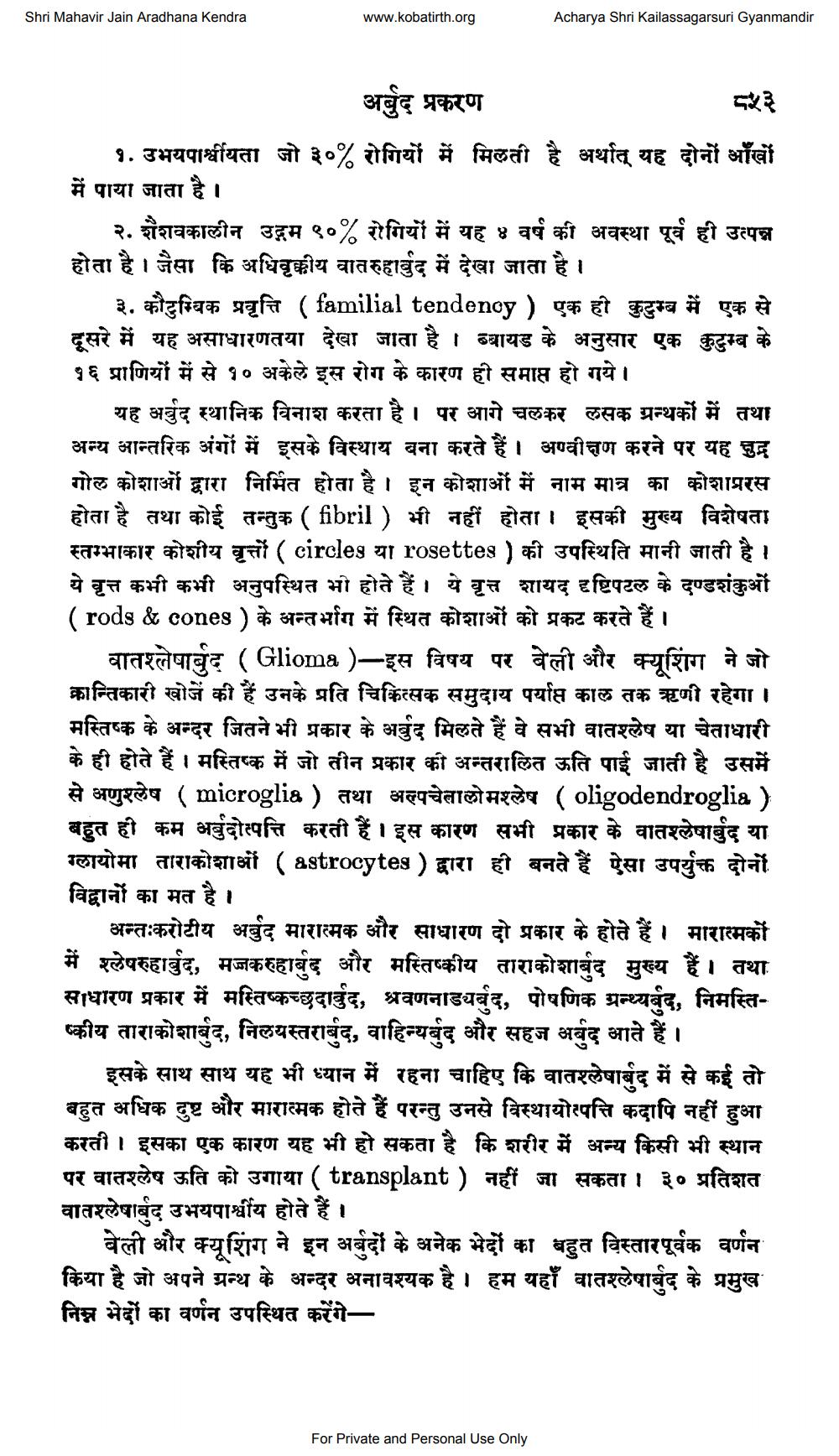________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
अर्बुद प्रकरण
८५३ १. उभयपार्थीयता जो ३०% रोगियों में मिलती है अर्थात् यह दोनों आँखों में पाया जाता है।
२. शैशवकालीन उद्गम ९०% रोगियों में यह ४ वर्ष की अवस्था पूर्व ही उत्पन्न होता है । जैसा कि अधिवृक्कीय वातरुहार्बुद में देखा जाता है।
३. कौटुम्बिक प्रवृत्ति ( familial tendenoy ) एक ही कुटुम्ब में एक से दूसरे में यह असाधारणतया देखा जाता है। ब्वायड के अनुसार एक कुटुम्ब के १६ प्राणियों में से १० अकेले इस रोग के कारण ही समाप्त हो गये। ___ यह अर्बुद स्थानिक विनाश करता है। पर आगे चलकर लसक ग्रन्थकों में तथा अन्य आन्तरिक अंगों में इसके विस्थाय बना करते हैं। अण्वीक्षण करने पर यह क्षुद्र गोल कोशाओं द्वारा निर्मित होता है। इन कोशाओं में नाम मात्र का कोशाप्ररस होता है तथा कोई तन्तुक ( fibril ) भी नहीं होता। इसकी मुख्य विशेषता स्तम्भाकार कोशीय वृत्तों ( circles या rosettes ) की उपस्थिति मानी जाती है। ये वृत्त कभी कभी अनुपस्थित भी होते हैं। ये वृत्त शायद दृष्टिपटल के दण्डशंकुओं ( rods & cones ) के अन्तर्भाग में स्थित कोशाओं को प्रकट करते हैं ।
वातश्लेषार्बुद (Glioma )-इस विषय पर बेली और क्यूशिंग ने जो क्रान्तिकारी खोजें की हैं उनके प्रति चिकित्सक समुदाय पर्याप्त काल तक ऋणी रहेगा। मस्तिष्क के अन्दर जितने भी प्रकार के अर्बुद मिलते हैं वे सभी वातश्लेष या चेताधारी के ही होते हैं । मस्तिष्क में जो तीन प्रकार की अन्तरालित ऊति पाई जाती है उसमें से अणुश्लेष ( microglia) तथा अल्पचेलालोमश्लेष (oligodendroglia) बहुत ही कम अर्बुदोत्पत्ति करती हैं। इस कारण सभी प्रकार के वातश्लेषार्बुद या ग्लायोमा ताराकोशाओं (astrocytes) द्वारा ही बनते हैं ऐसा उपर्युक्त दोनों विद्वानों का मत है।
अन्तःकरोटीय अर्बुद मारात्मक और साधारण दो प्रकार के होते हैं। मारात्मकों में श्लेषरुहार्बुद, मज्जकरुहार्बद और मस्तिष्कीय ताराकोशार्बुद मुख्य हैं। तथा. साधारण प्रकार में मस्तिष्कच्छदार्बुद, श्रवणनाड्यर्बुद, पोषणिक ग्रन्थ्यर्बुद, निमस्तिकीय ताराकोशार्बुद, निलयस्तरार्बुद, वाहिन्यर्बुद और सहज अर्बुद आते हैं।
इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि वातश्लेषार्बुद में से कई तो बहुत अधिक दुष्ट और मारात्मक होते हैं परन्तु उनसे विस्थायोत्पत्ति कदापि नहीं हुआ करती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शरीर में अन्य किसी भी स्थान पर वातश्लेष उति को उगाया ( transplant ) नहीं जा सकता। ३० प्रतिशत वातश्लेषाबंद उभयपा/य होते हैं।
बेली और क्यूशिंग ने इन अर्बुदों के अनेक भेदों का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है जो अपने ग्रन्थ के अन्दर अनावश्यक है। हम यहाँ वातश्लेषार्बुद के प्रमुख निम्न भेदों का वर्णन उपस्थित करेंगे
For Private and Personal Use Only