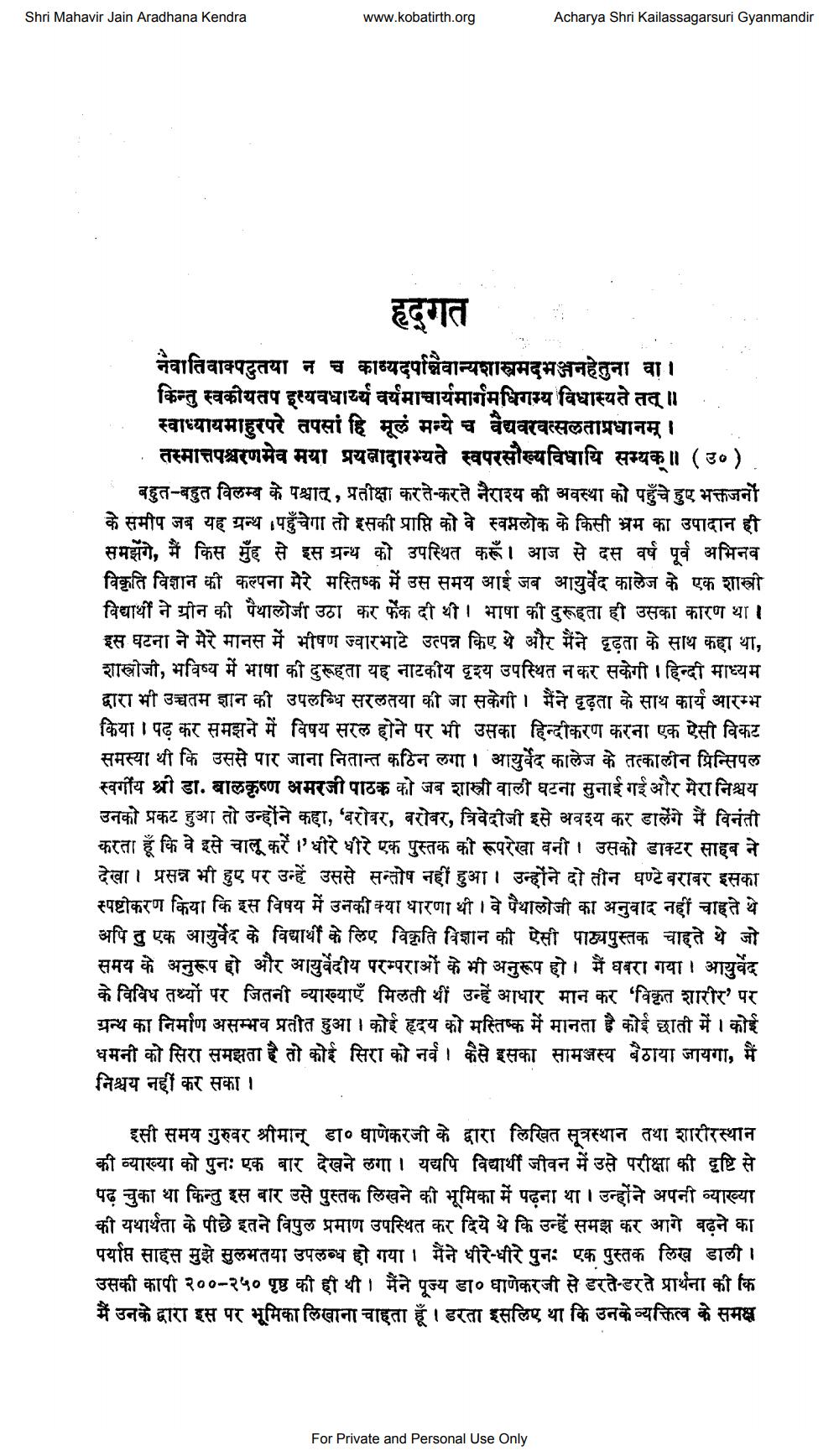________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
हृद्गत
नैवातिवाक्पटुतया न च काव्यदर्पान्नैवान्यशास्त्रमदभअनहेतुना वा । किन्तु स्वकीयतप इत्यवधार्थं वर्यमाचार्यमार्गमधिगम्य विधास्यते तत् ॥ स्वाध्यायमाहुरपरे तपसां हि मूलं मन्ये च वैद्यवरवत्सलताप्रधानम् । तस्मात्तपश्चरणमेव मया प्रयत्नादारभ्यते स्वपरसौख्यविधायि सम्यक् ॥ ( उ० )
बहुत-बहुत विलम्ब के पश्चात्, प्रतीक्षा करते-करते नैराश्य की अवस्था को पहुँचे हुए भक्तजनों के समीप जब यह ग्रन्थ पहुँचेगा तो इसकी प्राप्ति को वे स्वप्नलोक के किसी भ्रम का उपादान ही समझेंगे, मैं किस मुँह से इस ग्रन्थ को उपस्थित करूँ । आज से दस वर्ष पूर्व अभिनव विकृति विज्ञान की कल्पना मेरे मस्तिष्क में उस समय आई जब आयुर्वेद कालेज के एक शास्त्री विद्यार्थी ने ग्रीन की पैथालोजी उठा कर फेंक दी थी। भाषा की दुरूहता ही उसका कारण था । इस घटना ने मेरे मानस में भीषण ज्वारभाटे उत्पन्न किए थे और मैंने दृढ़ता के साथ कहा था, शास्त्रीजी, भविष्य में भाषा की दुरूहता यह नाटकीय दृश्य उपस्थित न कर सकेगी । हिन्दी माध्यम द्वारा भी उच्चतम ज्ञान की उपलब्धि सरलतया की जा सकेगी। मैंने दृढ़ता के साथ कार्य आरम्भ किया। पढ़ कर समझने में विषय सरल होने पर भी उसका हिन्दीकरण करना एक ऐसी विकट समस्या थी कि उससे पार जाना नितान्त कठिन लगा । आयुर्वेद कालेज के तत्कालीन प्रिन्सिपल स्वर्गीय श्री डा. बालकृष्ण अमरजी पाठक को जब शास्त्री वाली घटना सुनाई गई और मेरा निश्चय उनको प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा, 'बरोबर, बरोबर, त्रिवेदीजी इसे अवश्य कर डालेंगे मैं विनंती करता हूँ कि वे इसे चालू करें ।' धीरे धीरे एक पुस्तक की रूपरेखा बनी । उसको डाक्टर साहब ने देखा । प्रसन्न भी हुए पर उन्हें उससे सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने दो तीन घण्टे बराबर इसका स्पष्टीकरण किया कि इस विषय में उनकी क्या धारणा थी । वे पैथालोजी का अनुवाद नहीं चाहते थे अपि तु एक आयुर्वेद के विद्यार्थी के लिए विकृति विज्ञान की ऐसी पाठ्यपुस्तक चाहते थे जो समय के अनुरूप हो और आयुर्वेदीय परम्पराओं के भी अनुरूप हो। मैं घबरा गया। आयुर्वेद के विविध तथ्यों पर जितनी व्याख्याएँ मिलती थीं उन्हें आधार मान कर 'विकृत शारीर' पर ग्रन्थ का निर्माण असम्भव प्रतीत हुआ । कोई हृदय को मस्तिष्क में मानता है कोई छाती में । कोई धमनी को सिरा समझता है तो कोई सिरा को नर्व । कैसे इसका सामञ्जस्य बैठाया जायगा, मैं निश्चय नहीं कर सका ।
इसी समय गुरुवर श्रीमान् डा० घाणेकरजी के द्वारा लिखित सूत्रस्थान तथा शारीरस्थान की व्याख्या को पुनः एक बार देखने लगा । यद्यपि विद्यार्थी जीवन में उसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़ चुका था किन्तु इस बार उसे पुस्तक लिखने की भूमिका में पढ़ना था । उन्होंने अपनी व्याख्या की यथार्थता के पीछे इतने विपुल प्रमाण उपस्थित कर दिये थे कि उन्हें समझ कर आगे बढ़ने का पर्याप्त साहस मुझे सुलभतया उपलब्ध हो गया । मैंने धीरे-धीरे पुनः एक पुस्तक लिख डाली । उसकी कापी २००-२५० पृष्ठ की ही थी। मैंने पूज्य डा० घाणेकरजी से डरते-डरते प्रार्थना की कि मैं उनके द्वारा इस पर भूमिका लिखाना चाहता हूँ । डरता इसलिए था कि उनके व्यक्तित्व के समक्ष
For Private and Personal Use Only