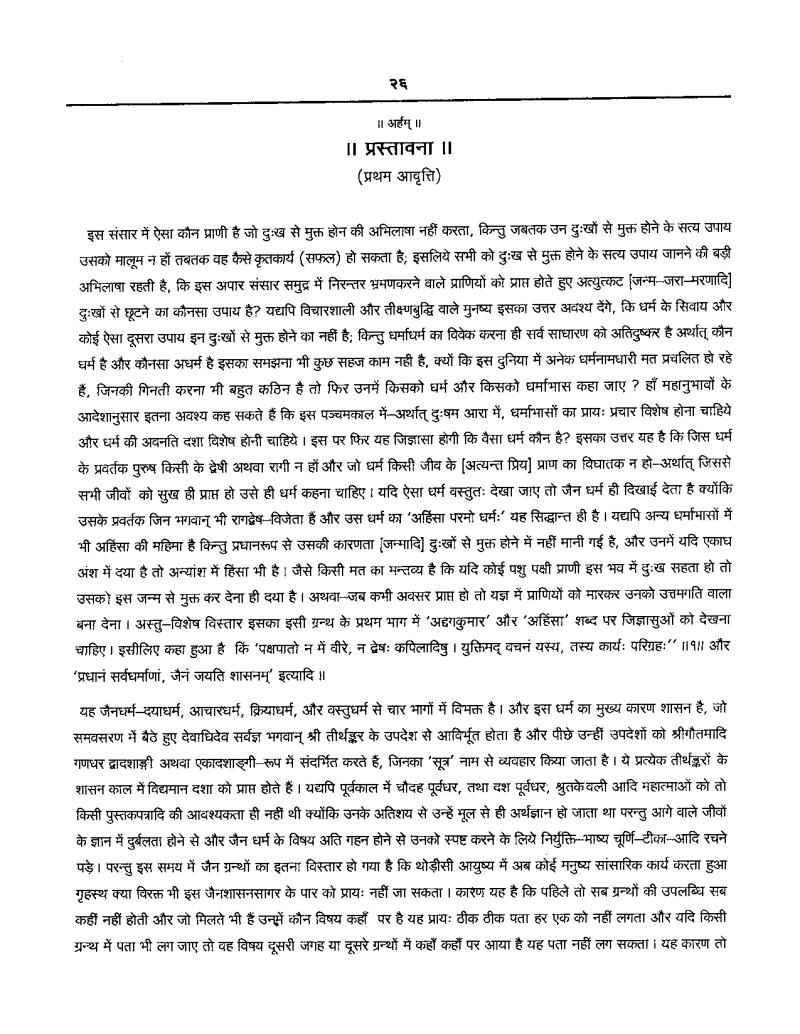________________ // अर्हम्॥ / प्रस्तावना / / (प्रथम आवृत्ति) इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो दुःख से मुक्त होन की अभिलाषा नहीं करता, किन्तु जबतक उन दुःखों से मुक्त होने के सत्य उपाय उसको मालूम न हों तबतक वह कैसे कृतकार्य (सफल) हो सकता है; इसलिये सभी को दुःख से मुक्त होने के सत्य उपाय जानने की बड़ी अभिलाषा रहती है, कि इस अपार संसार समुद्र में निरन्तर भ्रमणकरने वाले प्राणियों को प्राप्त होते हुए अत्युत्कट जन्म-जरा-मरणादि] दुःखों से छूटने का कौनसा उपाय है? यद्यपि विचारशाली और तीक्ष्णबुद्धि वाले मुनष्य इसका उत्तर अवश्य देंगे, कि धर्म के सिवाय और कोई ऐसा दूसरा उपाय इन दुःखों से मुक्त होने का नहीं है; किन्तु धर्माधर्म का विवेक करना ही सर्व साधारण को अतिदुष्कर है अर्थात् कौन धर्म है और कौनसा अधर्म है इसका समझना भी कुछ सहज काम नही है, क्यों कि इस दुनिया में अनेक धर्मनामधारी मत प्रचलित हो रहे हैं, जिनकी गिनती करना भी बहुत कठिन है तो फिर उनमें किसको धर्म और किसको धर्माभास कहा जाए ? हाँ महानुभावों के आदेशानुसार इतना अवश्य कह सकते हैं कि इस पञ्चमकाल में अर्थात् दुःषम आरा में, धर्माभासों का प्रायः प्रचार विशेष होना चाहिये और धर्म की अवनति दशा विशेष होनी चाहिये। इस पर फिर यह जिज्ञासा होगी कि वैसा धर्म कौन है? इसका उत्तर यह है कि जिस धर्म के प्रवर्तक पुरुष किसी के द्वेषी अथवा रागी न हों और जो धर्म किसी जीव के [अत्यन्त प्रिय प्राण का विघातक न हो-अर्थात् जिससे सभी जीवों को सुख ही प्राप्त हो उसे ही धर्म कहना चाहिए। यदि ऐसा धर्म वस्तुतः देखा जाए तो जैन धर्म ही दिखाई देता है क्योंकि उसके प्रवर्तक जिन भगवान् भी रागद्वेष--विजेता हैं और उस धर्म का 'अहिंसा परमो धर्मः' यह सिद्धान्त ही है। यद्यपि अन्य धर्माभासों में भी अहिंसा की महिमा है किन्तु प्रधानरूप से उसकी कारणता जन्मादि] दुःखों से मुक्त होने में नहीं मानी गई है, और उनमें यदि एकाध अंश में दया है तो अन्यांश में हिंसा भी है। जैसे किसी मत का मन्तव्य है कि यदि कोई पशु पक्षी प्राणी इस भव में दुःख सहता हो तो उसको इस जन्म से मुक्त कर देना ही दया है। अथवा जब कभी अवसर प्राप्त हो तो यज्ञ में प्राणियों को मारकर उनको उत्तमगति वाला बना देना / अस्तु-विशेष विस्तार इसका इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में 'अदृगकुमार' और 'अहिंसा' शब्द पर जिज्ञासुओं को देखना चाहिए। इसीलिए कहा हुआ है कि 'पक्षपातो न में वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु / युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः" ||14 और 'प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्' इत्यादि / यह जैनधर्म-दयाधर्म, आचारधर्म, क्रियाधर्म, और वस्तुधर्म से चार भागों में विभक्त है। और इस धर्म का मुख्य कारण शासन है, जो समवसरण में बैठे हुए देवाधिदेव सर्वज्ञ भगवान् श्री तीर्थङ्कर के उपदेश से आविर्भूत होता है और पीछे उन्हीं उपदेशों को श्रीगौतमादि गणधर द्वादशाङ्गी अथवा एकादशागी रूप में संदर्भित करते हैं, जिनका 'सूत्र' नाम से व्यवहार किया जाता है। ये प्रत्येक तीर्थक्करों के शासन काल में विद्यमान दशा को प्राप्त होते हैं / यद्यपि पूर्वकाल में चौदह पूर्वधर, तथा दश पूर्वधर, श्रुतके वली आदि महात्माओं को तो किसी पुस्तकपत्रादि की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि उनके अतिशय से उन्हें मूल से ही अर्थज्ञान हो जाता था परन्तु आगे वाले जीवों के ज्ञान में दुर्बलता होने से और जैन धर्म के विषय अति गहन होने से उनको स्पष्ट करने के लिये नियुक्ति-भाष्य चूर्णि-टीका-आदि रचने पड़े। परन्तु इस समय में जैन ग्रन्थों का इतना विस्तार हो गया है कि थोड़ीसी आयुष्य में अब कोई मनुष्य सांसारिक कार्य करता हुआ गृहस्थ क्या विरक्त भी इस जैनशासनसागर के पार को प्रायः नहीं जा सकता। कारण यह है कि पहिले तो सब ग्रन्थों की उपलब्धि सब कहीं नहीं होती और जो मिलते भी हैं उनमें कौन विषय कहाँ पर है यह प्रायः ठीक ठीक पता हर एक को नहीं लगता और यदि किसी ग्रन्थ में पता भी लग जाए तो वह विषय दूसरी जगह या दूसरे ग्रन्थों में कहाँ कहाँ पर आया है यह पता नहीं लग सकता। यह कारण तो