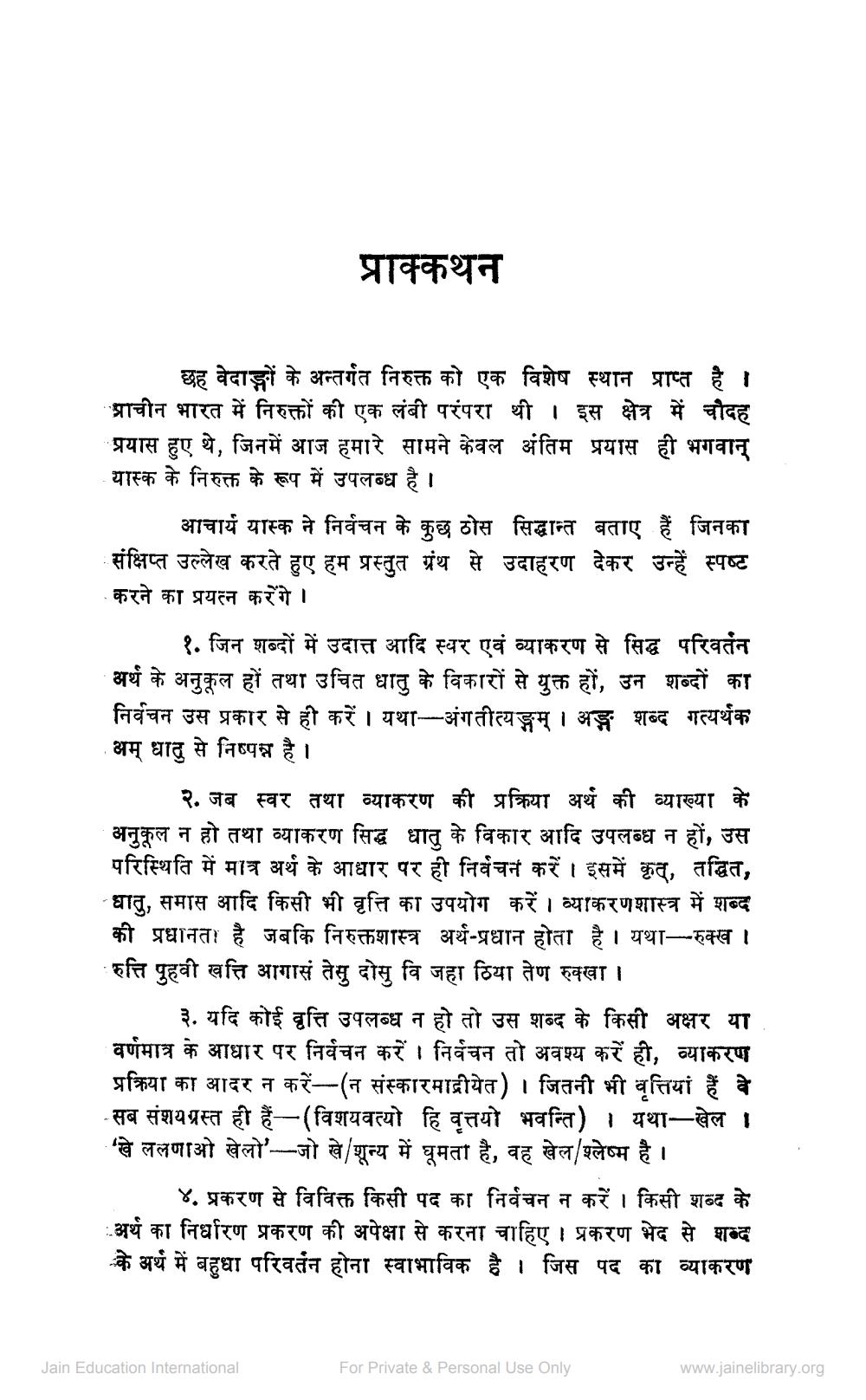________________
प्राक्कथन
छह वेदाङ्गों के अन्तर्गत निरुक्त को एक विशेष स्थान प्राप्त है । प्राचीन भारत में निरुक्तों की एक लंबी परंपरा थी । इस क्षेत्र में चौदह प्रयास हुए थे, जिनमें आज हमारे सामने केवल अंतिम प्रयास ही भगवान् - यास्क के निरुक्त के रूप में उपलब्ध है ।
आचार्य यास्क ने निर्वचन के कुछ ठोस सिद्धान्त बताए हैं जिनका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए हम प्रस्तुत ग्रंथ से उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे ।
१. जिन शब्दों में उदात्त आदि स्वर एवं व्याकरण से सिद्ध परिवर्तन अर्थ के अनुकूल हों तथा उचित धातु के विकारों से युक्त हों, उन शब्दों का निर्वचन उस प्रकार से ही करें । यथा - अंगतीत्यङ्गम् । अङ्ग शब्द गत्यर्थक अम् धातु से निष्पन्न है ।
२. जब स्वर तथा व्याकरण की प्रक्रिया अर्थ की व्याख्या के अनुकूल न हो तथा व्याकरण सिद्ध धातु के विकार आदि उपलब्ध न हों, उस परिस्थिति में मात्र अर्थ के आधार पर ही निर्वचन करें। इसमें कृत्, तद्धित, धातु, समास आदि किसी भी वृत्ति का उपयोग करें । व्याकरणशास्त्र में शब्द की प्रधानता है जबकि निरुक्तशास्त्र अर्थ - प्रधान होता है । यथा — रुक्ख । रुत्ति पुहवी खत्ति आगासं तेसु दोसु वि जहा ठिया तेण रुक्खा ।
३. यदि कोई वृत्ति उपलब्ध न हो तो उस शब्द के किसी अक्षर या वर्णमात्र के आधार पर निर्वचन करें । निर्वचन तो अवश्य करें ही, व्याकरण प्रक्रिया का आदर न करें - ( न संस्कारमाद्रीयेत ) । जितनी भी वृत्तियां हैं वे - सब संशयग्रस्त ही हैं - ( विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति ) । यथा — खेल 1 'खे ललणाओ खेलो' – जो खे / शून्य में घूमता है, वह खेल / श्लेष्म है ।
४. प्रकरण से विविक्त किसी पद का निर्वचन न करें । किसी शब्द के अर्थ का निर्धारण प्रकरण की अपेक्षा से करना चाहिए। प्रकरण भेद से शब्द -के अर्थ में बहुधा परिवर्तन होना स्वाभाविक है । जिस पद का व्याकरण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org