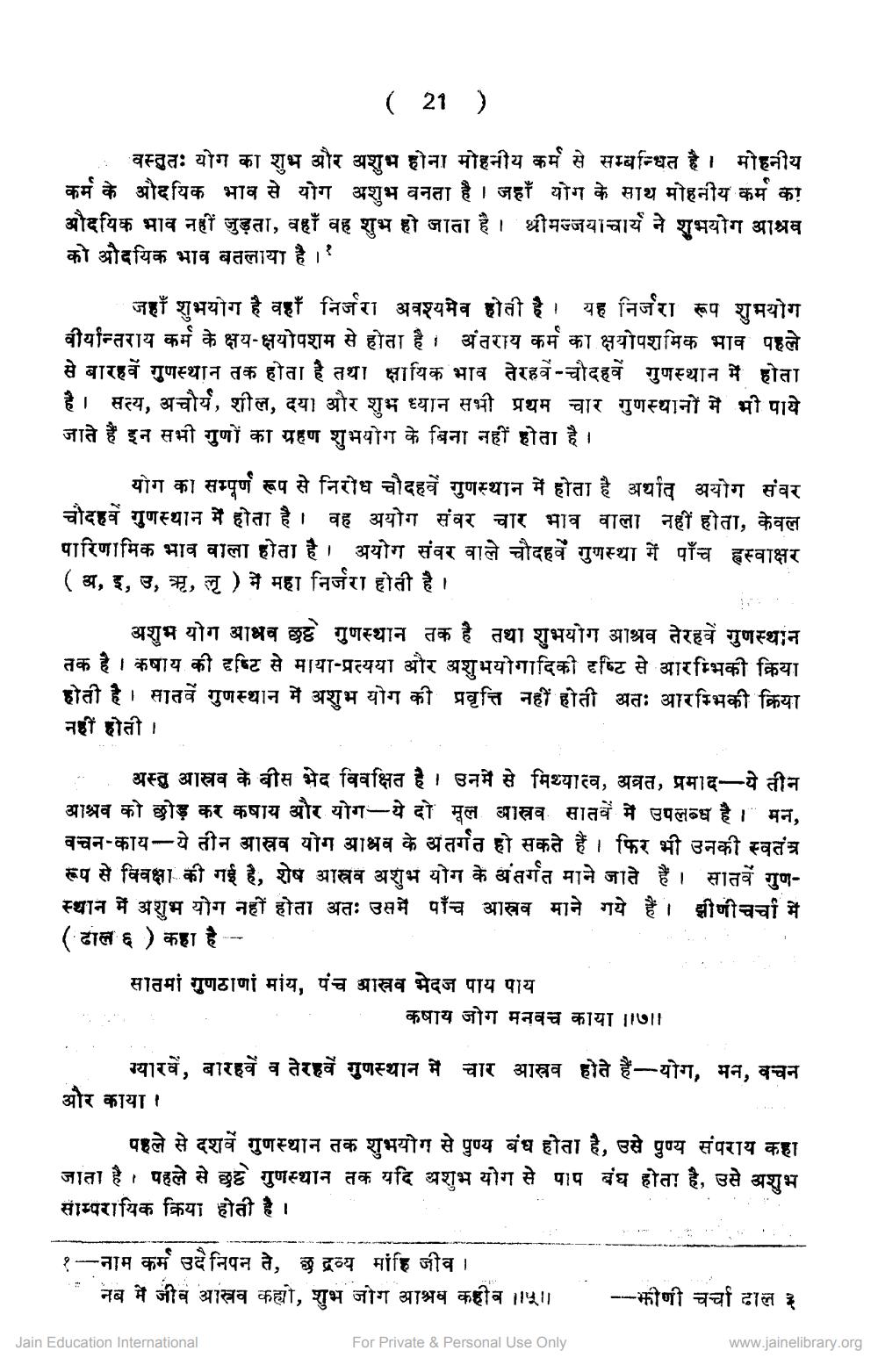________________
( 21 ) वस्तुतः योग का शुभ और अशुभ होना मोहनीय कर्म से सम्बन्धित है। मोहनीय कर्म के औदयिक भाव से योग अशुभ वनता है । जहाँ योग के साथ मोहनीय कर्म का औदयिक भाव नहीं जुड़ता, वहाँ वह शुभ हो जाता है। श्रीमज्जयाचार्य ने शुभयोग आश्रव को औदयिक भाव बतलाया है।'
जहाँ शुभयोग है वहाँ निर्जरा अवश्यमेव होती है। यह निर्जरा रूप शुभयोग वीर्यान्तराय कर्म के क्षय-क्षयोपशम से होता है। अंतराय कर्म का क्षयोपशमिक भाव पहले से बारहवें गुणस्थान तक होता है तथा क्षायिक भाव तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में होता है। सत्य, अचौर्य, शील, दया और शुभ ध्यान सभी प्रथम चार गुणस्थानों में भी पाये जाते हैं इन सभी गुणों का ग्रहण शुभयोग के बिना नहीं होता है।
योग का सम्पूर्ण रूप से निरोध चौदहवें गुणस्थान में होता है अर्थात् अयोग संवर चौदहवें गुणस्थान में होता है। वह अयोग संवर चार भाव वाला नहीं होता, केवल पारिणामिक भाव वाला होता है। अयोग संवर वाले चौदहवं गुणस्था में पाँच हस्वाक्षर ( अ, इ, उ, ऋ, 7 ) में महा निर्जरा होती है ।
__ अशुभ योग आव छठे गुणस्थान तक है तथा शुभयोग आश्रव तेरहवें गुणस्थान तक है । कषाय की दृष्टि से माया-प्रत्यया और अशुभयोगादिको दृष्टि से आरम्भिकी क्रिया होती है। सातवें गुणस्थान में अशुभ योग की प्रवृत्ति नहीं होती अतः आरम्भिकी क्रिया नहीं होती।
... अस्तु आस्रव के बीस भेद विवक्षित है। उनमें से मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद-ये तीन आश्रव को छोड़ कर कषाय और योग-ये दो मूल आस्रव सातवें में उपलब्ध है। मन, वचन-काय-ये तीन आस्रव योग आश्रव के अंतर्गत हो सकते हैं। फिर भी उनकी स्वतंत्र रूप से विवक्षा की गई है, शेष आस्रव अशुभ योग के अंतर्गत माने जाते हैं। सातवें गुणस्थान में अशुभ योग नहीं होता अतः उसमें पाँच आस्रव माने गये हैं। झीणीचर्चा में (ढाल ६ ) कहा है -- सातमां गुणठाणां मांय, पंच आस्रव भेदज पाय पाय
कषाय जोग मनवच काया ।।७।।
__ ग्यारवें, बारहवें व तेरहवें गुणस्थान में चार आस्रव होते हैं-योग, मन, वचन और काया।
पहले से दशवे गुणस्थान तक शुभयोग से पुण्य बंध होता है, उसे पुण्य संपराय कहा जाता है। पहले से छठे गुणस्थान तक यदि अशुभ योग से पाप बंघ होता है, उसे अशुभ साम्परायिक क्रिया होती है।
१-नाम कर्म उदैनिपन ते, छ द्रव्य मांहि जीव।।
नब में जीव आत्रव कह्यो, शुभ जोग आश्रव कहीव ॥५॥
---झीणी चर्चा दाल ३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org