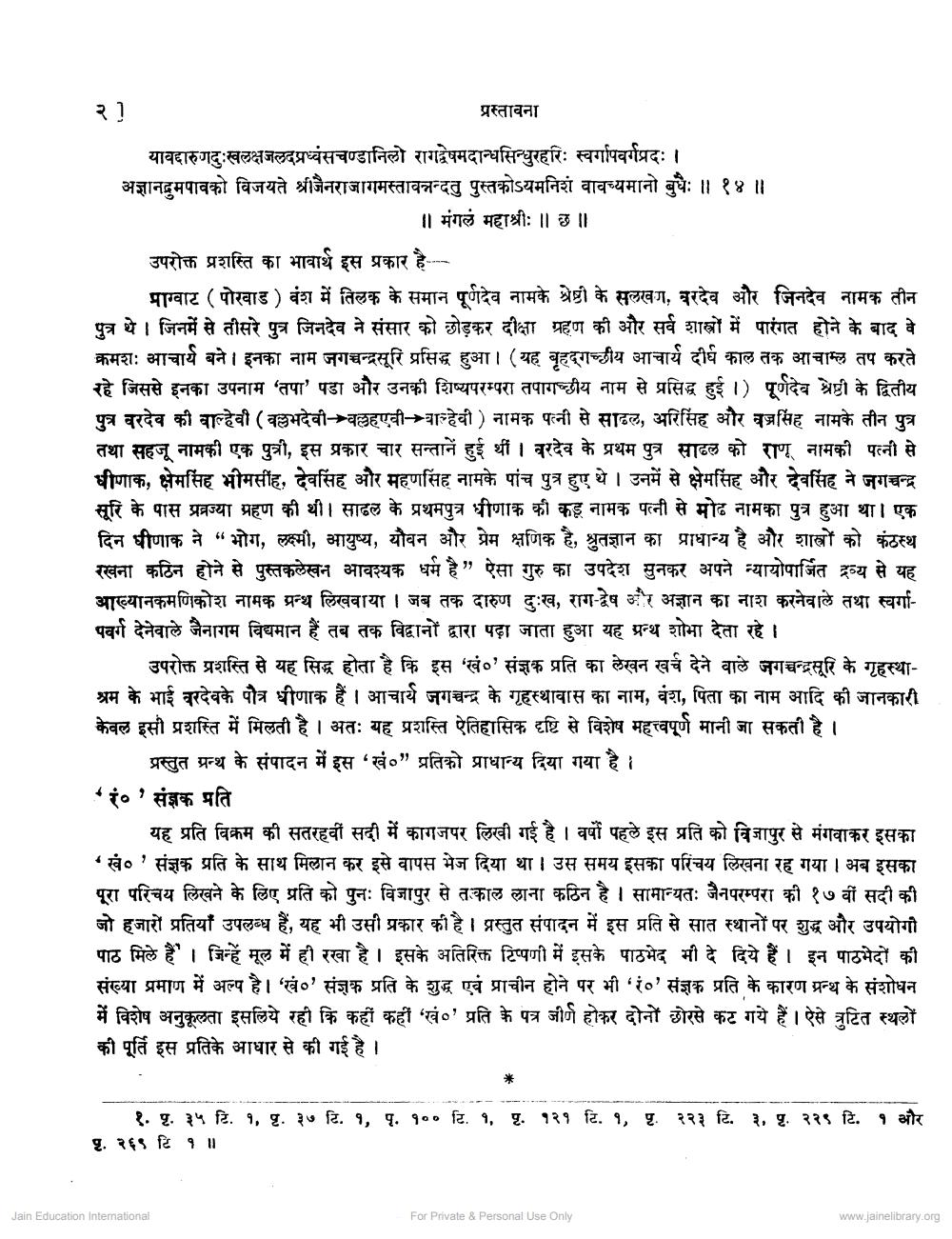________________
प्रस्तावना
यावद्दारुणदुःखलक्षजलदप्रध्वंसचण्डानिलो रागद्वेषमदान्धसिन्धुरहरिः स्वर्गापवर्गप्रदः । अज्ञानदुमपावको विजयते श्रीजैनराजागमस्तावन्नन्दतु पुस्तकोऽयमनिशं वावच्यमानो बुधैः ॥ १४॥
॥ मंगलं महाश्रीः ॥ छ ।
उपरोक्त प्रशस्ति का भावार्थ इस प्रकार है-----
प्राग्वाट ( पोरवाड) वंश में तिलक के समान पूर्णदेव नामके श्रेष्ठी के सलखग, वरदेव और जिनदेव नामक तीन पुत्र थे। जिनमें से तीसरे पुत्र जिनदेव ने संसार को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की और सर्व शास्त्रों में पारंगत होने के बाद वे क्रमशः आचार्य बने । इनका नाम जगच्चन्द्रसूरि प्रसिद्ध हुआ। (यह बहद्गच्छीय आचार्य दीर्घ काल तक आचाम्ल तप करते रहे जिससे इनका उपनाम 'तपा' पडा और उनकी शिष्यपरम्परा तपागच्छीय नाम से प्रसिद्ध हुई ।) पूर्णदेव श्रेष्ठी के द्वितीय पुत्र वरदेव की वाल्हेवी (वल्लभदेवीवल्लहएवी-वाल्हेवी) नामक पत्नी से साढल, अरिसिंह और वज्रसिंह नामके तीन पुत्र तथा सहजू नामकी एक पुत्री, इस प्रकार चार सन्तानें हुई थीं। वरदेव के प्रथम पुत्र साढल को राणू नामकी पत्नी से धीणाक, क्षेमसिंह भीमसींह, देवसिंह और महणसिंह नामके पांच पुत्र हए थे । उनमें से क्षेमसिंह और देवसिंह ने जगच्चन्द्र सूरि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की थी। साढल के प्रथमपुत्र धीणाक की कडू नामक पत्नी से मोढ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन धीणाक ने “भोग, लक्ष्मी, आयुष्य, यौवन और प्रेम क्षणिक है, श्रुतज्ञान का प्राधान्य है और शास्त्रों को कंठस्थ रखना कठिन होने से पुस्तकलेखन आवश्यक धर्म है" ऐसा गुरु का उपदेश सुनकर अपने न्यायोपार्जित द्रव्य से यह आख्यानकमणिकोश नामक ग्रन्थ लिखवाया । जब तक दारुण दुःख, राग-द्वेष और अज्ञान का नाश करनेवाले तथा स्वर्गापवर्ग देनेवाले जैनागम विद्यमान हैं तब तक विद्वानों द्वारा पढ़ा जाता हुआ यह ग्रन्थ शोभा देता रहे।
उपरोक्त प्रशस्ति से यह सिद्ध होता है कि इस 'खं०' संज्ञक प्रति का लेखन खर्च देने वाले जगच्चन्द्रसूरि के गृहस्थाश्रम के भाई वरदेवके पौत्र धीणाक हैं । आचार्य जगच्चन्द्र के गृहस्थावास का नाम, वंश, पिता का नाम आदि की जानकारी केवल इसी प्रशस्ति में मिलती है । अतः यह प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है ।
प्रस्तुत ग्रन्थ के संपादन में इस 'खं०" प्रतिको प्राधान्य दिया गया है। “२०' संज्ञक प्रति
यह प्रति विक्रम की सतरहवीं सदी में कागजपर लिखी गई है । वर्षों पहले इस प्रति को विजापुर से मंगवाकर इसका 'ख' संज्ञक प्रति के साथ मिलान कर इसे वापस भेज दिया था। उस समय इसका परिचय लिखना रह गया। अब इसका पूरा परिचय लिखने के लिए प्रति को पुनः विजापुर से तकाल लाना कठिन है । सामान्यतः जैनपरम्परा की १७ वीं सदी की जो हजारों प्रतियाँ उपलब्ध हैं, यह भी उसी प्रकार की है। प्रस्तुत संपादन में इस प्रति से सात स्थानों पर शुद्ध और उपयोगी पाठ मिले हैं। जिन्हें मूल में ही रखा है। इसके अतिरिक्त टिप्पणी में इसके पाठभेद भी दे दिये हैं। इन पाठभेदों की संख्या प्रमाण में अल्प है। 'खं०' संज्ञक प्रति के शुद्ध एवं प्राचीन होने पर भी '२०' संज्ञक प्रति के कारण ग्रन्थ के संशोधन में विशेष अनुकूलता इसलिये रही कि कहीं कहीं 'खं०' प्रति के पत्र जीर्ण होकर दोनों छोरसे कट गये हैं। ऐसे त्रटित स्थलों की पूर्ति इस प्रतिके आधार से की गई है ।
पृ. १२१ टि. १, पृ. २२३ टि. ३, पृ. २२९ टि. १ और
१. पृ. ३५ टि. १, पृ. ३७ टि. १, पृ. १०. टि. १, पृ. २६९ टि १ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org