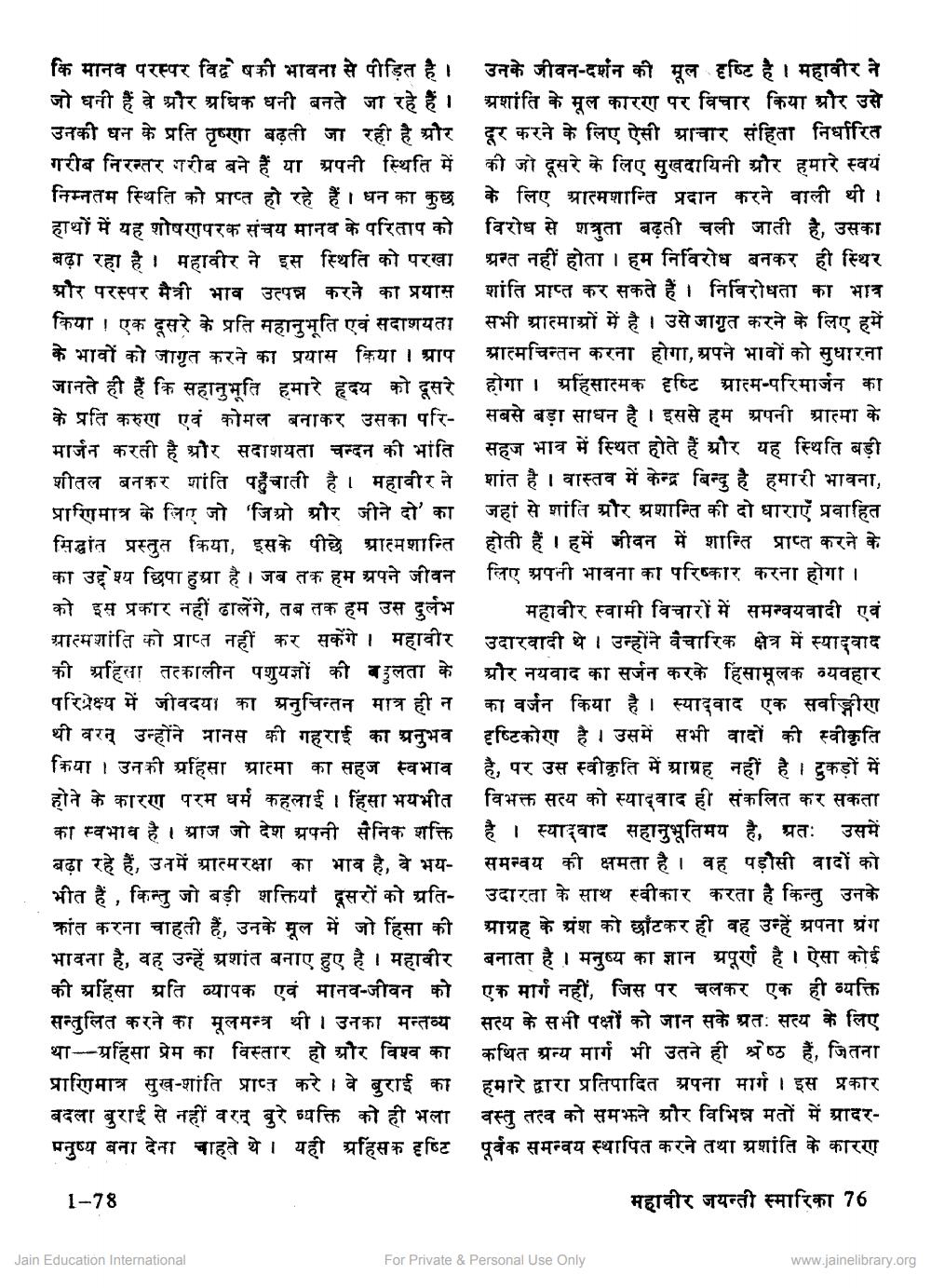________________
पीड़ित है। जा रहे हैं ।
अपनी
कि मानव परस्पर विद्वे षकी भावना जो धनी हैं वे और अधिक धनी बनते उनकी धन के प्रति तृष्णा बढ़ती जा रही है और गरीब निरन्तर गरीब बने हैं या स्थिति में निम्नतम स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। धन का कुछ हाथों में यह शोषणपरक संचय मानव के परिताप को बढ़ा रहा है। महावीर ने इस स्थिति को परखा और परस्पर मैत्री भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। एक दूसरे के प्रति महानुभूति एवं सदाशयता के भावों को जागृत करने का प्रयास किया । श्राप जानते ही हैं कि सहानुभूति हमारे हृदय को दूसरे के प्रति करुण एवं कोमल बनाकर उसका परिमार्जन करती है और सदाशयता चन्दन की भांति शीतल बनकर शांति पहुँचाती है। महावीर ने प्राणिमात्र के लिए जो 'जियो और जीने दो' का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसके पीछे श्रात्मशान्ति का उद्देश्य छिपा हुआ है। जब तक हम अपने जीवन को इस प्रकार नहीं ढालेंगे, तब तक हम उस दुर्लभ आत्मशांति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे । महावीर की हिंसा तत्कालीन पशुयज्ञों की बहुलता के परिप्रेक्ष्य में जीवदया का अनुचिन्तन मात्र ही न थी वरन् उन्होंने मानस की गहराई का अनुभव किया। उनकी हिंसा श्रात्मा का सहज स्वभाव होने के कारण परम धर्म कहलाई । हिंसा भयभीत का स्वभाव है । आज जो देश अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, उनमें आत्मरक्षा का भाव है, वे भयभीत हैं, किन्तु जो बड़ी शक्तियाँ दूसरों को प्रतिक्रांत करना चाहती हैं, उनके मूल में जो हिंसा की भावना है, वह उन्हें प्रशांत बनाए हुए है । महावीर की अहिंसा प्रति व्यापक एवं मानव-जीवन को सन्तुलित करने का मूलमन्त्र थी। उनका मन्तव्य था -- प्रहिंसा प्रेम का विस्तार हो और विश्व का प्राणिमात्र सुख-शांति प्राप्त करे। वे बुराई का बदला बुराई से नहीं वरन बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते थे । यही अहिंसक दृष्टि
1-78
Jain Education International
उनके जीवन-दर्शन की मूल दृष्टि है । महावीर ने अशांति के मूल कारण पर विचार किया और उसे दूर करने के लिए ऐसी आचार संहिता निर्धारित की जो दूसरे के लिए सुखदायिनी और हमारे स्वयं के लिए आत्मशान्ति प्रदान करने वाली थी । विरोध से शत्रुता बढ़ती चली जाती है, उसका अन्त नहीं होता । हम निर्विरोध बनकर ही स्थिर शांति प्राप्त कर सकते हैं । निविरोधता का भाव सभी आत्माओं में है । उसे जागृत करने के लिए हमें आत्मचिन्तन करना होगा, अपने भावों को सुधारना होगा । अहिंसात्मक दृष्टि आत्म- परिमार्जन का सबसे बड़ा साधन है । इससे हम अपनी श्रात्मा के सहज भाव में स्थित होते हैं और यह स्थिति बड़ी शांत है । वास्तव में केन्द्र बिन्दु है हमारी भावना, जहां से शांति और अशान्ति की दो धाराएँ प्रवाहित होती हैं । हमें जीवन में शान्ति प्राप्त करने के लिए अपनी भावना का परिष्कार करना होगा ।
महावीर स्वामी विचारों में समन्वयवादी एवं उदारवादी थे । उन्होंने वैचारिक क्षेत्र में स्याद्वाद और नयवाद का सर्जन करके हिंसामूलक व्यवहार का वर्जन किया है । स्यादवाद एक सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण है । उसमें सभी वादों की स्वीकृति है, पर उस स्वीकृति में प्राग्रह नहीं है । टुकड़ों में विभक्त सत्य को स्याद्वाद ही संकलित कर सकता है । स्यादवाद सहानुभूतिमय है, श्रतः उसमें समन्वय की क्षमता है । वह पड़ौसी वादों को उदारता के साथ स्वीकार करता है किन्तु उनके आग्रह के अंश को छाँटकर ही वह उन्हें अपना अंग बनाता है । मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण है । ऐसा कोई एक मार्ग नहीं, जिस पर चलकर एक ही व्यक्ति सत्य के सभी पक्षों को जान सके प्रतः सत्य के लिए कथित अन्य मार्ग भी उतने ही श्रेष्ठ हैं, जितना हमारे द्वारा प्रतिपादित अपना मार्ग । इस प्रकार वस्तु तत्व को समझने और विभिन्न मतों में प्रदरपूर्वक समन्वय स्थापित करने तथा प्रशांति के कारण
महावीर जयन्ती स्मारिका 76
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org