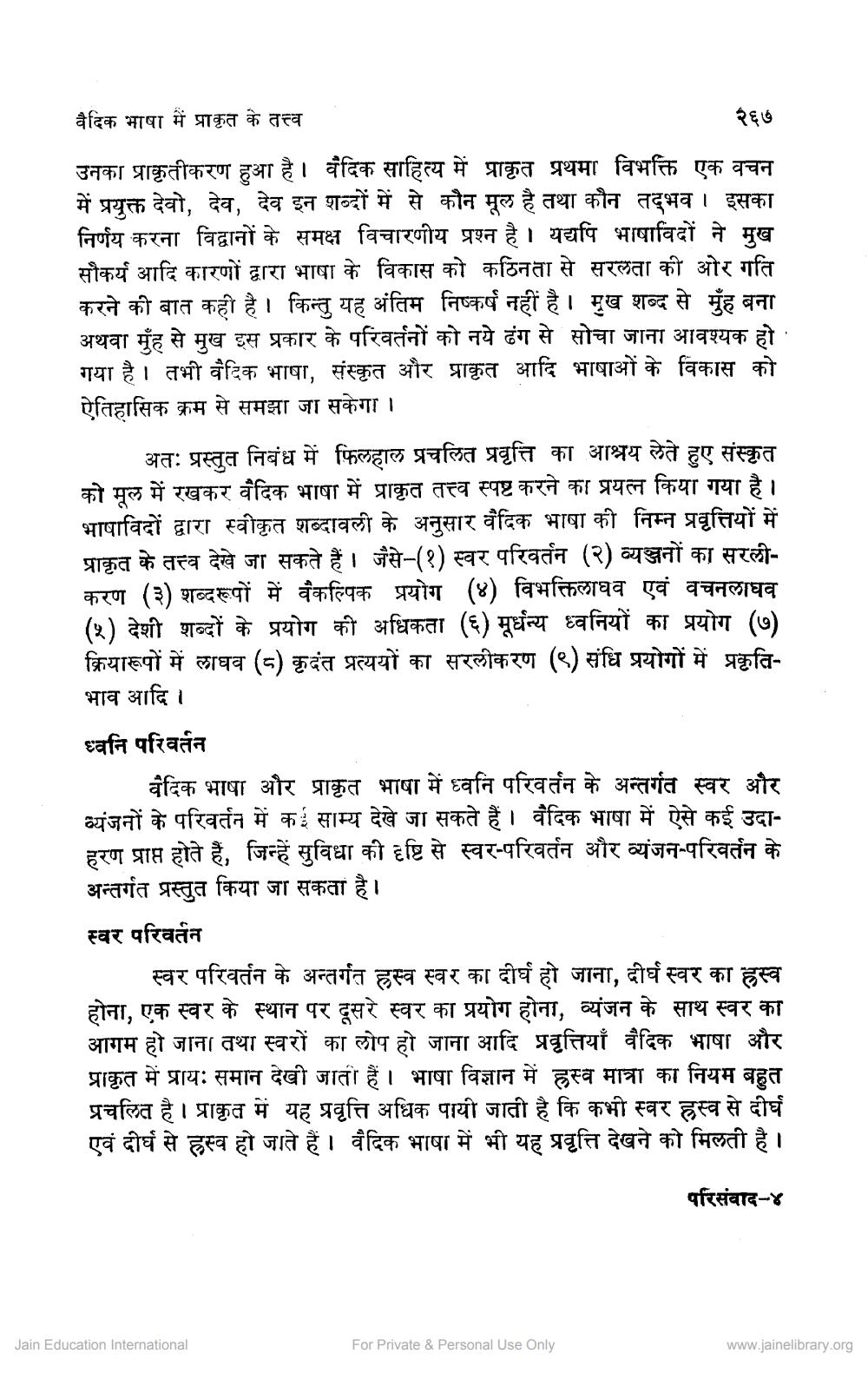________________
वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व
२६७
उनका प्राकृतीकरण हुआ है। वैदिक साहित्य में प्राकृत प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त देवो, देव, देव इन शब्दों में से कौन मूल है तथा कौन तद्भव । इसका निर्णय करना विद्वानों के समक्ष विचारणीय प्रश्न है। यद्यपि भाषाविदों ने मुख सौकर्य आदि कारणों द्वारा भाषा के विकास को कठिनता से सरलता की ओर गति करने की बात कही है। किन्तु यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। मुख शब्द से मुँह बना अथवा मुँह से मुख इस प्रकार के परिवर्तनों को नये ढंग से सोचा जाना आवश्यक हो । गया है। तभी वैदिक भाषा, संस्कृत और प्राकृत आदि भाषाओं के विकास को ऐतिहासिक क्रम से समझा जा सकेगा।
अतः प्रस्तुत निबंध में फिलहाल प्रचलित प्रवृत्ति का आश्रय लेते हुए संस्कृत को मूल में रखकर वैदिक भाषा में प्राकृत तत्त्व स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। भाषाविदों द्वारा स्वीकृत शब्दावली के अनुसार वैदिक भाषा की निम्न प्रवृत्तियों में प्राकृत के तत्त्व देखे जा सकते हैं। जैसे-(१) स्वर परिवर्तन (२) व्यञ्जनों का सरलीकरण (३) शब्दरूपों में वैकल्पिक प्रयोग (४) विभक्तिलाघव एवं वचनलाघव (५) देशी शब्दों के प्रयोग की अधिकता (६) मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग (७) क्रियारूपों में लाघव (८) कृदंत प्रत्ययों का सरलीकरण (९) संधि प्रयोगों में प्रकृतिभाव आदि। ध्वनि परिवर्तन
वैदिक भाषा और प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवर्तन के अन्तर्गत स्वर और व्यंजनों के परिवर्तन में कई साम्य देखे जा सकते हैं। वैदिक भाषा में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से स्वर-परिवर्तन और व्यंजन-परिवर्तन के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वर परिवर्तन
स्वर परिवर्तन के अन्तर्गत ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना, दीर्घ स्वर का ह्रस्व होना, एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर का प्रयोग होना, व्यंजन के साथ स्वर का आगम हो जाना तथा स्वरों का लोप हो जाना आदि प्रवृत्तियाँ वैदिक भाषा और प्राकृत में प्रायः समान देखी जाती हैं। भाषा विज्ञान में ह्रस्व मात्रा का नियम बहुत प्रचलित है। प्राकृत में यह प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है कि कभी स्वर ह्रस्व से दीर्घ एवं दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। वैदिक भाषा में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
परिसंवाद-४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org