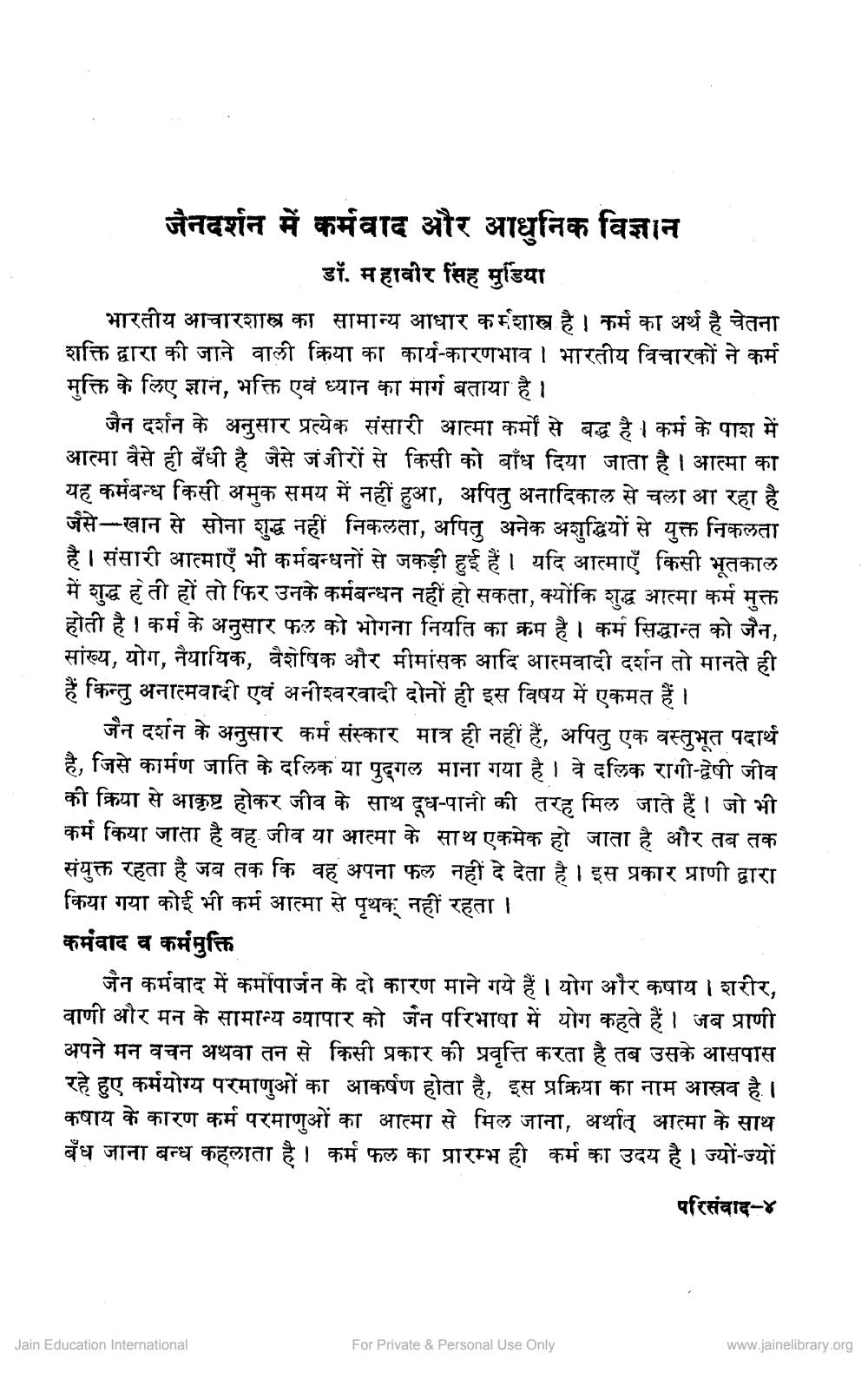________________
जैनदर्शन में कर्मवाद और आधुनिक विज्ञान
डॉ. महावीर सिंह मुडिया भारतीय आचारशास्त्र का सामान्य आधार कर्मशास्त्र है। कर्म का अर्थ है चेतना शक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया का कार्य-कारणभाव । भारतीय विचारकों ने कर्म मुक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का मार्ग बताया है।
जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक संसारी आत्मा कर्मों से बद्ध है। कर्म के पाश में आत्मा वैसे ही बँधी है जैसे जंजीरों से किसी को बाँध दिया जाता है । आत्मा का यह कर्मबन्ध किसी अमुक समय में नहीं हुआ, अपितु अनादिकाल से चला आ रहा है जैसे-खान से सोना शुद्ध नहीं निकलता, अपितु अनेक अशुद्धियों से युक्त निकलता है । संसारी आत्माएँ भी कर्मबन्धनों से जकड़ी हुई हैं। यदि आत्माएँ किसी भूतकाल में शुद्ध हे ती हों तो फिर उनके कर्मबन्धन नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध आत्मा कर्म मुक्त होती है । कर्म के अनुसार फल को भोगना नियति का क्रम है। कर्म सिद्धान्त को जैन, सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इस विषय में एकमत हैं।
जैन दर्शन के अनुसार कर्म संस्कार मात्र ही नहीं हैं, अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ है, जिसे कार्मण जाति के दलिक या पुद्गल माना गया है। वे दलिक रागी-द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाते हैं। जो भी कर्म किया जाता है वह जीव या आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है और तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता है । इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक नहीं रहता। कर्मवाद व कर्ममुक्ति
जैन कर्मवाद में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं । योग और कषाय । शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार को जैन परिभाषा में योग कहते हैं। जब प्राणी अपने मन वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आसपास रहे हुए कर्मयोग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है, इस प्रक्रिया का नाम आस्रव है। कषाय के कारण कर्म परमाणुओं का आत्मा से मिल जाना, अर्थात् आत्मा के साथ बँध जाना बन्ध कहलाता है। कर्म फल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है । ज्यों-ज्यों
परिसंवाद-४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org