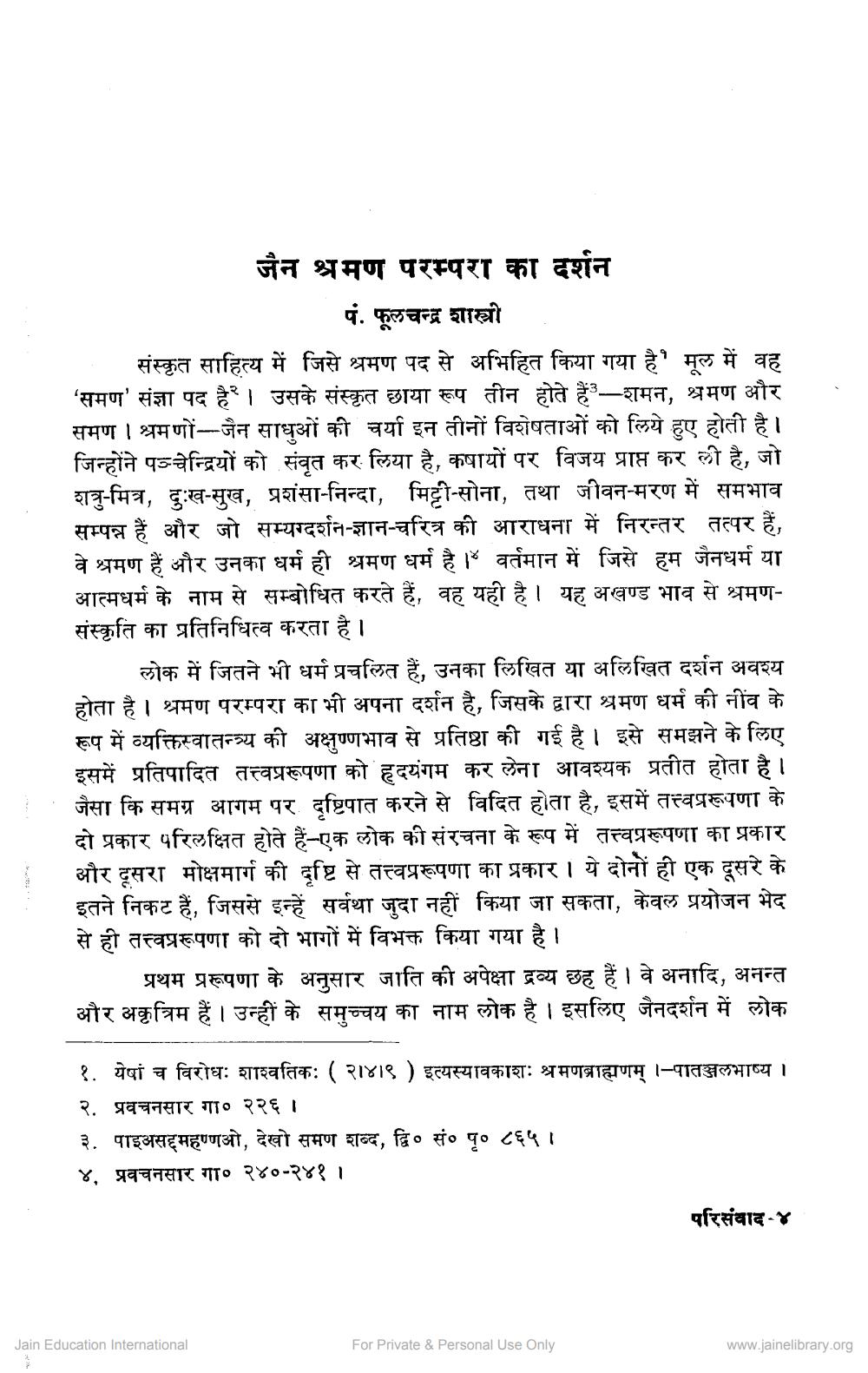________________
जैन श्रमण परम्परा का दर्शन
पं. फूलचन्द्र शास्त्री संस्कृत साहित्य में जिसे श्रमण पद से अभिहित किया गया है' मूल में वह 'समण' संज्ञा पद है। उसके संस्कृत छाया रूप तीन होते हैं-शमन, श्रमण और समण । श्रमणों-जैन साधुओं की चर्या इन तीनों विशेषताओं को लिये हुए होती है। जिन्होंने पञ्चेन्द्रियों को संवृत कर लिया है, कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो शत्रु-मित्र, दुःख-सुख, प्रशंसा-निन्दा, मिट्टी-सोना, तथा जीवन-मरण में समभाव सम्पन्न हैं और जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र की आराधना में निरन्तर तत्पर हैं, वे श्रमण हैं और उनका धर्म ही श्रमण धर्म है। वर्तमान में जिसे हम जैनधर्म या आत्मधर्म के नाम से सम्बोधित करते हैं, वह यही है। यह अखण्ड भाव से श्रमणसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है।
लोक में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनका लिखित या अलिखित दर्शन अवश्य होता है। श्रमण परम्परा का भी अपना दर्शन है, जिसके द्वारा श्रमण धर्म की नींव के रूप में व्यक्तिस्वातन्त्र्य की अक्षुण्णभाव से प्रतिष्ठा की गई है। इसे समझने के लिए इसमें प्रतिपादित तत्त्वप्ररूपणा को हृदयंगम कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसा कि समग्र आगम पर दृष्टिपात करने से विदित होता है, इसमें तत्त्वप्ररूपणा के दो प्रकार परिलक्षित होते हैं-एक लोक की संरचना के रूप में तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार और दूसरा मोक्षमार्ग की दृष्टि से तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार । ये दोनों ही एक दूसरे के इतने निकट हैं, जिससे इन्हें सर्वथा जुदा नहीं किया जा सकता, केवल प्रयोजन भेद से ही तत्त्वप्ररूपणा को दो भागों में विभक्त किया गया है।
प्रथम प्ररूपणा के अनुसार जाति की अपेक्षा द्रव्य छह हैं। वे अनादि, अनन्त और अकृत्रिम हैं । उन्हीं के समुच्चय का नाम लोक है। इसलिए जैनदर्शन में लोक
१. येषां च विरोधः शाश्वतिकः ( २।४।९ ) इत्यस्यावकाशः श्रमणब्राह्मणम् । पातञ्जलभाष्य । २. प्रवचनसार गा० २२६ । ३. पाइअसद्दमहण्णओ, देखो समण शब्द, द्वि० सं० पृ० ८६५ । ४, प्रवचनसार गा० २४०-२४१ ।
परिसंवाद-४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org