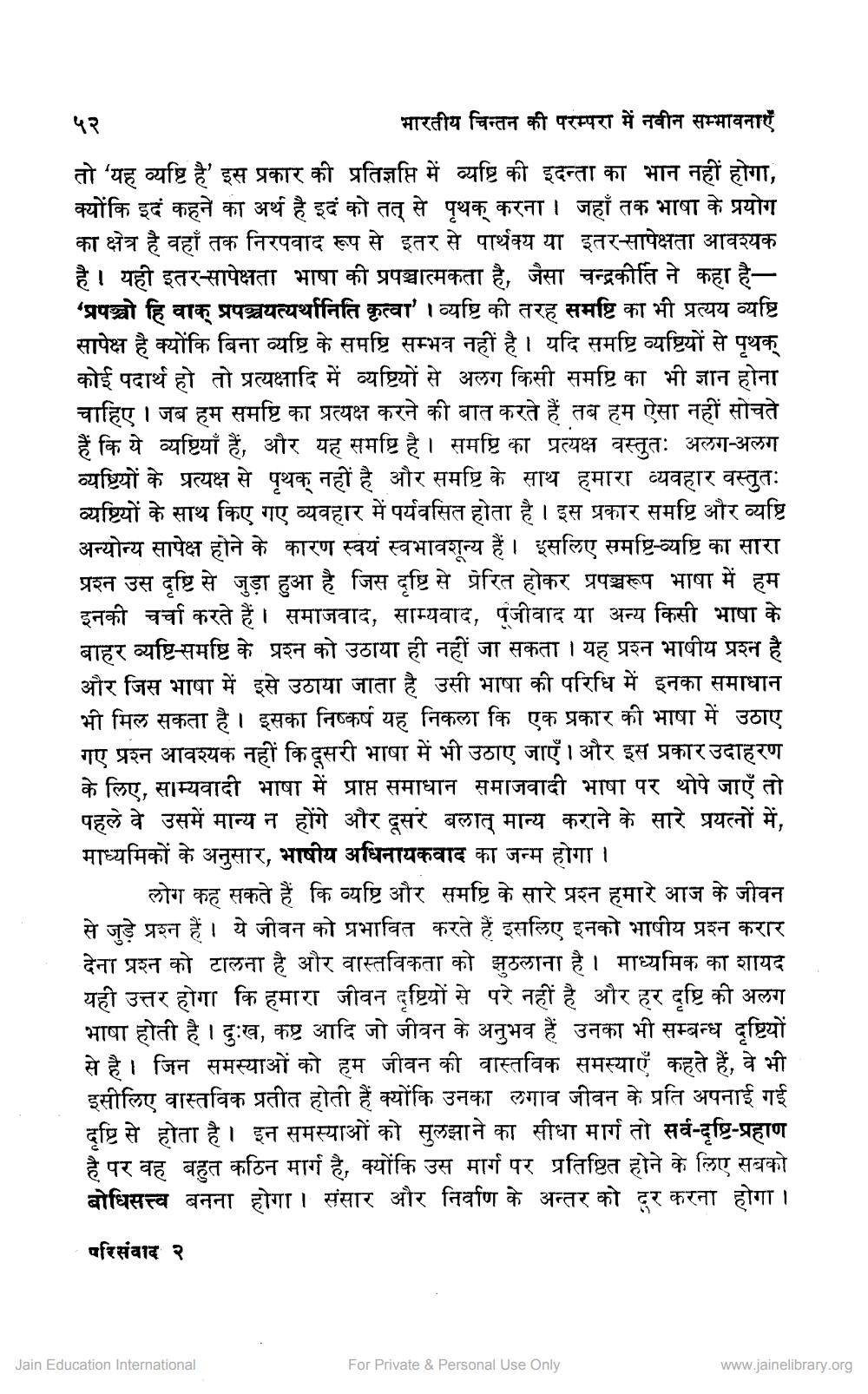________________
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं तो 'यह व्यष्टि है' इस प्रकार की प्रतिज्ञप्ति में व्यष्टि की इदन्ता का भान नहीं होगा, क्योंकि इदं कहने का अर्थ है इदं को तत् से पृथक् करना । जहाँ तक भाषा के प्रयोग का क्षेत्र है वहाँ तक निरपवाद रूप से इतर से पार्थक्य या इतर-सापेक्षता आवश्यक है। यही इतर-सापेक्षता भाषा की प्रपञ्चात्मकता है, जैसा चन्द्रकीर्ति ने कहा है'प्रपञ्चो हि वाक् प्रपञ्चयत्यानिति कृत्वा' । व्यष्टि की तरह समष्टि का भी प्रत्यय व्यष्टि सापेक्ष है क्योंकि बिना व्यष्टि के समष्टि सम्भव नहीं है। यदि समष्टि व्यष्टियों से पृथक् कोई पदार्थ हो तो प्रत्यक्षादि में व्यष्टियों से अलग किसी समष्टि का भी ज्ञान होना चाहिए । जब हम समष्टि का प्रत्यक्ष करने की बात करते हैं तब हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये व्यष्टियाँ हैं, और यह समष्टि है। समष्टि का प्रत्यक्ष वस्तुतः अलग-अलग व्यष्टियों के प्रत्यक्ष से पृथक् नहीं है और समष्टि के साथ हमारा व्यवहार वस्तुतः व्यष्टियों के साथ किए गए व्यवहार में पर्यवसित होता है । इस प्रकार समष्टि और व्यष्टि अन्योन्य सापेक्ष होने के कारण स्वयं स्वभावशून्य हैं। इसलिए समष्टि-व्यष्टि का सारा प्रश्न उस दृष्टि से जुड़ा हुआ है जिस दृष्टि से प्रेरित होकर प्रपञ्चरूप भाषा में हम इनकी चर्चा करते हैं। समाजवाद, साम्यवाद, पूजीवाद या अन्य किसी भाषा के बाहर व्यष्टि समष्टि के प्रश्न को उठाया ही नहीं जा सकता। यह प्रश्न भाषीय प्रश्न है और जिस भाषा में इसे उठाया जाता है उसी भाषा की परिधि में इनका समाधान भी मिल सकता है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि एक प्रकार की भाषा में उठाए गए प्रश्न आवश्यक नहीं कि दूसरी भाषा में भी उठाए जाएँ। और इस प्रकार उदाहरण के लिए, साम्यवादी भाषा में प्राप्त समाधान समाजवादी भाषा पर थोपे जाएँ तो पहले वे उसमें मान्य न होंगे और दूसरे बलात् मान्य कराने के सारे प्रयत्नों में, माध्यमिकों के अनुसार, भाषीय अधिनायकवाद का जन्म होगा।
लोग कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि के सारे प्रश्न हमारे आज के जीवन से जुड़े प्रश्न हैं। ये जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए इनको भाषीय प्रश्न करार देना प्रश्न को टालना है और वास्तविकता को झुठलाना है। माध्यमिक का शायद यही उत्तर होगा कि हमारा जीवन दृष्टियों से परे नहीं है और हर दृष्टि की अलग भाषा होती है । दुःख, कष्ट आदि जो जीवन के अनुभव हैं उनका भी सम्बन्ध दृष्टियों से है। जिन समस्याओं को हम जीवन की वास्तविक समस्याएँ कहते हैं, वे भी इसीलिए वास्तविक प्रतीत होती हैं क्योंकि उनका लगाव जीवन के प्रति अपनाई गई दृष्टि से होता है। इन समस्याओं को सुलझाने का सीधा मार्ग तो सर्व-दृष्टि-प्रहाण है पर वह बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि उस मार्ग पर प्रतिष्ठित होने के लिए सबको बोधिसत्त्व बनना होगा। संसार और निर्वाण के अन्तर को दूर करना होगा।
परिसंवाद २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org