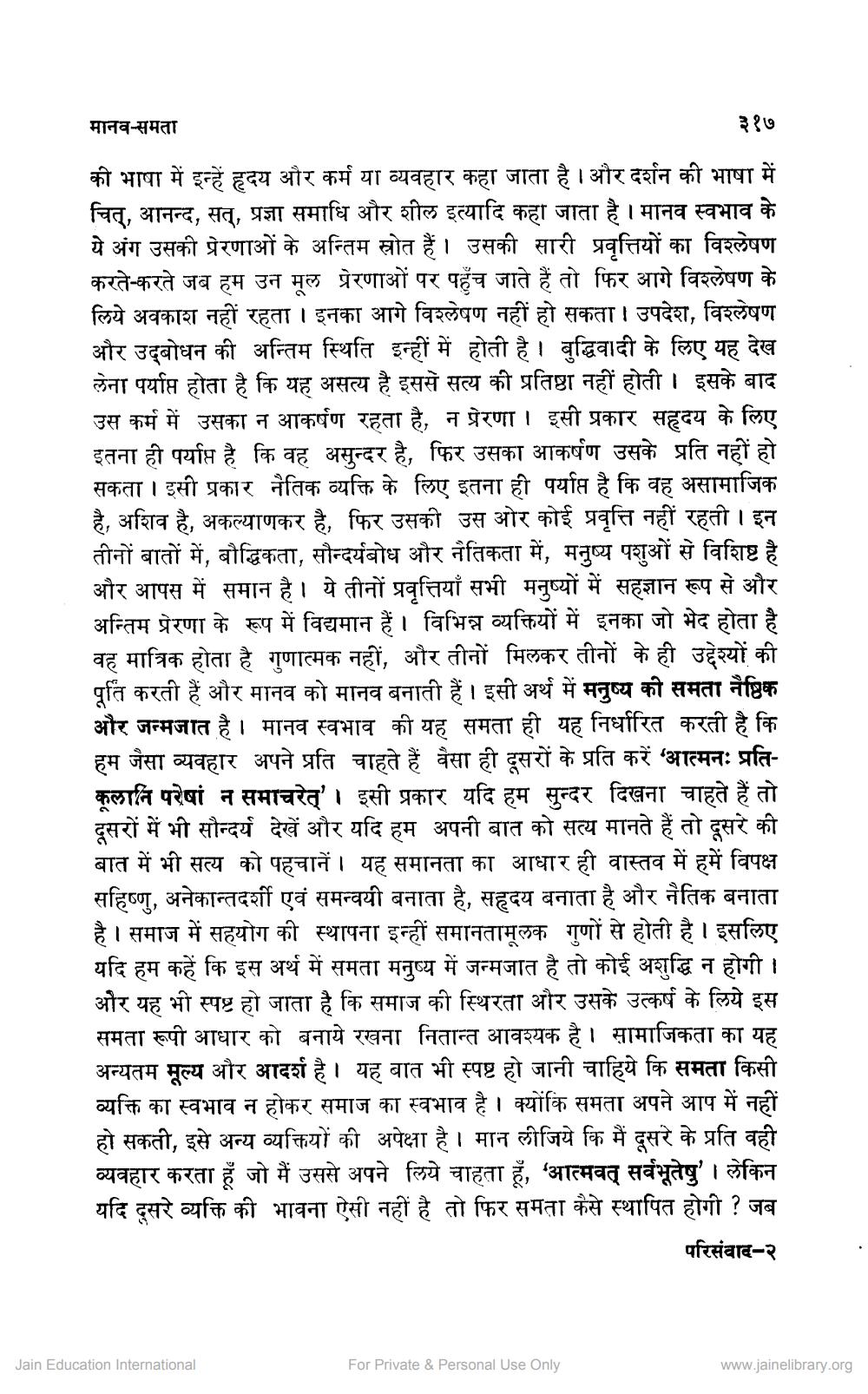________________
३१७
की भाषा में इन्हें हृदय और कर्म या व्यवहार कहा जाता है । और दर्शन की भाषा में चित्, आनन्द, सत्, प्रज्ञा समाधि और शील इत्यादि कहा जाता है । मानव स्वभाव के ये अंग उसकी प्रेरणाओं के अन्तिम स्रोत हैं । उसकी सारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते-करते जब हम उन मूल प्रेरणाओं पर पहुँच जाते हैं तो फिर आगे विश्लेषण के लिये अवकाश नहीं रहता । इनका आगे विश्लेषण नहीं हो सकता । उपदेश, विश्लेषण और उद्बोधन की अन्तिम स्थिति इन्हीं में होती है । बुद्धिवादी के लिए यह देख लेना पर्याप्त होता है कि यह असत्य है इससे सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती । इसके बाद उस कर्म में उसका न आकर्षण रहता है, न प्रेरणा । इसी प्रकार सहृदय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह असुन्दर है, फिर उसका आकर्षण उसके प्रति नहीं हो सकता । इसी प्रकार नैतिक व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह असामाजिक है, अशिव है, अकल्याणकर है, फिर उसकी उस ओर कोई प्रवृत्ति नहीं रहती । इन तीनों बातों में, बौद्धिकता, सौन्दर्यबोध और नैतिकता में, मनुष्य पशुओं से विशिष्ट है और आपस में समान है । ये तीनों प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्यों में सहज्ञान रूप से और अन्तिम प्रेरणा के रूप में विद्यमान हैं । विभिन्न व्यक्तियों में इनका जो भेद होता है वह मात्रिक होता है गुणात्मक नहीं, और तीनों मिलकर तीनों के ही उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और मानव को मानव बनाती हैं। इसी अर्थ में मनुष्य की समता नैष्ठिक और जन्मजात है । मानव स्वभाव की यह समता ही यह निर्धारित करती है कि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरों के प्रति करें 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' । इसी प्रकार यदि हम सुन्दर दिखना चाहते हैं तो दूसरों में भी सौन्दर्य देखें और यदि हम अपनी बात को सत्य मानते हैं तो दूसरे की बात में भी सत्य को पहचानें । यह समानता का आधार ही वास्तव में हमें विपक्ष सहिष्णु, अनेकान्तदर्शी एवं समन्वयी बनाता है, सहृदय बनाता है और नैतिक बनाता है । समाज में सहयोग की स्थापना इन्हीं समानतामूलक गुणों से होती है । इसलिए यदि हम कहें कि इस अर्थ में समता मनुष्य में जन्मजात है तो कोई अशुद्धि न होगी । और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज की स्थिरता और उसके उत्कर्ष के लिये इस समता रूपी आधार को बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । सामाजिकता का यह अन्यतम मूल्य और आदर्श है । यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिये कि समता किसी व्यक्ति का स्वभाव न होकर समाज का स्वभाव है । क्योंकि समता अपने आप में नहीं हो सकती, इसे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा है । मान लीजिये कि मैं दूसरे के प्रति वही व्यवहार करता हूँ जो मैं उससे अपने लिये चाहता हूँ, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' । लेकिन यदि दूसरे व्यक्ति की भावना ऐसी नहीं है तो फिर समता कैसे स्थापित होगी ? जब
परिसंवाद - २
मानव-समता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org