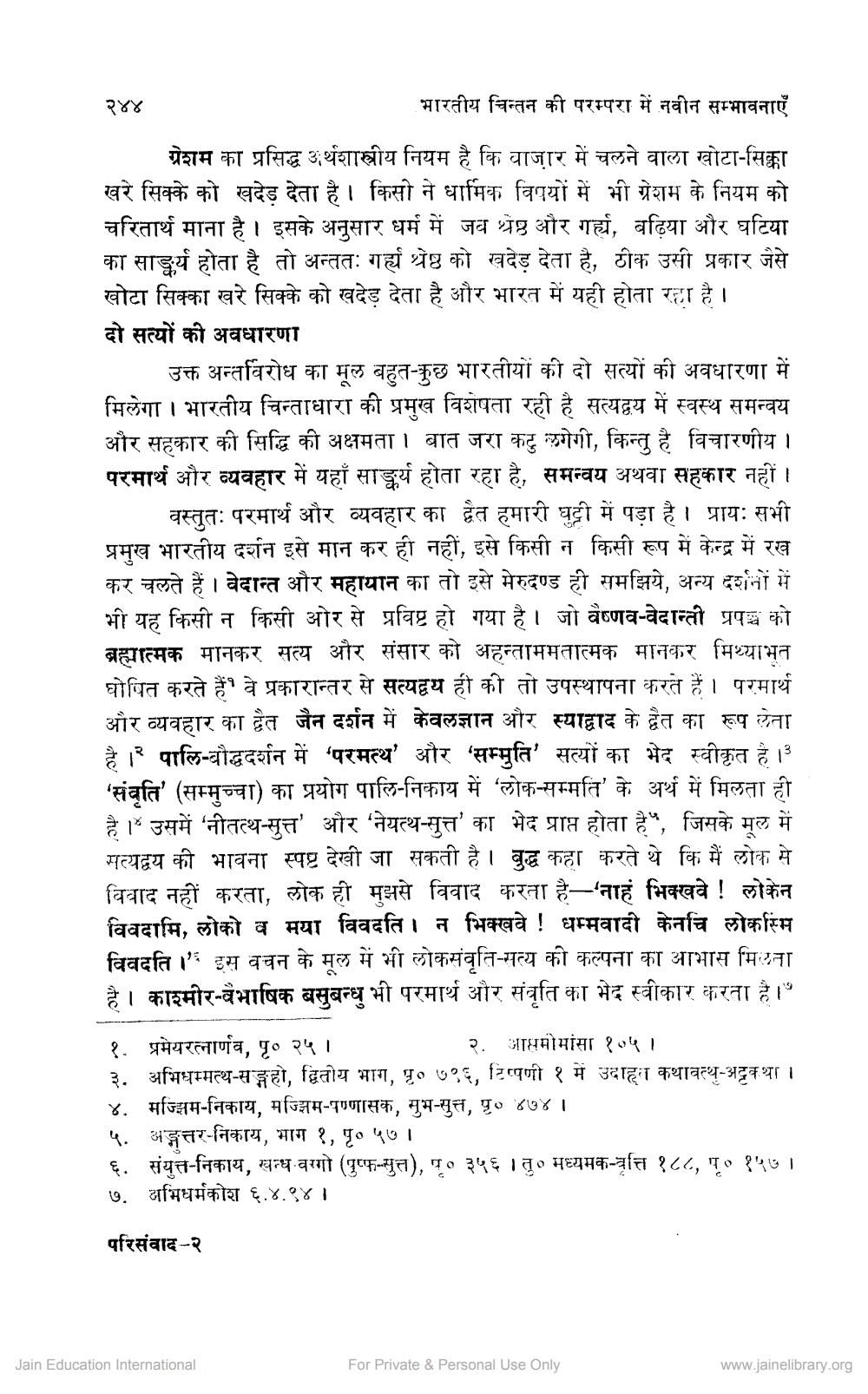________________
२४४
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ
ग्रेशम का प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय नियम है कि बाजार में चलने वाला खोटा-सिक्का खरे सिक्के को खदेड देता है। किसी ने धार्मिक विषयों में भी ग्रेशम के नियम को चरितार्थ माना है। इसके अनुसार धर्म में जब थेष्ठ और गर्दा, बढ़िया और घटिया का सार्य होता है तो अन्ततः गमु श्रेष्ठ को खदेड़ देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे खोटा सिक्का खरे सिक्के को खदेड़ देता है और भारत में यही होता रहा है । दो सत्यों की अवधारणा
उक्त अन्तविरोध का मूल बहुत-कुछ भारतीयों की दो सत्यों की अवधारणा में मिलेगा। भारतीय चिन्ताधारा की प्रमुख विशेषता रही है सत्यद्वय में स्वस्थ समन्वय
और सहकार की सिद्धि की अक्षमता। बात जरा कटु लगेगी, किन्तु है विचारणीय । परमार्थ और व्यवहार में यहाँ साङ्कर्य होता रहा है, समन्वय अथवा सहकार नहीं।
वस्तुतः परमार्थ और व्यवहार का द्वैत हमारी धुट्टी में पड़ा है। प्रायः सभी प्रमुख भारतीय दर्शन इसे मान कर ही नहीं, इसे किसी न किसी रूप में केन्द्र में रख कर चलते हैं । वेदान्त और महायान का तो इसे मेरुदण्ड ही समझिये, अन्य दर्शनों में भी यह किसी न किसी ओर से प्रविष्ट हो गया है। जो वैष्णव-वेदान्ती प्रपञ्च को ब्रह्मात्मक मानकर सत्य और संसार को अहन्ताममतात्मक मानकर मिथ्याभत घोषित करते हैं वे प्रकारान्तर से सत्यद्वय ही की तो उपस्थापना करते हैं। परमार्थ और व्यवहार का द्वैत जैन दर्शन में केवलज्ञान और स्याद्वाद के द्वैत का रूप लेता है ।२ पालि-बौद्धदर्शन में 'परमत्थ' और 'सम्मुति' सत्यों का भेद स्वीकृत है । 'संवृति' (सम्मुच्चा) का प्रयोग पालि-निकाय में 'लोक-सम्मति' के अर्थ में मिलता ही है। उसमें 'नीतत्थ-सुत्त' और 'नेयत्थ-सुत्त' का भेद प्राप्त होता है, जिसके मूल में सत्यद्वय की भावना स्पष्ट देखी जा सकती है। बुद्ध कहा करते थे कि मैं लोक से विवाद नहीं करता, लोक ही मुझसे विवाद करता है-'नाहं भिक्खवे ! लोकेन विवदामि, लोको व मया विवदति। न भिक्खवे ! धम्मवादी केनचि लोकस्मि विवदति । इस वचन के मूल में भी लोकसंवृति-सत्य की कल्पना का आभास मिलना है। काश्मीर-वैभाषिक बसुबन्धु भी परमार्थ और संवृति का भेद स्वीकार करता है। १. प्रमेयरत्नार्णव, पृ० २५ ।
२. आप्तमीमांसा १०५ । ३. अभिधम्मत्थ-सङ्गहो, द्वितीय भाग, पृ० ७९६, टिप्पणी १ में उदाहृत कथावत्थ-अट्टकथा । ४. मज्झिम-निकाय, मज्झिम-पण्णासक, सुभ-सुत्त, पृ० ४७४ । ५. अङ्गत्तर-निकाय, भाग १, पृ० ५७ । ६. संयुत्त-निकाय, खन्ध वरगो (पुप्फ-सुत्त), पृ० ३५६ । तु० मध्यमक-वृत्ति १८८, पृ० १५७ । ७. अभिधर्मकोश ६.४.९४ ।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org