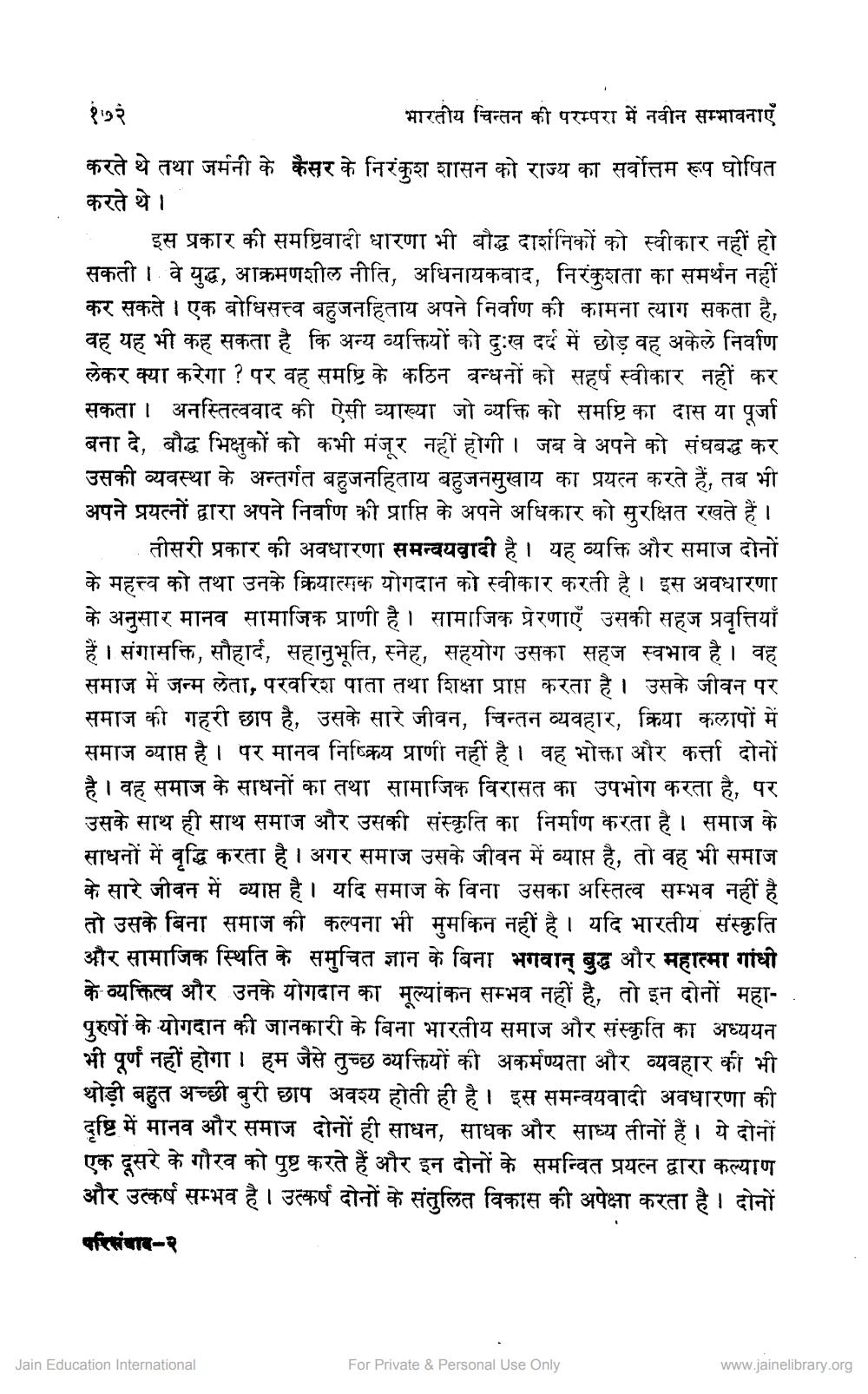________________
१७२
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ करते थे तथा जर्मनी के कैसर के निरंकुश शासन को राज्य का सर्वोत्तम रूप घोषित करते थे।
इस प्रकार की समष्टिवादी धारणा भी बौद्ध दार्शनिकों को स्वीकार नहीं हो सकती। वे युद्ध, आक्रमणशील नीति, अधिनायकवाद, निरंकुशता का समर्थन नहीं कर सकते । एक बोधिसत्त्व बहुजनहिताय अपने निर्वाण की कामना त्याग सकता है, वह यह भी कह सकता है कि अन्य व्यक्तियों को दुःख दर्द में छोड़ वह अकेले निर्वाण लेकर क्या करेगा ? पर वह समष्टि के कठिन बन्धनों को सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकता। अनस्तित्ववाद की ऐसी व्याख्या जो व्यक्ति को समष्टि का दास या पूर्जा बना दे, बौद्ध भिक्षुकों को कभी मंजूर नहीं होगी। जब वे अपने को संघबद्ध कर उसकी व्यवस्था के अन्तर्गत बहुजनहिताय बहुजनसुखाय का प्रयत्न करते हैं, तब भी अपने प्रयत्नों द्वारा अपने निर्वाण की प्राप्ति के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।
तीसरी प्रकार की अवधारणा समन्वयवादी है। यह व्यक्ति और समाज दोनों के महत्त्व को तथा उनके क्रियात्मक योगदान को स्वीकार करती है। इस अवधारणा के अनुसार मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्रेरणाएँ उसकी सहज प्रवृत्तियाँ हैं। संगासक्ति, सौहार्द, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग उसका सहज स्वभाव है। वह समाज में जन्म लेता, परवरिश पाता तथा शिक्षा प्राप्त करता है। उसके जीवन पर समाज की गहरी छाप है, उसके सारे जीवन, चिन्तन व्यवहार, क्रिया कलापों में समाज व्याप्त है। पर मानव निष्क्रिय प्राणी नहीं है। वह भोक्ता और कर्ता दोनों है। वह समाज के साधनों का तथा सामाजिक विरासत का उपभोग करता है, पर उसके साथ ही साथ समाज और उसकी संस्कृति का निर्माण करता है। समाज के साधनों में वृद्धि करता है । अगर समाज उसके जीवन में व्याप्त है, तो वह भी समाज के सारे जीवन में व्याप्त है। यदि समाज के विना उसका अस्तित्व सम्भव नहीं है तो उसके बिना समाज की कल्पना भी मुमकिन नहीं है। यदि भारतीय संस्कृति और सामाजिक स्थिति के समुचित ज्ञान के बिना भगवान् बुद्ध और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके योगदान का मूल्यांकन सम्भव नहीं है, तो इन दोनों महापुरुषों के योगदान की जानकारी के बिना भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन भी पूर्ण नहीं होगा। हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों की अकर्मण्यता और व्यवहार की भी थोड़ी बहुत अच्छी बुरी छाप अवश्य होती ही है। इस समन्वयवादी अवधारणा की दृष्टि में मानव और समाज दोनों ही साधन, साधक और साध्य तीनों हैं। ये दोनों एक दूसरे के गौरव को पुष्ट करते हैं और इन दोनों के समन्वित प्रयत्न द्वारा कल्याण और उत्कर्ष सम्भव है । उत्कर्ष दोनों के संतुलित विकास की अपेक्षा करता है। दोनों परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org