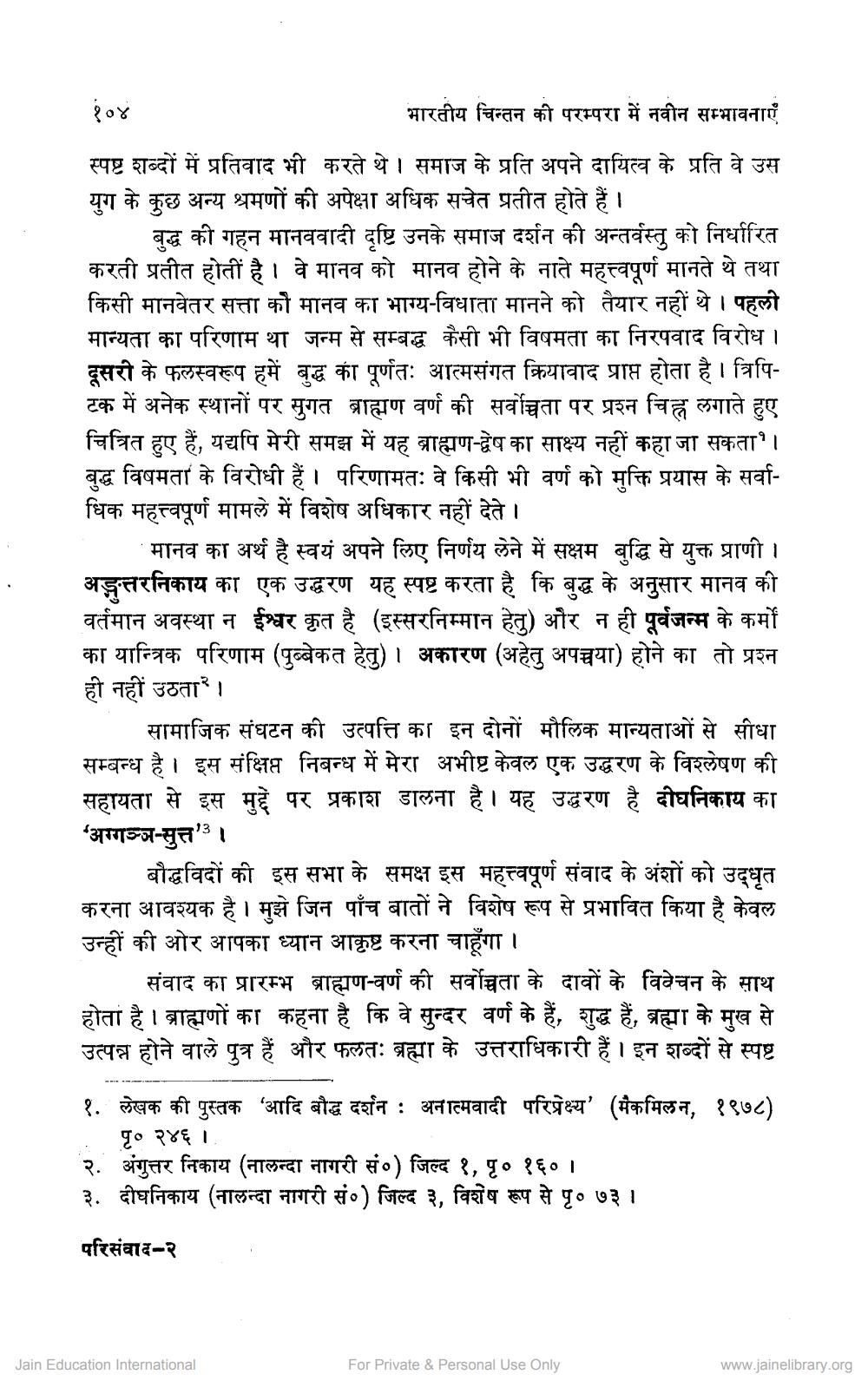________________
१०४
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं स्पष्ट शब्दों में प्रतिवाद भी करते थे। समाज के प्रति अपने दायित्व के प्रति वे उस युग के कुछ अन्य श्रमणों की अपेक्षा अधिक सचेत प्रतीत होते हैं ।
बुद्ध की गहन मानववादी दृष्टि उनके समाज दर्शन की अन्तर्वस्तु को निर्धारित करती प्रतीत होती है। वे मानव को मानव होने के नाते महत्त्वपूर्ण मानते थे तथा किसी मानवेतर सत्ता को मानव का भाग्य-विधाता मानने को तैयार नहीं थे । पहली मान्यता का परिणाम था जन्म से सम्बद्ध कैसी भी विषमता का निरपवाद विरोध । दूसरी के फलस्वरूप हमें बुद्ध का पूर्णतः आत्मसंगत क्रियावाद प्राप्त होता है । त्रिपिटक में अनेक स्थानों पर सुगत ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए चित्रित हए हैं, यद्यपि मेरी समझ में यह ब्राह्मण-द्वेष का साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। बुद्ध विषमता के विरोधी हैं। परिणामतः वे किसी भी वर्ण को मुक्ति प्रयास के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मामले में विशेष अधिकार नहीं देते।
मानव का अर्थ है स्वयं अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम बुद्धि से युक्त प्राणी। अङ्गत्तरनिकाय का एक उद्धरण यह स्पष्ट करता है कि बुद्ध के अनुसार मानव की वर्तमान अवस्था न ईश्वर कृत है (इस्सरनिम्मान हेतु) और न ही पूर्वजन्म के कर्मों का यान्त्रिक परिणाम (पुब्बेकत हेतु)। अकारण (अहेतु अपच्चया) होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
सामाजिक संघटन की उत्पत्ति का इन दोनों मौलिक मान्यताओं से सीधा सम्बन्ध है। इस संक्षिप्त निबन्ध में मेरा अभीष्ट केवल एक उद्धरण के विश्लेषण की सहायता से इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है। यह उद्धरण है दीघनिकाय का 'अग्गा -सुत्त'।
बौद्धविदों की इस सभा के समक्ष इस महत्त्वपूर्ण संवाद के अंशों को उद्धृत करना आवश्यक है। मुझे जिन पाँच बातों ने विशेष रूप से प्रभावित किया है केवल उन्हीं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
संवाद का प्रारम्भ ब्राह्मण-वर्ण की सर्वोच्चता के दावों के विवेचन के साथ होता है। ब्राह्मणों का कहना है कि वे सुन्दर वर्ण के हैं, शुद्ध हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं और फलतः ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। इन शब्दों से स्पष्ट
१. लेखक की पुस्तक 'आदि बौद्ध दर्शन : अनात्मवादी परिप्रेक्ष्य' (मैकमिलन, १९७८) . पृ० २४६ । २. अंगुत्तर निकाय (नालन्दा नागरी सं०) जिल्द १, पृ० १६० । ३. दीघनिकाय (नालन्दा नागरी सं०) जिल्द ३, विशेष रूप से पृ० ७३ ।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org