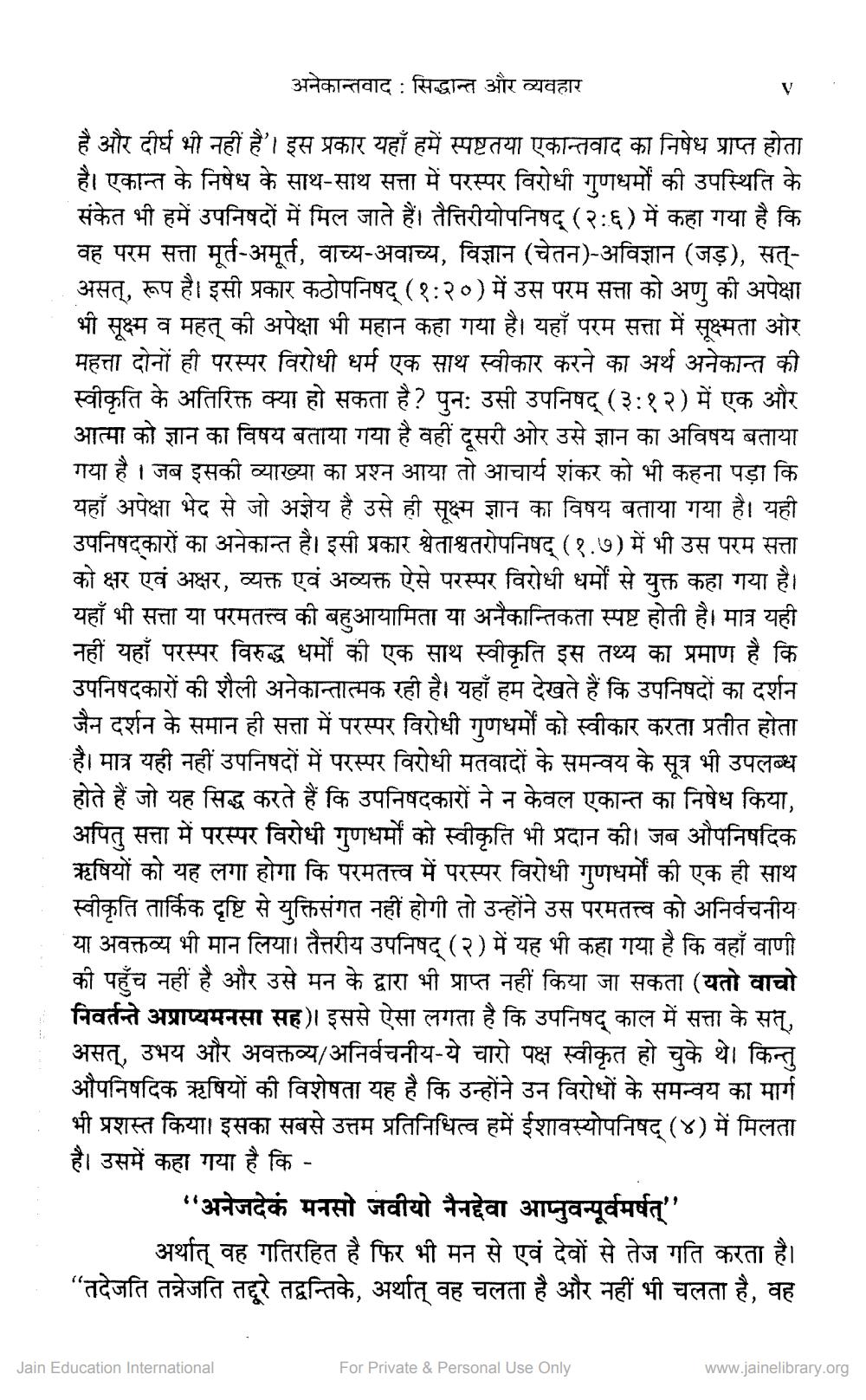________________
अनेकान्तवाद : सिद्धान्त और व्यवहार
है और दीर्घ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ हमें स्पष्टतया एकान्तवाद का निषेध प्राप्त होता है। एकान्त के निषेध के साथ-साथ सत्ता में परस्पर विरोधी गुणधर्मों की उपस्थिति के संकेत भी हमें उपनिषदों में मिल जाते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् (२:६) में कहा गया है कि वह परम सत्ता मूर्त-अमर्त, वाच्य-अवाच्य, विज्ञान (चेतन)-अविज्ञान (जड़), सतअसत्, रूप है। इसी प्रकार कठोपनिषद् (१:२०) में उस परम सत्ता को अणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म व महत् की अपेक्षा भी महान कहा गया है। यहाँ परम सत्ता में सूक्ष्मता ओर महत्ता दोनों ही परस्पर विरोधी धर्म एक साथ स्वीकार करने का अर्थ अनेकान्त की स्वीकृति के अतिरिक्त क्या हो सकता है? पुन: उसी उपनिषद् (३:१२) में एक और आत्मा को ज्ञान का विषय बताया गया है वहीं दूसरी ओर उसे ज्ञान का अविषय बताया गया है । जब इसकी व्याख्या का प्रश्न आया तो आचार्य शंकर को भी कहना पड़ा कि यहाँ अपेक्षा भेद से जो अज्ञेय है उसे ही सूक्ष्म ज्ञान का विषय बताया गया है। यही उपनिषदकारों का अनेकान्त है। इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद् (१.७) में भी उस परम सत्ता को क्षर एवं अक्षर, व्यक्त एवं अव्यक्त ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त कहा गया है। यहाँ भी सत्ता या परमतत्त्व की बहआयामिता या अनैकान्तिकता स्पष्ट होती है। मात्र यही नहीं यहाँ परस्पर विरुद्ध धर्मों की एक साथ स्वीकृति इस तथ्य का प्रमाण है कि उपनिषदकारों की शैली अनेकान्तात्मक रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उपनिषदों का दर्शन जैन दर्शन के समान ही सत्ता में परस्पर विरोधी गुणधर्मों को स्वीकार करता प्रतीत होता है। मात्र यही नहीं उपनिषदों में परस्पर विरोधी मतवादों के समन्वय के सूत्र भी उपलब्ध होते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि उपनिषदकारों ने न केवल एकान्त का निषेध किया, अपितु सत्ता में परस्पर विरोधी गणधर्मों को स्वीकृति भी प्रदान की। जब औपनिषदिक ऋषियों को यह लगा होगा कि परमतत्त्व में परस्पर विरोधी गुणधर्मों की एक ही साथ स्वीकृति तार्किक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं होगी तो उन्होंने उस परमतत्त्व को अनिर्वचनीय या अवक्तव्य भी मान लिया। तैत्तरीय उपनिषद् (२) में यह भी कहा गया है कि वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है और उसे मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता (यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह)। इससे ऐसा लगता है कि उपनिषद् काल में सत्ता के सत्, असत, उभय और अवक्तव्य/अनिर्वचनीय-ये चारो पक्ष स्वीकृत हो चुके थे। किन्त औपनिषदिक ऋषियों की विशेषता यह है कि उन्होंने उन विरोधों के समन्वय का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसका सबसे उत्तम प्रतिनिधित्व हमें ईशावस्योपनिषद् (४) में मिलता है। उसमें कहा गया है कि -
___ "अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्"
अर्थात् वह गतिरहित है फिर भी मन से एवं देवों से तेज गति करता है। "तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके, अर्थात् वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org