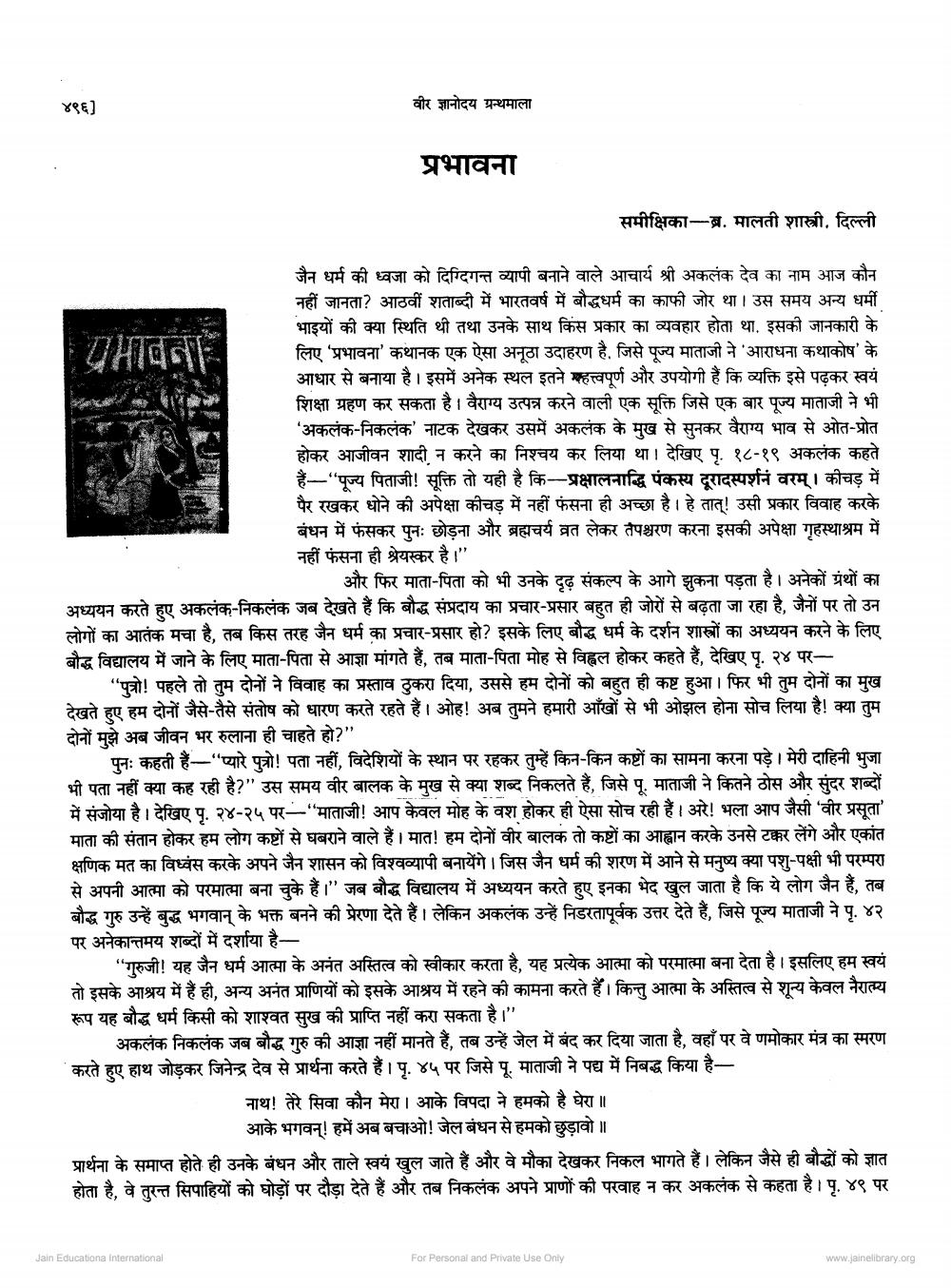________________
४९६]
वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला
प्रभावना
समीक्षिका-ब्र. मालती शास्त्री, दिल्ली
प्रमावताः
जैन धर्म की ध्वजा को दिग्दिगन्त व्यापी बनाने वाले आचार्य श्री अकलंक देव का नाम आज कौन नहीं जानता? आठवीं शताब्दी में भारतवर्ष में बौद्धधर्म का काफी जोर था। उस समय अन्य धर्मी भाइयों की क्या स्थिति थी तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था. इसकी जानकारी के लिए 'प्रभावना' कथानक एक ऐसा अनूठा उदाहरण है, जिसे पूज्य माताजी ने 'आराधना कथाकोष' के
आधार से बनाया है। इसमें अनेक स्थल इतने छहत्त्वपूर्ण और उपयोगी हैं कि व्यक्ति इसे पढ़कर स्वयं शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वैराग्य उत्पन्न करने वाली एक सूक्ति जिसे एक बार पूज्य माताजी ने भी 'अकलंक-निकलंक' नाटक देखकर उसमें अकलंक के मुख से सुनकर वैराग्य भाव से ओत-प्रोत होकर आजीवन शादी न करने का निश्चय कर लिया था। देखिए पृ. १८-१९ अकलंक कहते हैं-"पूज्य पिताजी! सूक्ति तो यही है कि-प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्। कीचड़ में पैर रखकर धोने की अपेक्षा कीचड़ में नहीं फंसना ही अच्छा है। हे तात्! उसी प्रकार विवाह करके बंधन में फंसकर पुनः छोड़ना और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तपश्चरण करना इसकी अपेक्षा गृहस्थाश्रम में नहीं फंसना ही श्रेयस्कर है।"
और फिर माता-पिता को भी उनके दृढ़ संकल्प के आगे झुकना पड़ता है। अनेकों ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अकलंक-निकलंक जब देखते हैं कि बौद्ध संप्रदाय का प्रचार-प्रसार बहुत ही जोरों से बढ़ता जा रहा है, जैनों पर तो उन लोगों का आतंक मचा है, तब किस तरह जैन धर्म का प्रचार-प्रसार हो? इसके लिए बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बौद्ध विद्यालय में जाने के लिए माता-पिता से आज्ञा मांगते हैं, तब माता-पिता मोह से विह्वल होकर कहते हैं, देखिए पृ. २४ पर
“पुत्रो! पहले तो तुम दोनों ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, उससे हम दोनों को बहुत ही कष्ट हुआ। फिर भी तुम दोनों का मुख देखते हुए हम दोनों जैसे-तैसे संतोष को धारण करते रहते हैं। ओह! अब तुमने हमारी आँखों से भी ओझल होना सोच लिया है! क्या तुम दोनों मुझे अब जीवन भर रुलाना ही चाहते हो?"
पुनः कहती हैं-"प्यारे पुत्रो! पता नहीं, विदेशियों के स्थान पर रहकर तुम्हें किन-किन कष्टों का सामना करना पड़े। मेरी दाहिनी भुजा भी पता नहीं क्या कह रही है?" उस समय वीर बालक के मुख से क्या शब्द निकलते हैं, जिसे पू. माताजी ने कितने ठोस और सुंदर शब्दों में संजोया है। देखिए पृ. २४-२५ पर-"माताजी! आप केवल मोह के वश होकर ही ऐसा सोच रही हैं। अरे! भला आप जैसी 'वीर प्रसूता' माता की संतान होकर हम लोग कष्टों से घबराने वाले हैं। मात! हम दोनों वीर बालक तो कष्टों का आह्वान करके उनसे टक्कर लेंगे और एकांत क्षणिक मत का विध्वंस करके अपने जैन शासन को विश्वव्यापी बनायेंगे। जिस जैन धर्म की शरण में आने से मनुष्य क्या पशु-पक्षी भी परम्परा से अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं।" जब बौद्ध विद्यालय में अध्ययन करते हुए इनका भेद खुल जाता है कि ये लोग जैन हैं, तब बौद्ध गुरु उन्हें बुद्ध भगवान् के भक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अकलंक उन्हें निडरतापूर्वक उत्तर देते हैं, जिसे पूज्य माताजी ने पृ. ४२ पर अनेकान्तमय शब्दों में दर्शाया है
"गुरुजी! यह जैन धर्म आत्मा के अनंत अस्तित्व को स्वीकार करता है, यह प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बना देता है। इसलिए हम स्वयं तो इसके आश्रय में हैं ही, अन्य अनंत प्राणियों को इसके आश्रय में रहने की कामना करते हैं। किन्तु आत्मा के अस्तित्व से शून्य केवल नैरात्म्य रूप यह बौद्ध धर्म किसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता है।"
अकलंक निकलंक जब बौद्ध गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, तब उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर वे णमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते हैं। पृ. ४५ पर जिसे पू. माताजी ने पद्य में निबद्ध किया है
नाथ! तेरे सिवा कौन मेरा। आके विपदा ने हमको है घेरा ॥
आके भगवन्! हमें अब बचाओ! जेल बंधन से हमको छुड़ावो॥ प्रार्थना के समाप्त होते ही उनके बंधन और ताले स्वयं खुल जाते हैं और वे मौका देखकर निकल भागते हैं। लेकिन जैसे ही बौद्धों को ज्ञात होता है, वे तुरन्त सिपाहियों को घोड़ों पर दौड़ा देते हैं और तब निकलंक अपने प्राणों की परवाह न कर अकलंक से कहता है। पृ. ४९ पर
Jain Educationa international
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org