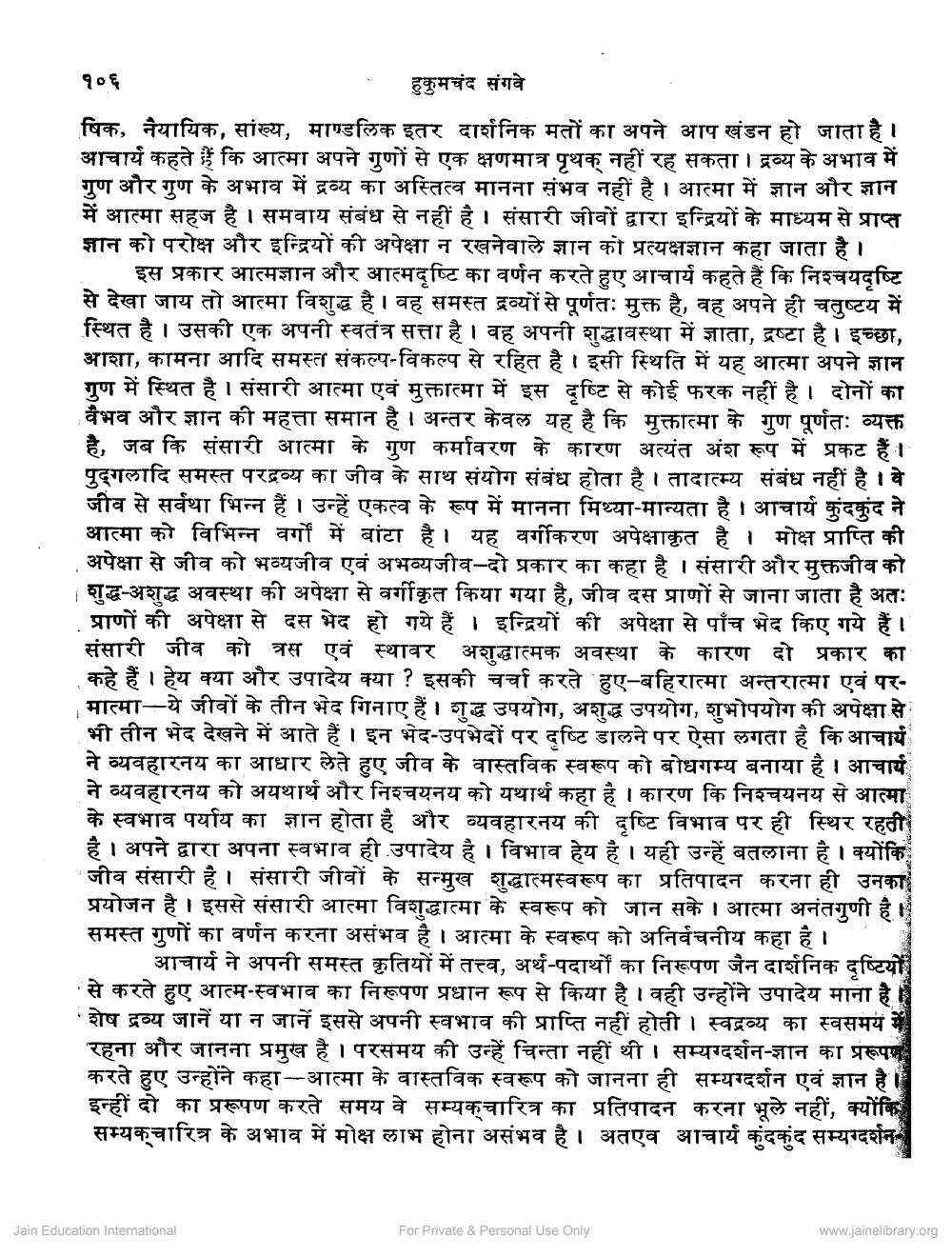________________
-
हुकुमचंद संगवे
षिक, नैयायिक, सांख्य, माण्डलिक इतर दार्शनिक मतों का अपने आप खंडन हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा अपने गुणों से एक क्षणमात्र पृथक् नहीं रह सकता। द्रव्य के अभाव में गुण और गुण के अभाव में द्रव्य का अस्तित्व मानना संभव नहीं है । आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में आत्मा सहज है । समवाय संबंध से नहीं है। संसारी जीवों द्वारा इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को परोक्ष और इन्द्रियों की अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है।
इस प्रकार आत्मज्ञान और आत्मदृष्टि का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि निश्चयदृष्टि से देखा जाय तो आत्मा विशुद्ध है । वह समस्त द्रव्यों से पूर्णतः मुक्त है, वह अपने ही चतुष्टय में स्थित है । उसकी एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वह अपनी शुद्धावस्था में ज्ञाता, द्रष्टा है। इच्छा, आशा, कामना आदि समस्त संकल्प-विकल्प से रहित है । इसी स्थिति में यह आत्मा अपने ज्ञान गुण में स्थित है । संसारी आत्मा एवं मुक्तात्मा में इस दृष्टि से कोई फरक नहीं है। दोनों का वैभव और ज्ञान की महत्ता समान है। अन्तर केवल यह है कि मुक्तात्मा के गुण पूर्णतः व्यक्त है, जब कि संसारी आत्मा के गुण कर्मावरण के कारण अत्यंत अंश रूप में प्रकट हैं। पुद्गलादि समस्त परद्रव्य का जीव के साथ संयोग संबंध होता है। तादात्म्य संबंध नहीं है । वे जीव से सर्वथा भिन्न हैं। उन्हें एकत्व के रूप में मानना मिथ्या-मान्यता है । आचार्य कुंदकुंद ने आत्मा को विभिन्न वर्गों में बांटा है। यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत है । मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा से जीव को भव्यजीव एवं अभव्यजीव-दो प्रकार का कहा है । संसारी और मुक्तजीव को शुद्ध-अशुद्ध अवस्था की अपेक्षा से वर्गीकृत किया गया है, जीव दस प्राणों से जाना जाता है अतः प्राणों की अपेक्षा से दस भेद हो गये हैं । इन्द्रियों की अपेक्षा से पाँच भेद किए गये हैं। संसारी जीव को त्रस एवं स्थावर अशुद्धात्मक अवस्था के कारण दो प्रकार का कहे हैं। हेय क्या और उपादेय क्या ? इसकी चर्चा करते हए-बहिरात्मा अन्तरात्मा एवं परमात्मा-ये जीवों के तीन भेद गिनाए हैं। शद्ध उपयोग. अशद्ध उपयोग, शभोपयोग की अपेक्षा से भी तीन भेद देखने में आते हैं। इन भेद-उपभेदों पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है कि आचार्य ने व्यवहारनय का आधार लेते हुए जीव के वास्तविक स्वरूप को बोधगम्य बनाया है । आचार्य ने व्यवहारनय को अयथार्थ और निश्चयनय को यथार्थ कहा है । कारण कि निश्चयनय से आत्मा के स्वभाव पर्याय का ज्ञान होता है और व्यवहारनय की दृष्टि विभाव पर ही स्थिर रहती है। अपने द्वारा अपना स्वभाव ही उपादेय है। विभाव हेय है । यही उन्हें बतलाना है। क्योंकि जीव संसारी है। संसारी जीवों के सन्मुख शुद्धात्मस्वरूप का प्रतिपादन करना ही उनका प्रयोजन है। इससे संसारी आत्मा विशुद्धात्मा के स्वरूप को जान सके । आत्मा अनंतगुणी है।। समस्त गुणों का वर्णन करना असंभव है । आत्मा के स्वरूप को अनिर्वचनीय कहा है।
आचार्य ने अपनी समस्त कृतियों में तत्त्व, अर्थ-पदार्थों का निरूपण जैन दार्शनिक दृष्टियों से करते हुए आत्म-स्वभाव का निरूपण प्रधान रूप से किया है । वही उन्होंने उपादेय माना है ।। 'शेष द्रव्य जानें या न जानें इससे अपनी स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। स्वद्रव्य का स्वसमय में रहना और जानना प्रमुख है। परसमय की उन्हें चिन्ता नहीं थी। सम्यग्दर्शन-ज्ञान का प्ररूपण करते हुए उन्होंने कहा-आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही सम्यग्दर्शन एवं ज्ञान है ।। इन्हीं दो का प्ररूपण करते समय वे सम्यक्चारित्र का प्रतिपादन करना भूले नहीं, क्योंकि सम्यक्चारित्र के अभाव में मोक्ष लाभ होना असंभव है। अतएव आचार्य कुंदकुंद सम्यग्दर्शन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org