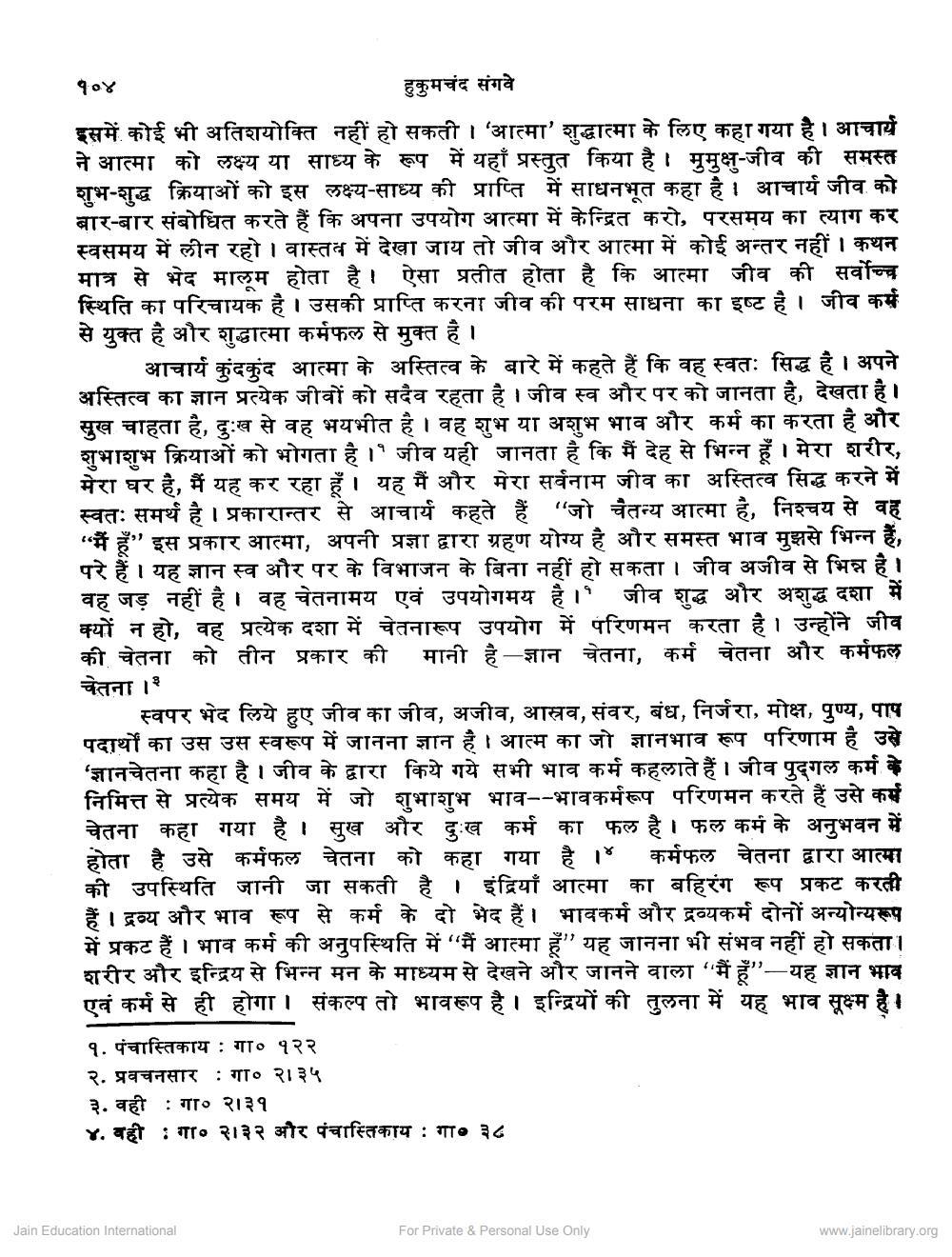________________
१०४
हुकुमचंद संगवे
इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती । 'आत्मा' शुद्धात्मा के लिए कहा गया है। आचार्य ने आत्मा को लक्ष्य या साध्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। मुमुक्ष-जीव की समस्त शुभ-शुद्ध क्रियाओं को इस लक्ष्य-साध्य की प्राप्ति में साधनभूत कहा है। आचार्य जीव को बार-बार संबोधित करते हैं कि अपना उपयोग आत्मा में केन्द्रित करो, परसमय का त्याग कर स्वसमय में लीन रहो । वास्तव में देखा जाय तो जीव और आत्मा में कोई अन्तर नहीं । कथन मात्र से भेद मालम होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा जीव की सर्वोच्च स्थिति का परिचायक है। उसकी प्राप्ति करना जीव की परम साधना का इष्ट है। जीव कर्म से युक्त है और शुद्धात्मा कर्मफल से मुक्त है।
आचार्य कुंदकुंद आत्मा के अस्तित्व के बारे में कहते हैं कि वह स्वतः सिद्ध है । अपने अस्तित्व का ज्ञान प्रत्येक जीवों को सदैव रहता है । जीव स्व और पर को जानता है, देखता है। सुख चाहता है, दुःख से वह भयभीत है । वह शुभ या अशुभ भाव और कर्म का करता है और शुभाशुभ क्रियाओं को भोगता है।' जीव यही जानता है कि मैं देह से भिन्न हूँ। मेरा शरीर, मेरा घर है, मैं यह कर रहा हूँ। यह मैं और मेरा सर्वनाम जीव का अस्तित्व सिद्ध करने में स्वतः समर्थ है । प्रकारान्तर से आचार्य कहते हैं "जो चैतन्य आत्मा है, निश्चय से वह "मैं हूँ" इस प्रकार आत्मा, अपनी प्रज्ञा द्वारा ग्रहण योग्य है और समस्त भाव मुझसे भिन्न हैं, परे हैं । यह ज्ञान स्व और पर के विभाजन के बिना नहीं हो सकता। जीव अजीव से भिन्न है। वह जड़ नहीं है। वह चेतनामय एवं उपयोगमय है।' जीव शुद्ध और अशुद्ध दशा में क्यों न हो, वह प्रत्येक दशा में चेतनारूप उपयोग में परिणमन करता है। उन्होंने जीव की चेतना को तीन प्रकार की मानी है—ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना।
स्वपर भेद लिये हुए जीव का जीव, अजीव, आस्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप पदार्थों का उस उस स्वरूप में जानना ज्ञान है। आत्म का जो ज्ञानभाव रूप परिणाम है उसे 'ज्ञानचेतना कहा है । जीव के द्वारा किये गये सभी भाव कर्म कहलाते हैं । जीव पुद्गल कर्म के निमित्त से प्रत्येक समय में जो शुभाशुभ भाव--भावकर्मरूप परिणमन करते हैं उसे कर्म चेतना कहा गया है। सुख और दुःख कर्म का फल है। फल कर्म के अनुभवन में होता है उसे कर्मफल चेतना को कहा गया है ।४ कर्मफल चेतना द्वारा आत्मा की उपस्थिति जानी जा सकती है । इंद्रियाँ आत्मा का बहिरंग रूप प्रकट करती हैं । द्रव्य और भाव रूप से कर्म के दो भेद हैं। भावकर्म और द्रव्यकर्म दोनों अन्योन्यरूप में प्रकट हैं । भाव कर्म की अनुपस्थिति में "मैं आत्मा हूँ" यह जानना भी संभव नहीं हो सकता। शरीर और इन्द्रिय से भिन्न मन के माध्यम से देखने और जानने वाला “मैं हूँ”—यह ज्ञान भाव एवं कर्म से ही होगा। संकल्प तो भावरूप है। इन्द्रियों की तुलना में यह भाव सूक्ष्म है। १. पंचास्तिकाय : गा० १२२ २. प्रवचनसार : गा० २।३५ ३. वही : गा० २।३१ ४. वही : गा० २।३२ और पंचास्तिकाय : गा० ३८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org