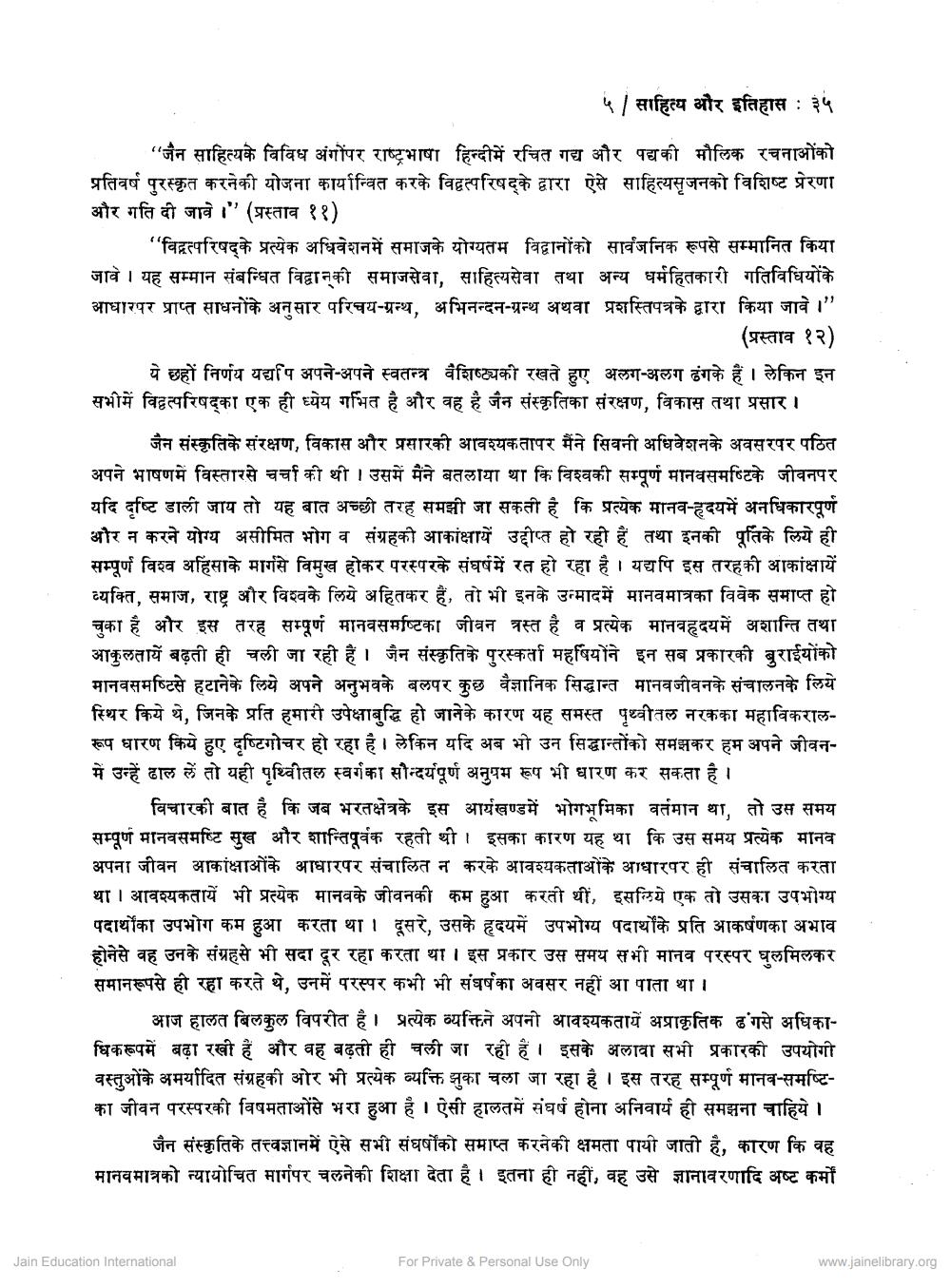________________
५ / साहित्य और इतिहास : ३५
"जैन साहित्य के विविध अंगोंपर राष्ट्रभाषा हिन्दीमें रचित गद्य और पद्यकी मौलिक रचनाओंको प्रतिवर्ष पुरस्कृत करने की योजना कार्यान्वित करके विद्वत्परिषद्के द्वारा ऐसे साहित्यसृजनको विशिष्ट प्रेरणा और गति दी जावे । " ( प्रस्ताव ११ )
"विद्वत्परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन में समाजके योग्यतम विद्वानोंको सार्वजनिक रूपसे सम्मानित किया जावे | यह सम्मान संबन्धित विद्वान्की समाजसेवा, साहित्यसेवा तथा अन्य धर्महितकारी गतिविधियों के आधारपर प्राप्त साधनोंके अनुसार परिचय-ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ अथवा प्रशस्तिपत्रके द्वारा किया जावे।" ( प्रस्ताव १२ ) अलग-अलग ढंगके हैं । लेकिन इन
ये छहों निर्णय यद्यपि अपने-अपने स्वतन्त्र वैशिष्ट्यकी रखते हुए सभी में विद्वत्परिषद्का एक ही ध्येय गर्भित है और वह है जैन संस्कृतिका संरक्षण, विकास तथा प्रसार ।
जैन संस्कृतिके संरक्षण, विकास और प्रसारकी आवश्यकतापर मैंने सिवनी अधिवेशन के अवसरपर पठित अपने भाषण में विस्तार से चर्चा की थी । उसमें मैंने बतलाया था कि विश्वकी सम्पूर्ण मानवसमष्टिके जीवनपर यदि दृष्टि डाली जाय तो यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि प्रत्येक मानव-हृदयमें अनधिकारपूर्ण और न करने योग्य असीमित भोग व संग्रहकी आकांक्षायें उद्दीप्त हो रही हैं तथा इनकी पूर्तिके लिये ही सम्पूर्ण विश्व अहिंसा मार्गसे विमुख होकर परस्परके संघर्ष में रत हो रहा है । यद्यपि इस तरह की आकांक्षायें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्वके लिये अहितकर हैं, तो भी इनके उन्मादमें मानवमात्रका विवेक समाप्त हो चुका है और इस तरह सम्पूर्ण मानवसर्माष्टका जीवन त्रस्त है व प्रत्येक मानवहृदय में अशान्ति तथा आकुलतायें बढ़ती ही चली जा रही हैं । जैन संस्कृतिके पुरस्कर्ता महर्षियोंने इन सब प्रकारको बुराईयों को मानवसमष्टिसे हटाने के लिये अपने अनुभवके बलपर कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्त मानवजीवनके संचालनके लिये स्थिर किये थे, जिनके प्रति हमारी उपेक्षाबुद्धि हो जानेके कारण यह समस्त पृथ्वीतल नरकका महाविकराल - रूप धारण किये हुए दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन यदि अब भी उन सिद्धान्तों को समझकर हम अपने जीवनमें उन्हें ढाल लें तो यही पृथ्विीतल स्वर्गका सौन्दर्यपूर्ण अनुपम रूप भी धारण कर सकता है ।
विचारकी बात है कि जब भरतक्षेत्रके इस आर्यखण्ड में भोगभूमिका वर्तमान था, तो उस समय सम्पूर्ण मानवसमष्टि सुख और शान्तिपूर्वक रहती थी। इसका कारण यह था कि उस समय प्रत्येक मानव अपना जीवन आकांक्षाओंके आधारपर संचालित न करके आवश्यकताओंके आधारपर ही संचालित करता था । आवश्यकतायें भी प्रत्येक मानवके जीवनकी कम हुआ करती थीं, इसलिये एक तो उसका उपभोग्य पदार्थोंका उपभोग कम हुआ करता था । दूसरे, उसके हृदयमें उपभोग्य पदार्थोंके प्रति आकर्षणका अभाव होनेसे वह उनके संग्रहसे भी सदा दूर रहा करता था । इस प्रकार उस समय सभी मानव परस्पर घुलमिलकर समानरूपसे ही रहा करते थे, उनमें परस्पर कभी भी संघर्षका अवसर नहीं आ पाता था ।
आज हालत बिलकुल विपरीत है । प्रत्येक व्यक्तिने अपनी आवश्यकतायें अप्राकृतिक ढंगसे अधिकाधिकरूपमें बढ़ा रखी हैं और वह बढ़ती ही चली जा रही हैं । इसके अलावा सभी प्रकारकी उपयोगी वस्तुओंके अमर्यादित संग्रहकी ओर भी प्रत्येक व्यक्ति झुका चला जा रहा है । इस तरह सम्पूर्ण मानव- समष्टिका जीवन परस्परकी विषमताओंसे भरा हुआ है । ऐसी हालत में संघर्ष होना अनिवार्य ही समझना चाहिये ।
जैन संस्कृतिके तत्त्वज्ञानमें ऐसे सभी संघर्षोंको समाप्त करनेकी क्षमता पायी जाती है, कारण कि वह मानवमात्रको न्यायोचित मार्गपर चलनेकी शिक्षा देता है । इतना ही नहीं, वह उसे ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org