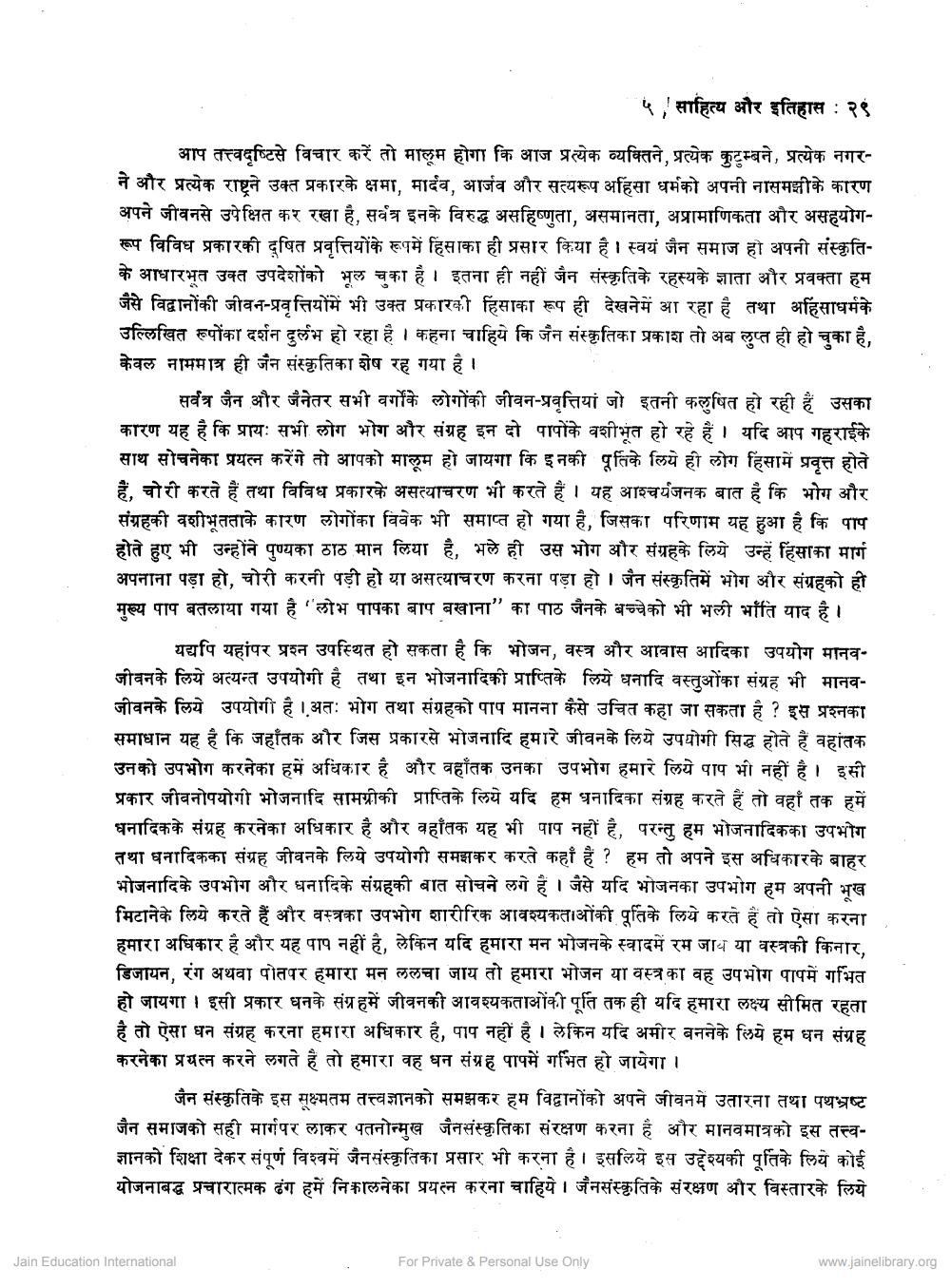________________
५ साहित्य और इतिहास : २९
आप तत्त्वदृष्टिसे विचार करें तो मालूम होगा कि आज प्रत्येक व्यक्तिने, प्रत्येक कुटुम्बने, प्रत्येक नगरने और प्रत्येक राष्ट्रने उक्त प्रकारके क्षमा, मार्दव, आर्जव और सत्यरूप अहिंसा धर्मको अपनी नासमझी के कारण अपने जीवनसे उपेक्षित कर रखा है, सर्वत्र इनके विरुद्ध असहिष्णुता, असमानता, अप्रामाणिकता और असहयोगरूप विविध प्रकारकी दूषित प्रवृत्तियोंके रूपमें हिंसाका ही प्रसार किया है। स्वयं जैन समाज ही अपनी संस्कृतिके आधारभूत उक्त उपदेशोंको भूल चुका है। इतना ही नहीं जैन संस्कृतिके रहस्यके ज्ञाता और प्रवक्ता हम जैसे विद्वानोंकी जीवन- प्रवृत्तियोंमें भी उक्त प्रकारकी हिंसाका रूप ही देखनेमें आ रहा है तथा अहिंसा धर्म के उल्लिखित रूपों का दर्शन दुर्लभ हो रहा है । कहना चाहिये कि जैन संस्कृतिका प्रकाश तो अब लुप्त ही हो चुका है, केवल नाममात्र ही जैन संस्कृतिका शेष रह गया है ।
सर्वत्र जैन और जैनेतर सभी वर्गोंके लोगोंकी जीवन-प्रवृत्तियां जो इतनी कलुषित हो रही हैं उसका कारण यह है कि प्रायः सभी लोग भोग और संग्रह इन दो पापोंके वशीभूत हो रहे हैं। यदि आप गहराई के साथ सोचनेका प्रयत्न करेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि इनकी पूर्तिके लिये ही लोग हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, चोरी करते हैं तथा विविध प्रकारके असत्याचरण भी करते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि भोग और संग्रहकी वशीभूतताकै कारण लोगोंका विवेक भी समाप्त हो गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि पाप होते हुए भी उन्होंने पुण्यका ठाठ मान लिया है, भले ही उस भोग और संग्रहके लिये उन्हें हिंसाका मार्ग अपनाना पड़ा हो, चोरी करनी पड़ी हो या असत्याचरण करना पड़ा हो । जैन संस्कृतिमें भोग और संग्रहको ही मुख्य पाप बतलाया गया है "लोभ पापका बाप बखाना" का पाठ जैनके बच्चे को भी भली भाँति याद है ।
यद्यपि यहां पर प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भोजन, वस्त्र और आवास आदिका उपयोग मानवजीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है तथा इन भोजनादिकी प्राप्तिके लिये धनादि वस्तुओंका संग्रह भी मानवजीवनके लिये उपयोगी है। अतः भोग तथा संग्रहको पाप मानना कैसे उचित कहा जा सकता है ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि जहाँतक और जिस प्रकारसे भोजनादि हमारे जीवन के लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं वहांतक उनको उपभोग करनेका हमें अधिकार है और वहाँतक उनका उपभोग हमारे लिये पाप भी नहीं है। इसी प्रकार जीवनोपयोगी भोजनादि सामग्रीकी प्राप्तिके लिये यदि हम धनाविका संग्रह करते हैं तो वहाँ तक हमें धनादिकके संग्रह करनेका अधिकार है और वहाँतक यह भी पाप नहीं है, परन्तु हम भोजनादिकका उपभोग तथा धनाविकका संग्रह जीवनके लिये उपयोगी समझकर करते कहाँ है? हम तो अपने इस अधिकारके बाहर भोजनादिके उपभोग और धनादिके संग्रहकी बात सोचने लगे हैं। जैसे यदि भोजनका उपभोग हम अपनी भूख मिटानेके लिये करते हैं और वस्त्रका उपभोग शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये करते हैं तो ऐसा करना हमारा अधिकार है और यह पाप नहीं है, लेकिन यदि हमारा मन भोजनके स्वावमें रम जाय या वस्त्रकी किनार, डिजायन, रंग अथवा पोतपर हमारा मन ललचा जाय तो हमारा भोजन या वस्त्रका वह उपभोग पापमें गभित हो जायगा। इसी प्रकार धनके संग्रहमें जीवनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही यदि हमारा लक्ष्य सीमित रहता है तो ऐसा धन संग्रह करना हमारा अधिकार है, पाप नहीं है। लेकिन यदि अमीर बनने के लिये हम धन संग्रह करनेका प्रयत्न करने लगते है तो हमारा वह धन संग्रह पापमें गर्भित हो जायेगा ।
जैन संस्कृतिके इस सूक्ष्मतम तत्त्वज्ञान को समझकर हम विद्वानोंको अपने जीवन में उतारना तथा पचभ्रष्ट जैन समाजको सही मार्गपर लाकर पतनोन्मुख जैनसंस्कृतिका संरक्षण करना है और मानवमात्रको इस तस्व ज्ञानको शिक्षा देकर संपूर्ण विश्वमें जैन संस्कृतिका प्रसार भी करना है। इसलिये इस उद्देश्यकी पूर्ति के लिये कोई योजनाबद्ध प्रचारात्मक ढंग हमें निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये । जैनसंस्कृतिके संरक्षण और विस्तार के लिये
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org