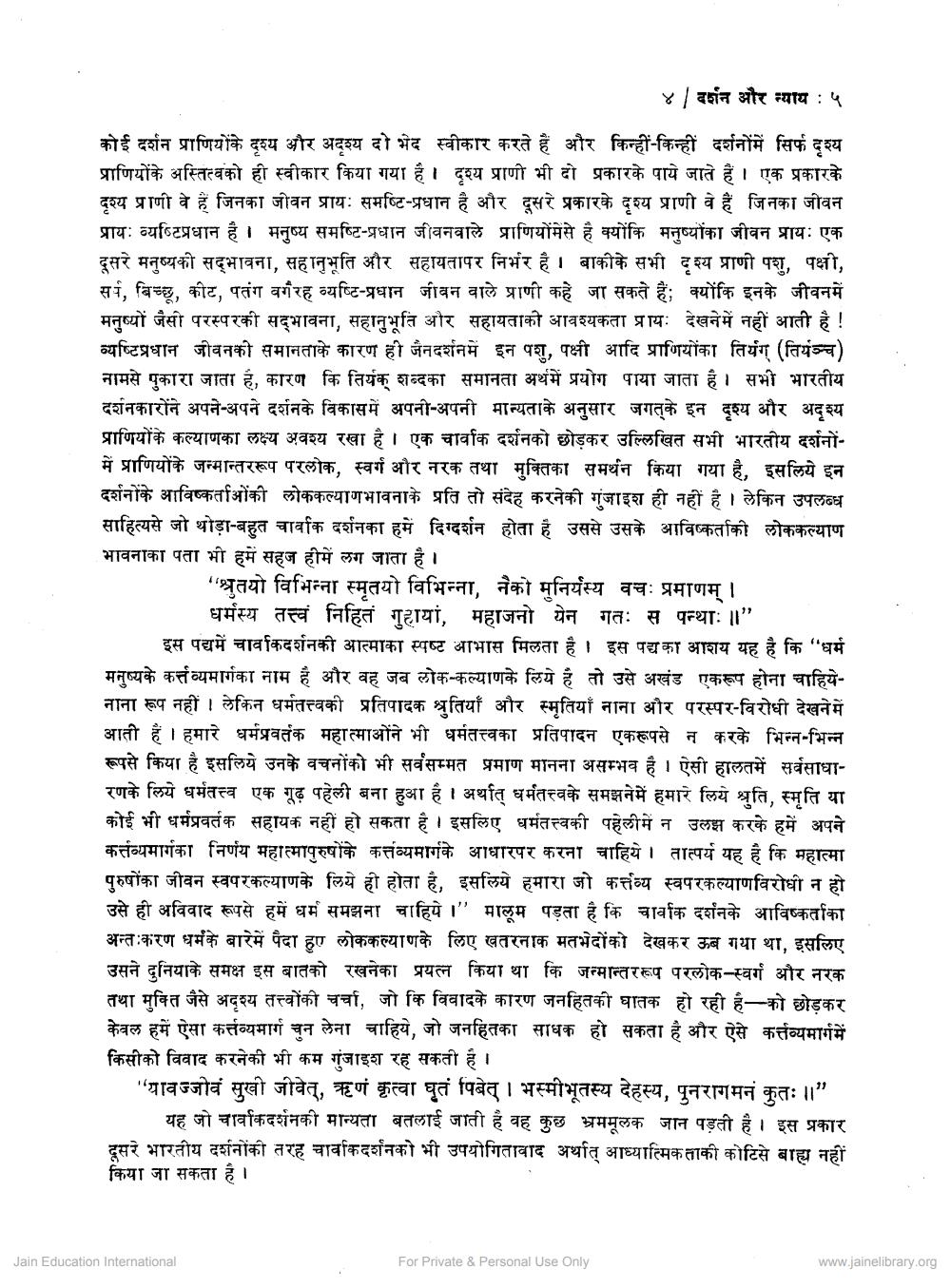________________
४ / दर्शन और न्याय : ५
कोई दर्शन प्राणियोंके दृश्य और अदृश्य दो भेद स्वीकार करते हैं और किन्हीं-किन्हीं दर्शनोंमें सिर्फ दृश्य प्राणियोंके अस्तित्वको ही स्वीकार किया गया है। दृश्य प्राणी भी दो प्रकारके पाये जाते हैं। एक प्रकारके दृश्य प्राणी वे है जिनका जीवन प्रायः समष्टि-प्रधान है और दूसरे प्रकारके दृश्य प्राणी वे हैं जिनका जीवन प्रायः व्यष्टिप्रधान है। मनुष्य समष्टि-प्रधान जीवनवाले प्राणियोंमेंसे है क्योंकि मनुष्योंका जीवन प्रायः एक दूसरे मनुष्यको सद्भावना, सहानुभूति और सहायतापर निर्भर है। बाकीके सभी दृश्य प्राणी पशु, पक्षी, सर्प, बिच्छू, कीट, पतंग वगैरह व्यष्टि-प्रधान जीवन वाले प्राणी कहे जा सकते हैं; क्योंकि इनके जीवनमें मनुष्यों जैसी परस्परकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायताको आवश्यकता प्रायः देखने में नहीं आती है ! व्यष्टिप्रधान जीवनको समानताके कारण ही जैनदर्शनमें इन पशु, पक्षी आदि प्राणियोंका तिर्यग (तियंञ्च) नामसे पुकारा जाता है, कारण कि तिर्यक् शब्दका समानता अर्थमें प्रयोग पाया जाता है। सभी भारतीय दर्शनकारोंने अपने-अपने दर्शनके विकासमें अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार जगत्के इन दृश्य और अदृश्य प्राणियोंके कल्याणका लक्ष्य अवश्य रखा है। एक चार्वाक दर्शनको छोड़कर उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमें प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिका समर्थन किया गया है, इसलिये इन दर्शनोंके आविष्कर्ताओंकी लोककल्याणभावनाके प्रति तो संदेह करनेकी गुंजाइश ही नहीं है । लेकिन उपलब्ध साहित्यसे जो थोड़ा-बहुत चार्वाक दर्शनका हमें दिग्दर्शन होता है उससे उसके आविष्कर्ताकी लोककल्याण भावनाका पता भी हमें सहज हीमें लग जाता है।
"श्रतयो विभिन्ना स्मतयो विभिन्ना, नैको मनिर्यस्य वचः प्रमाणम ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥" इस पद्यमें चार्वाकदर्शनकी आत्माका स्पष्ट आभास मिलता है। इस पद्य का आशय यह है कि "धर्म
है। इस पद्य का आशय यह है कि "धर्म मनुष्यके कर्तव्यमार्गका नाम है और वह जब लोक-कल्याणके लिये है तो उसे अखंड एकरूप होना चाहियेनाना रूप नहीं। लेकिन धर्मतत्त्वकी प्रतिपादक श्रतियाँ और स्मृतियाँ नाना और परस्पर-विरोधी देखने में आती हैं। हमारे धर्मप्रवर्तक महात्माओंने भी धर्मतत्त्वका प्रतिपादन एकरूपसे न करके भिन्न-भिन्न रूपसे किया है इसलिये उनके वचनोंको भी सर्वसम्मत प्रमाण मानना असम्भव है । ऐसी हालतमें सर्वसाधारणके लिये धर्मतत्त्व एक गूढ़ पहेली बना हुआ है । अर्थात् धर्मतत्त्वके समझने में हमारे लिये श्रुति, स्मृति या कोई भी धर्मप्रवर्तक सहायक नहीं हो सकता है । इसलिए धर्मतत्त्वकी पहेलीमें न उलझ करके हमें अपने कर्तव्यमार्गका निर्णय महात्मापरुषोंके कर्तव्यमार्गके आधारपर करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि महात्मा पुरुषोंका जीवन स्वपरकल्याणके लिये ही होता है, इसलिये हमारा जो कर्तव्य स्वपरकल्याणविरोधी न हो उसे ही अविवाद रूपसे हमें धर्म समझना चाहिये।" मालूम पड़ता है कि चार्वाक दर्शनके आविष्कर्ताका अन्तःकरण धर्म के बारेमें पैदा हए लोककल्याणके लिए खतरनाक मतभेदोंको देखकर ऊब गया था, इसलिए उसने दुनियाके समक्ष इस बातको रखनेका प्रयत्न किया था कि जन्मान्तररूप परलोक-स्वर्ग और नरक तथा मक्ति जैसे अदश्य तत्त्वोंकी चर्चा, जो कि विवादके कारण जनहितकी घातक हो रही है-को छोडकर केवल हमें ऐसा कर्तव्यमार्ग चन लेना चाहिये, जो जनहितका साधक हो सकता है और ऐसे कर्त्तव्यमार्गमें किसीको विवाद करनेकी भी कम गुंजाइश रह सकती है। "यावज्जीवं सुखी जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः॥"
यह जो चार्वाकदर्शनकी मान्यता बतलाई जाती है वह कुछ भ्रममूलक जान पड़ती है। इस प्रकार दसरे भारतीय दर्शनोंकी तरह चावकिदर्शनको भी उपयोगितावाद अर्थात् आध्यात्मिकताकी कोटिसे बाह्य नहीं किया जा सकता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org