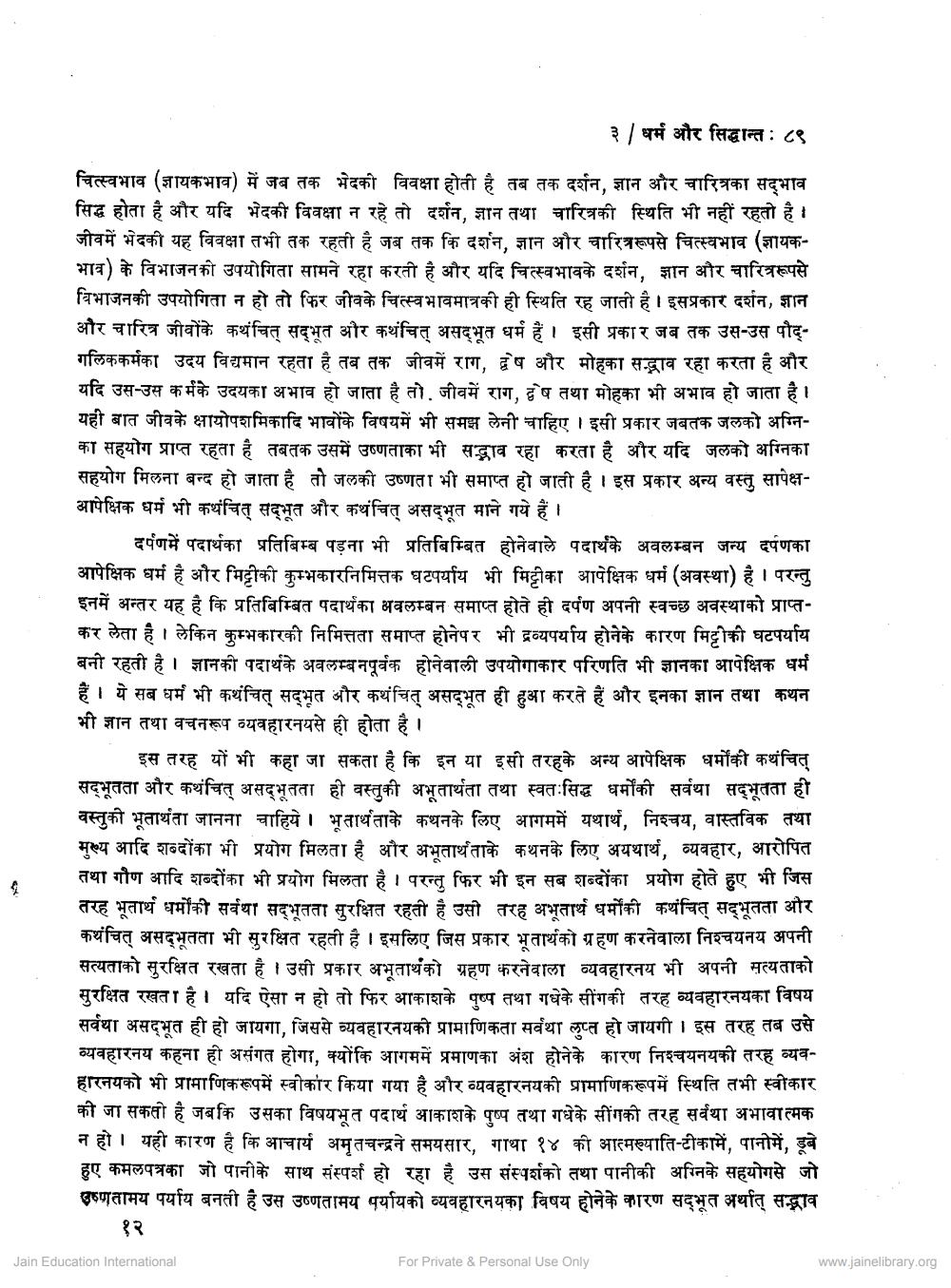________________
३ / धर्म और सिद्धान्त : ८९
चित्स्वभाव (ज्ञायकभाव ) में जब तक भेदको विवक्षा होती है तब तक दर्शन, ज्ञान और चारित्रका सद्भाव सिद्ध होता है और यदि भेदकी विवक्षा न रहे तो दर्शन, ज्ञान तथा चारित्रकी स्थिति भी नहीं रहती है । जीवमें भेदकी यह विवक्षा तभी तक रहती है जब तक कि दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूपसे चित्स्वभाव (ज्ञायक(भाव) के विभाजनको उपयोगिता सामने रहा करती है और यदि चित्स्वभावके दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूपसे विभाजनकी उपयोगिता न हो तो फिर जीवके चित्स्वभावमात्रकी ही स्थिति रह जाती है। इसप्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र जीवोंके कथंचित् सद्भूत और कथंचित् असद्भूत धर्म हैं । इसी प्रकार जब तक उस-उस पौद्गलिक कर्मका उदय विद्यमान रहता है तब तक जीवमें राग, द्वेष और मोहका सद्भाव रहा करता है और यदि उस उस कर्मके उदयका अभाव हो जाता है तो जीवमें राग, द्वेष तथा मोहका भी अभाव जाता है। यही बात जीवके क्षायोपशमिकादि भावोंके विषय में भी समझ लेनी चाहिए । इसी प्रकार जबतक जलको अग्निका सहयोग प्राप्त रहता है तबतक उसमें उष्णताका भी सद्भाव रहा करता है और यदि जलको अग्निका सहयोग मिलना बन्द हो जाता है तो जलकी उष्णता भी समाप्त हो जाती है । इस प्रकार अन्य वस्तु सापेक्षआपेक्षिक धर्म भी कथंचित् सद्भूत और कथंचित् असद्भूत माने गये हैं ।
4
दर्पण में पदार्थका प्रतिबिम्ब पड़ना भी प्रतिबिम्बित होनेवाले पदार्थके अवलम्बन जन्य दर्पणका आपेक्षिक धर्म है और मिट्टीकी कुम्भकारनिमित्तक घटपर्याय भी मिट्टीका आपेक्षिक धर्म (अवस्था) है । परन्तु इनमें अन्तर यह है कि प्रतिबिम्बित पदार्थका अवलम्बन समाप्त होते ही दर्पण अपनी स्वच्छ अवस्थाको प्राप्तकर लेता है । लेकिन कुम्भकारकी निमित्तता समाप्त होनेपर भी द्रव्यपर्याय होनेके कारण मिट्टीकी घटपर्याय बनी रहती है । ज्ञानकी पदार्थके अवलम्बनपूर्वक होनेवाली उपयोगाकार परिणति भी ज्ञानका आपेक्षिक धर्म
। ये सब धर्म भी कथंचित् सद्भूत और कथंचित् असद्भूत ही हुआ करते हैं और इनका ज्ञान तथा कथन भी ज्ञान तथा वचनरूप व्यवहारनयसे ही होता है ।
इस तरह यों भी कहा जा सकता है कि इन या इसी तरहके अन्य आपेक्षिक धर्मोकी कथंचित् सद्भूतता और कथंचित् असद्भूतता ही वस्तुकी अभूतार्थता तथा स्वतःसिद्ध धर्मोकी सर्वथा सद्भूतता ही वस्तुकी भूतार्थता जानना चाहिये । भूतार्थता के कथनके लिए आगममें यथार्थ, निश्चय, वास्तविक तथा मुख्य आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है और अभूतार्थताके कथन के लिए अयथार्थ, व्यवहार, आरोपित
तथा गौण आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । परन्तु फिर भी इन सब शब्दों का प्रयोग होते हुए भी जिस तरह भूतार्थं धर्मोकी सर्वथा सद्भूतता सुरक्षित रहती है उसी तरह अभूतार्थ धर्मोकी कथंचित् सद्भूतता और कथंचित् असद्भूतता भी सुरक्षित रहती है । इसलिए जिस प्रकार भूतार्थको ग्रहण करनेवाला निश्चयनय अपनी सत्यताको सुरक्षित रखता है । उसी प्रकार अभूतार्थको ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय भी अपनी सत्यताको सुरक्षित रखता है । यदि ऐसा न हो तो फिर आकाशके पुष्प तथा गधेके सींगकी तरह व्यवहारनयका विषय सर्वथा असद्भूत ही हो जायगा, जिससे व्यवहारनयकी प्रामाणिकता सर्वथा लुप्त हो जायगी । इस तरह तब उसे व्यवहारनय कहना ही असंगत होगा, क्योंकि आगममें प्रमाणका अंश होनेके कारण निश्चयनयकी तरह व्यवहानको भी प्रामाणिक रूपमें स्वीकार किया गया है और व्यवहारनयकी प्रामाणिक रूप में स्थिति तभी स्वीकार की जा सकती है जबकि उसका विषयभूत पदार्थ आकाशके पुष्प तथा गधेके सींगकी तरह सर्वथा अभावात्मक न हो । यही कारण है कि आचार्य अमृतचन्द्रने समयसार, गाथा १४ की आत्मख्याति - टीकामें, पानीमें, डूबे हुए कमलपत्रका जो पानी के साथ संस्पर्श हो रहा है उस संस्पर्शको तथा पानीकी अग्निके सहयोग से जो उष्णतामय पर्याय बनती उस उष्णतामय पर्यायको व्यवहारनयका विषय होनेके कारण सद्भूत अर्थात् सद्भाव
१२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org