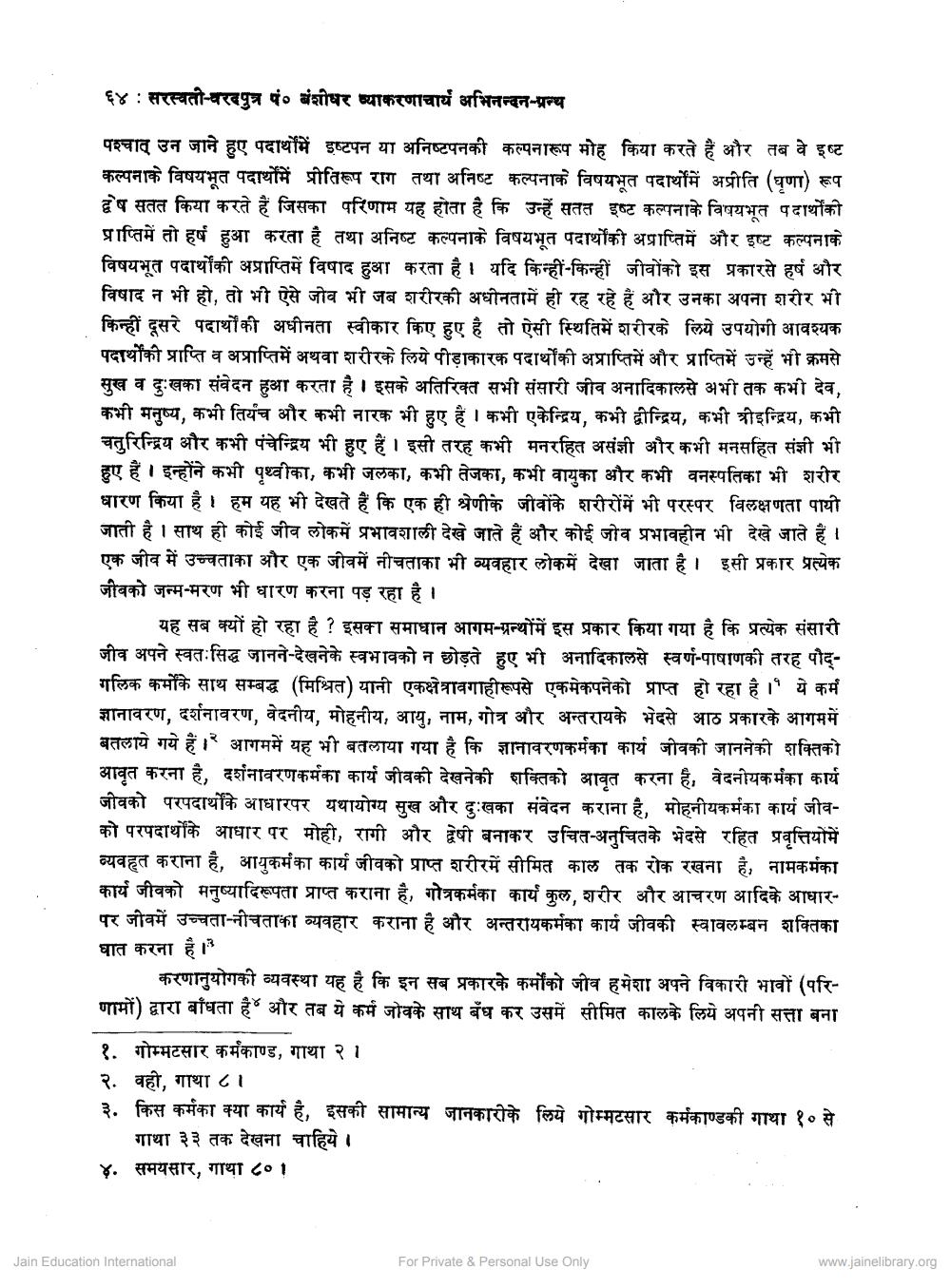________________
६४ : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-प्रन्थ
पश्चात् उन जाने हुए पदार्थोंमें इष्टपन या अनिष्टपनकी कल्पनारूप मोह किया करते हैं और तब वे इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें प्रीतिरूप राग तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें अप्रीति (घृणा) रूप द्वेष सतत किया करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सतत इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी प्राप्तिमें तो हर्ष हुआ करता है तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोकी अप्राप्तिमें और इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थों की अप्राप्तिमें विषाद हुआ करता है। यदि किन्हीं-किन्हीं जीवोंको इस प्रकारसे हर्ष और विषाद न भी हो, तो भी ऐसे जीव भी जब शरीरकी अधीनतामें ही रह रहे है और उनका अपना शरीर भी किन्हीं दूसरे पदार्थों की अधीनता स्वीकार किए हुए है तो ऐसी स्थितिमें शरीरके लिये उपयोगी आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति व अप्राप्तिमें अथवा शरीरके लिये पीडाकारक पदार्थोंकी अप्राप्तिमें और प्राप्तिमें उन्हें भी क्रमसे सुख व दुःखका संवेदन हआ करता है । इसके अतिरिक्त सभी संसारी जीव अनादिकालसे अभी तक कभी देव कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच और कभी नारक भी हुए है । कभी एकेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कभी श्रीइन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पंचेन्द्रिय भी हुए हैं। इसी तरह कभी मनरहित असंज्ञी और कभी मनसहित संज्ञी भी हुए हैं । इन्होंने कभी पृथ्वीका, कभी जलका, कभी तेजका, कभी वायुका और कभी वनस्पतिका भी शरीर धारण किया है। हम यह भी देखते हैं कि एक ही श्रेणीके जीवोंके शरीरोंमें भी परस्पर विलक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई जीव लोकमें प्रभावशाली देखे जाते हैं और कोई जोव प्रभावहीन भी देखे जाते है। एक जीव में उच्चताका और एक जीवमें नीचताका भी व्यवहार लोकमें देखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवको जन्म-मरण भी धारण करना पड़ रहा है ।
यह सब क्यों हो रहा है ? इसका समाधान आगम-ग्रन्थोंमें इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक संसारी जीव अपने स्वतःसिद्ध जानने-देखनेके स्वभावको न छोड़ते हुए भी अनादिकालसे स्वर्ण-पाषाणकी तरह पौद्गलिक कर्मोके साथ सम्बद्ध (मिश्रित) यानी एकक्षेत्रावगाहीरूपसे एकमेकपनेको प्राप्त हो रहा है।' ये कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके भेदसे आठ प्रकारके आगममें बतलाये गये है। आगममें यह भी बतलाया गया है कि ज्ञानावरणकर्मका कार्य जीवकी जाननेकी शक्तिको आवृत करना है, दर्शनावरणकर्मका कार्य जीवकी देखनेकी शक्तिको आवत करना है, वेदनीयकर्मका कार्य जीवको परपदार्थों के आधारपर यथायोग्य सुख और दुःखका संवेदन कराना है, मोहनीयकर्मका कार्य जीवको परपदार्थोंके आधार पर मोही, रागी और द्वेषी बनाकर उचित-अनुचितके भेदसे रहित प्रवृत्तियोंमें व्यवहृत कराना है, आयुकर्मका कार्य जीवको प्राप्त शरीरमें सीमित काल तक रोक रखना है, नामकर्मका कार्य जीवको मनुष्यादिरूपता प्राप्त कराना है, गोत्रकर्मका कार्य कुल, शरीर और आचरण आदिके आधारपर जीवमें उच्चता-नीचताका व्यवहार कराना है और अन्तरायकर्मका कार्य जीवकी स्वावलम्बन शक्तिका घात करना है।
करणानुयोगकी व्यवस्था यह है कि इन सब प्रकारके कर्मोको जीव हमेशा अपने विकारी भावों (परिणामों) द्वारा बाँधता है और तब ये कर्म जोवके साथ बँध कर उसमें सीमित कालके लिये अपनी सत्ता बना १. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा २ । २. वही, गाथा ८। ३. किस कर्मका क्या कार्य है, इसकी सामान्य जानकारीके लिये गोम्मटसार कर्मकाण्डकी गाथा १० से
गाथा ३३ तक देखना चाहिये। ४. समयसार, गाथा ८०॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org