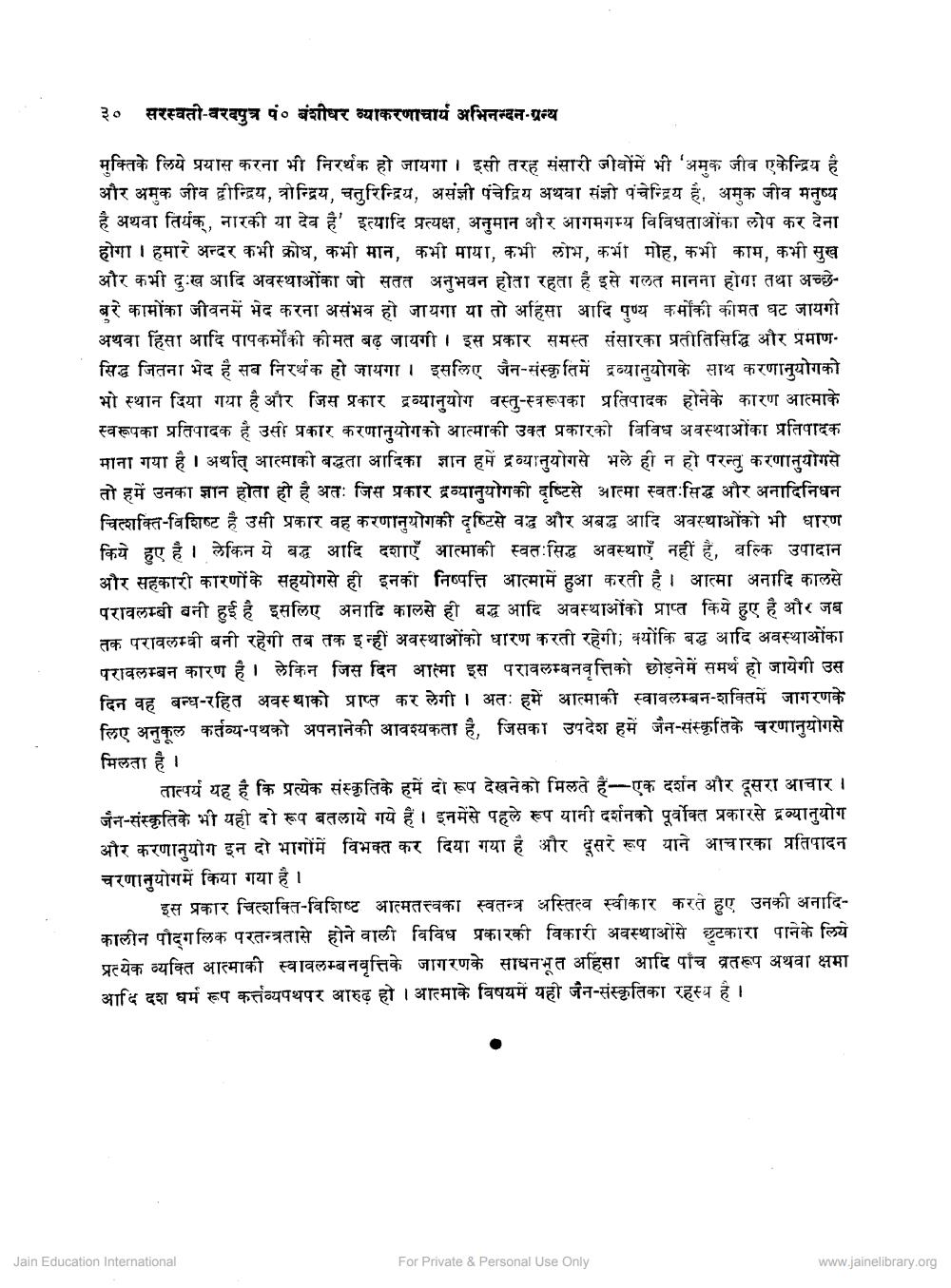________________
३० सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्य
मुक्तिके लिये प्रयास करना भी निरर्थक हो जायगा। इसी तरह संसारी जीवोंमें भी 'अमक जीव एकेन्द्रिय है और अमुक जीव द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेद्रिय अथवा संज्ञो पंचेन्द्रिय है, अमुक जीव मनुष्य है अथवा तिर्यक् , नारकी या देव है' इत्यादि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमगम्य विविधताओंका लोप कर देना होगा । हमारे अन्दर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम, कभी सुख और कभी दुःख आदि अवस्थाओंका जो सतत अनुभवन होता रहता है इसे गलत मानना होगा तथा अच्छेबुरे कामोंका जीवनमें भेद करना असंभव हो जायगा या तो अहिंसा आदि पुण्य कर्मोकी कीमत घट जायगी अथवा हिंसा आदि पापकर्मों की कीमत बढ़ जायगी। इस प्रकार समस्त संसारका प्रतीतिसिद्धि और प्रमाणसिद्ध जितना भेद है सब निरर्थक हो जायगा। इसलिए जैन-संस्कृतिमें द्रव्यानुयोगके साथ करणानुयोगको भो स्थान दिया गया है और जिस प्रकार द्रव्यानुयोग वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादक होने के कारण आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक है उसी प्रकार करणानुयोगको आत्माकी उक्त प्रकारको विविध अवस्थाओंका प्रतिपादक माना गया है । अर्थात् आत्माको बद्धता आदिका ज्ञान हमें द्रव्यानुयोगसे भले ही न हो परन्तु करणानुयोगसे तो हमें उनका ज्ञान होता ही है अतः जिस प्रकार द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे आत्मा स्वतःसिद्ध और अनादिनिधन चित्शक्ति-विशिष्ट है उसी प्रकार वह करणानुयोगकी दृष्टिसे वद्ध और अबद्ध आदि अवस्थाओंको भी धारण किये हए है । लेकिन ये बद्ध आदि दशाएँ आत्माकी स्वतःसिद्ध अवस्थाएँ नहीं है, बल्कि उपादान
और सहकारी कारणों के सहयोगसे ही इनकी निष्पत्ति आत्मामें हुआ करती है। आत्मा अनादि कालसे परावलम्बी बनी हुई है इसलिए अनादि कालसे ही बद्ध आदि अवस्थाओंको प्राप्त किये हुए है और जब तक परावलम्वी बनी रहेगी तब तक इन्हीं अवस्थाओंको धारण करती रहेगी, क्योंकि बद्ध आदि अवस्थाओंका परावलम्बन कारण है। लेकिन जिस दिन आत्मा इस परावलम्बनवृत्तिको छोड़ने में समर्थ हो जायेगी उस दिन वह बन्ध-रहित अवस्थाको प्राप्त कर लेगी। अतः हमें आत्माकी स्वावलम्बन-शक्तिमें जागरणके लिए अनकल कर्तव्य-पथको अपनानेकी आवश्यकता है, जिसका उपदेश हमें जैन-संस्कृतिके चरणानुयोगसे मिलता है।
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृतिके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं-एक दर्शन और दूसरा आचार । जैन-संस्कृतिके भी यही दो रूप बतलाये गये हैं। इनसे पहले रूप यानी दर्शनको पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्यानुयोग और करणानयोग इन दो भागोंमें विभक्त कर दिया गया है और दूसरे रूप याने आचारका प्रतिपादन चरणानुयोगमें किया गया है ।
इस प्रकार चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मतत्त्वका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हए उनकी अनादिकालीन पौदगलिक परतन्त्रतासे होने वाली विविध प्रकारकी विकारी अवस्थाओंसे छुटकारा पाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति आत्माकी स्वावलम्बनवृत्तिके जागरणके साधनभूत अहिंसा आदि पाँच व्रतरूप अथवा क्षमा आदि दश धर्म रूप कर्तव्यपथपर आरुढ़ हो । आत्माके विषयमें यही जैन-संस्कृतिका रहस्य है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org