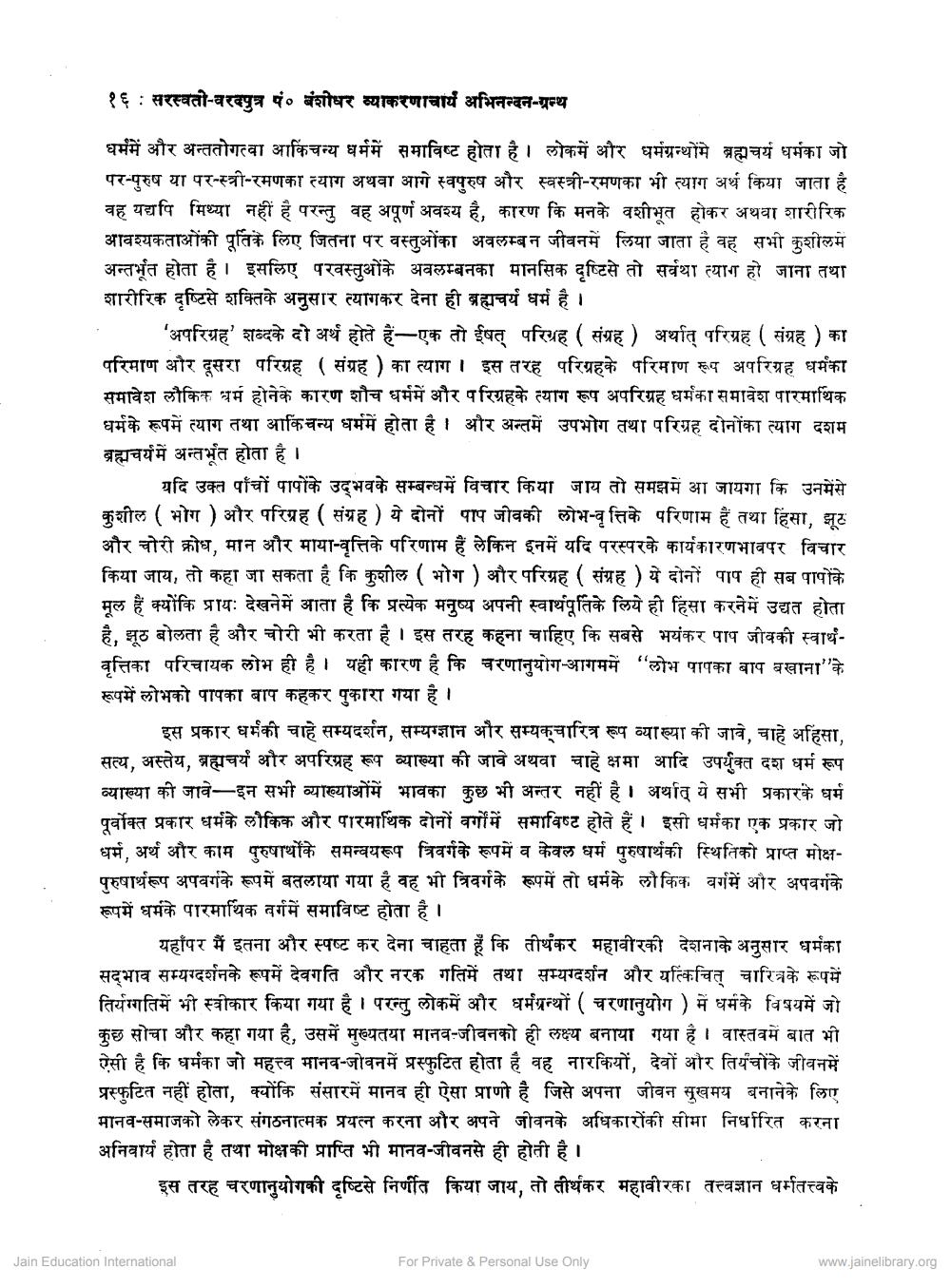________________
१६ : सरस्वती - वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन ग्रन्थ
धर्म में और अन्ततोगत्वा आकिंचन्य धर्ममें समाविष्ट होता है । लोकमें और धर्मग्रन्थोंमे ब्रह्मचर्य धर्मका जो पर-पुरुष या पर-स्त्री-रमणका त्याग अथवा आगे स्वपुरुष और स्वस्त्री - रमणका भी त्याग अर्थ किया जाता है। वह यद्यपि मिथ्या नहीं है परन्तु वह अपूर्ण अवश्य है, कारण कि मनके वशीभूत होकर अथवा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना पर वस्तुओंका अवलम्बन जीवनमें लिया जाता है वह सभी कुशीलमें अन्तर्भूत होता है । इसलिए परवस्तुओंके अवलम्बनका मानसिक दृष्टिसे तो सर्वथा त्याग हो जाना तथा शारीरिक दृष्टिसे शक्ति के अनुसार त्यागकर देना ही ब्रह्मचर्य धर्म है ।
'अपरिग्रह' शब्द के दो अर्थ होते हैं - एक तो ईषत् परिग्रह ( संग्रह ) अर्थात् परिग्रह ( संग्रह ) का परिमाण और दूसरा परिग्रह ( संग्रह ) का त्याग । इस तरह परिग्रहके परिमाण रूप अपरिग्रह धर्मका समावेश लौकिक धर्म होनेके कारण शौच धर्ममें और परिग्रहके त्याग रूप अपरिग्रह धर्मका समावेश पारमार्थिक धर्म के रूप में त्याग तथा आकिंचन्य धर्ममें होता है । और अन्तमें उपभोग तथा परिग्रह दोनोंका त्याग दशम ब्रह्मचर्य में अन्तर्भूत होता है ।
यदि उक्त पाँचों पापोंके उद्भव के सम्बन्धमें विचार किया जाय तो समझ में आ जायगा कि उनमें से कुशील ( भोग ) और परिग्रह ( संग्रह ) ये दोनों पाप जीवकी लोभ-वृत्तिके परिणाम हैं तथा हिंसा, झूट और चोरी क्रोध, मान और माया-वृत्तिके परिणाम हैं लेकिन इनमें यदि परस्परके कार्यकारणभावपर विचार किया जाय, तो कहा जा सकता है कि कुशील ( भोग ) और परिग्रह ( संग्रह ) ये दोनों पाप ही सब पापोंके मूल हैं क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये ही हिंसा करनेमें उद्यत होता है, झूठ बोलता है और चोरी भी करता है । इस तरह कहना चाहिए कि सबसे भयंकर पाप जीवकी स्वार्थवृत्तिका परिचायक लोभ ही है । यही कारण है कि चरणानुयोग-आगममें " लोभ पापका बाप बखाना" के रूपमें लोभको पापका बाप कहकर पुकारा गया है ।
अर्थात् ये सभी प्रकारके धर्म
इस प्रकार धर्मकी चाहे सम्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप व्याख्या की जावे, चाहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह रूप व्याख्या की जावे अथवा चाहे क्षमा आदि उपर्युक्त दश धर्म रूप व्याख्या की जावे – इन सभी व्याख्याओंमें भावका कुछ भी अन्तर नहीं है । पूर्वोक्त प्रकार धर्मके लौकिक और पारमार्थिक दोनों वर्गों में समाविष्ट होते । इसी धर्मका एक प्रकार जो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थोके समन्वयरूप त्रिवर्गके रूपमें व केवल धर्म पुरुषार्थकी स्थितिको प्राप्त मोक्षपुरुषार्थरूप अपवर्गके रूप में बतलाया गया है वह भी त्रिवर्ग के रूपमें तो धर्मके लौकिक वर्ग में और अपवर्गके रूपमें धर्मके पारमार्थिक वर्ग में समाविष्ट होता है ।
यहाँपर मैं इतना और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तीर्थंकर महावीरकी देशनाके अनुसार धर्मका सद्भाव सम्यग्दर्शनके रूपमें देवगति और नरक गतिमें तथा सम्यग्दर्शन और यत्किचित् चारित्र के रूपमें तिर्यग्गति में भी स्वीकार किया गया है । परन्तु लोकमें और धर्मग्रन्थों ( चरणानुयोग ) में धर्मके विषयमें जो कुछ सोचा और कहा गया है, उसमें मुख्यतया मानव-जीवनको ही लक्ष्य बनाया गया है । वास्तव में बात भी ऐसी है कि धर्मका जो महत्त्व मानव-जीवन में प्रस्फुटित होता है वह नारकियों, देवों और तियंचोंके जीवन में प्रस्फुटित नहीं होता, क्योंकि संसारमें मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना जीवन सुखमय बनानेके लिए मानव समाजको लेकर संगठनात्मक प्रयत्न करना और अपने जीवनके अधिकारोंकी सीमा निर्धारित करना अनिवार्य होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति भी मानव जीवनसे ही होती है ।
इस तरह चरणानुयोगकी दृष्टिसे निर्णीत किया जाय, तो तीर्थंकर महावीरका तत्वज्ञान धर्मतत्त्व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org