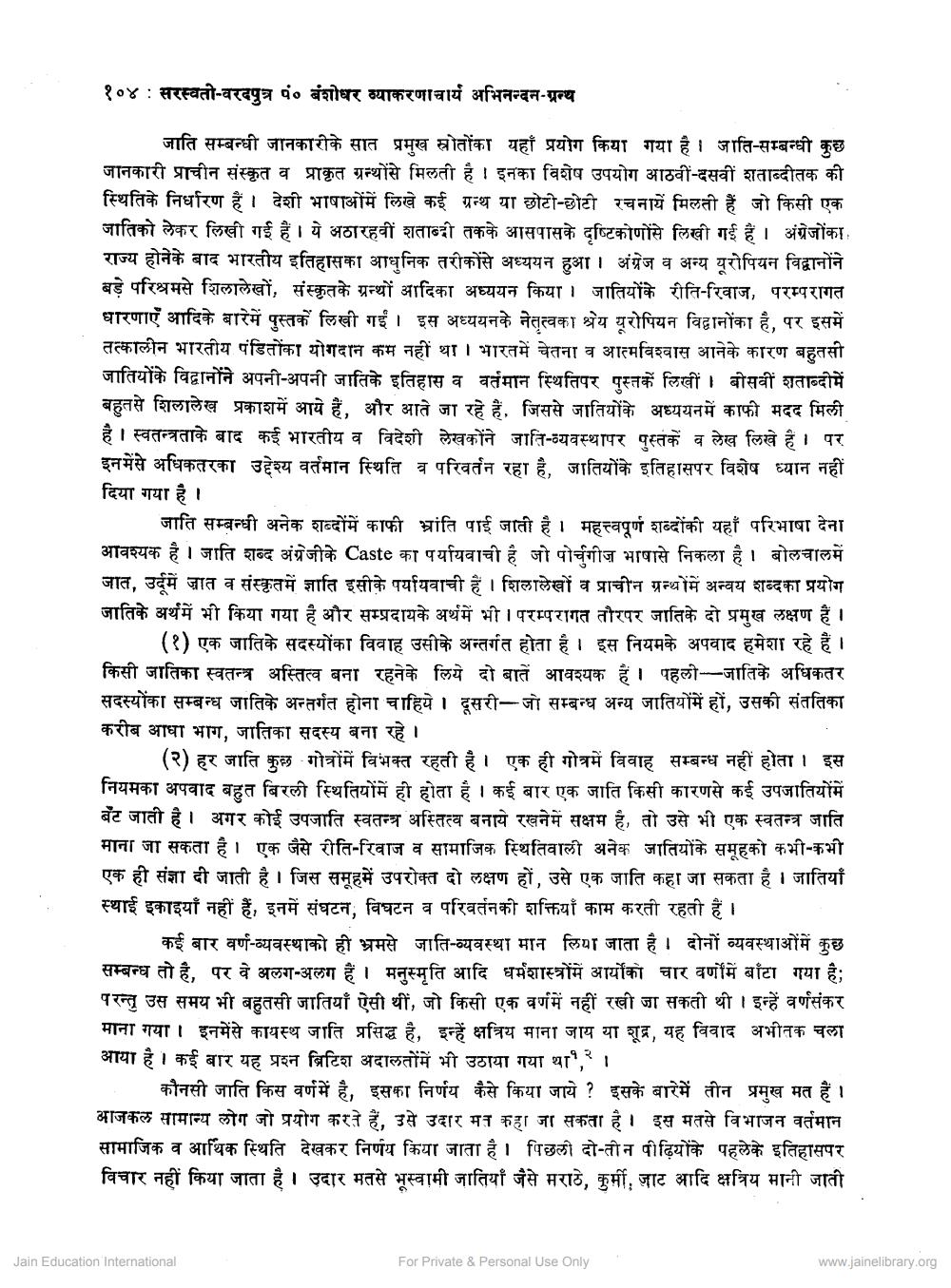________________
१०४ : सरस्वती-वरदपुत्र पं. बंशोधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ
जाति सम्बन्धी जानकारीके सात प्रमुख स्रोतोंका यहाँ प्रयोग किया गया है। जाति-सम्बन्धी कुछ जानकारी प्राचीन संस्कृत व प्राकृत ग्रन्थोंसे मिलती है। इनका विशेष उपयोग आठवीं-दसवीं शताब्दीतक की स्थितिके निर्धारण हैं। देशी भाषाओंमें लिखे कई ग्रन्थ या छोटी-छोटी रचनायें मिलती हैं जो किसी एक जातिको लेकर लिखी गई हैं। ये अठारहवीं शताब्दी तकके आसपासके दृष्टिकोणोंसे लिखी गई हैं। अंग्रेजोंका: राज्य होनेके बाद भारतीय इतिहासका आधनिक तरीकोंसे अध्ययन हआ। अंग्रेज व अन्य यूरोपियन विद्वानोंने बड़े परिश्रमसे शिलालेखों, संस्कृतके ग्रन्थों आदिका अध्ययन किया। जातियोंके रीति-रिवाज, परम्परागत धारणाएँ आदिके बारेमें पुस्तकें लिखी गईं। इस अध्ययनके नेतृत्वका श्रेय यूरोपियन विद्वानोंका है, पर इसमें तत्कालीन भारतीय पंडितोंका योगदान कम नहीं था। भारतमें चेतना व आत्मविश्वास आनेके कारण बहुतसी जातियोंके विद्वानोंने अपनी-अपनी जातिके इतिहास व वर्तमान स्थितिपर पस्तकें लिखीं। बीसवीं शताब्दीमें बहतसे शिलालेख प्रकाशमें आये हैं, और आते जा रहे है, जिससे जातियोंके अध्ययनमें काफी मदद मिली है। स्वतन्त्रताके बाद कई भारतीय व विदेशी लेखकोंने जाति-व्यवस्थापर पुस्तकें व लेख लिखे है। पर इनमेंसे अधिकतरका उद्देश्य वर्तमान स्थिति व परिवर्तन रहा है. जातियोंके इतिहासपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
जाति सम्बन्धी अनेक शब्दोंमें काफी भ्रांति पाई जाती है । महत्त्वपूर्ण शब्दोंकी यहाँ परिभाषा देना आवश्यक है । जाति शब्द अंग्रेजीके Caste का पर्यायवाची है जो पोर्चुगीज भाषासे निकला है । बोलचालमें जात, उर्दमें जात व संस्कृतमें ज्ञाति इसीके पर्यायवाची हैं । शिलालेखों व प्राचीन ग्रन्थोंमें अन्वय शब्दका प्रयोग जातिके अर्थ में भी किया गया है और सम्प्रदायके अर्थमें भी । परम्परागत तौरपर जातिके दो प्रमुख लक्षण है ।
(१) एक जातिके सदस्योंका विवाह उसीके अन्तर्गत होता है। इस नियमके अपवाद हमेशा रहे हैं। किसी जातिका स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहनेके लिये दो बातें आवश्यक हैं। पहली-जातिके अधिकतर सदस्योंका सम्बन्ध जातिके अन्तर्गत होना चाहिये। दूसरी-जो सम्बन्ध अन्य जातियोंमें हों, उसकी संततिका करीब आधा भाग, जातिका सदस्य बना रहे।
(२) हर जाति कुछ गोत्रोंमें विभक्त रहती है। एक ही गोत्रमें विवाह सम्बन्ध नहीं होता। इस नियमका अपवाद बहुत बिरली स्थितियोंमें ही होता है । कई बार एक जाति किसी कारणसे कई उपजातियोंमें बँट जाती है। अगर कोई उपजाति स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने में सक्षम है, तो उसे भी एक स्वतन्त्र जाति माना जा सकता है। एक जैसे रीति-रिवाज व सामाजिक स्थितिवाली अनेक जातियोंके समूहको कभी-कभी एक ही संज्ञा दी जाती है। जिस समूहमें उपरोक्त दो लक्षण हों, उसे एक जाति कहा जा सकता है । जातियाँ स्थाई इकाइयाँ नहीं हैं, इनमें संघटन, विघटन व परिवर्तन की शक्तियाँ काम करती रहती हैं।
___ कई बार वर्ण-व्यवस्थाको ही भ्रमसे जाति-व्यवस्था मान लिया जाता है। दोनों व्यवस्थाओं में कुछ सम्बन्ध तो है, पर वे अलग-अलग हैं। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रोंमें आर्योको चार वर्गों में बाँटा गया है। परन्तु उस समय भी बहुतसी जातियाँ ऐसी थीं, जो किसी एक वर्णमें नहीं रखी जा सकती थी। इन्हें वर्णसंकर माना गया। इनमेंसे कायस्थ जाति प्रसिद्ध है, इन्हें क्षत्रिय माना जाय या शूद्र, यह विवाद अभीतक चला आया है। कई बार यह प्रश्न ब्रिटिश अदालतोंमें भी उठाया गया था ।
कौनसी जाति किस वर्ण में है, इसका निर्णय कैसे किया जाये ? इसके बारेमें तीन प्रमुख मत है। आजकल सामान्य लोग जो प्रयोग करते हैं, उसे उदार मन कहा जा सकता है। इस मतसे विभाजन वर्तमान सामाजिक व आर्थिक स्थिति देखकर निर्णय किया जाता है। पिछली दो-तीन पीढ़ियोंके पहलेके इतिहासपर विचार नहीं किया जाता है। उदार मतसे भूस्वामी जातियाँ जैसे मराठे, कुर्मी, जाट आदि क्षत्रिय मानी जाती
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org