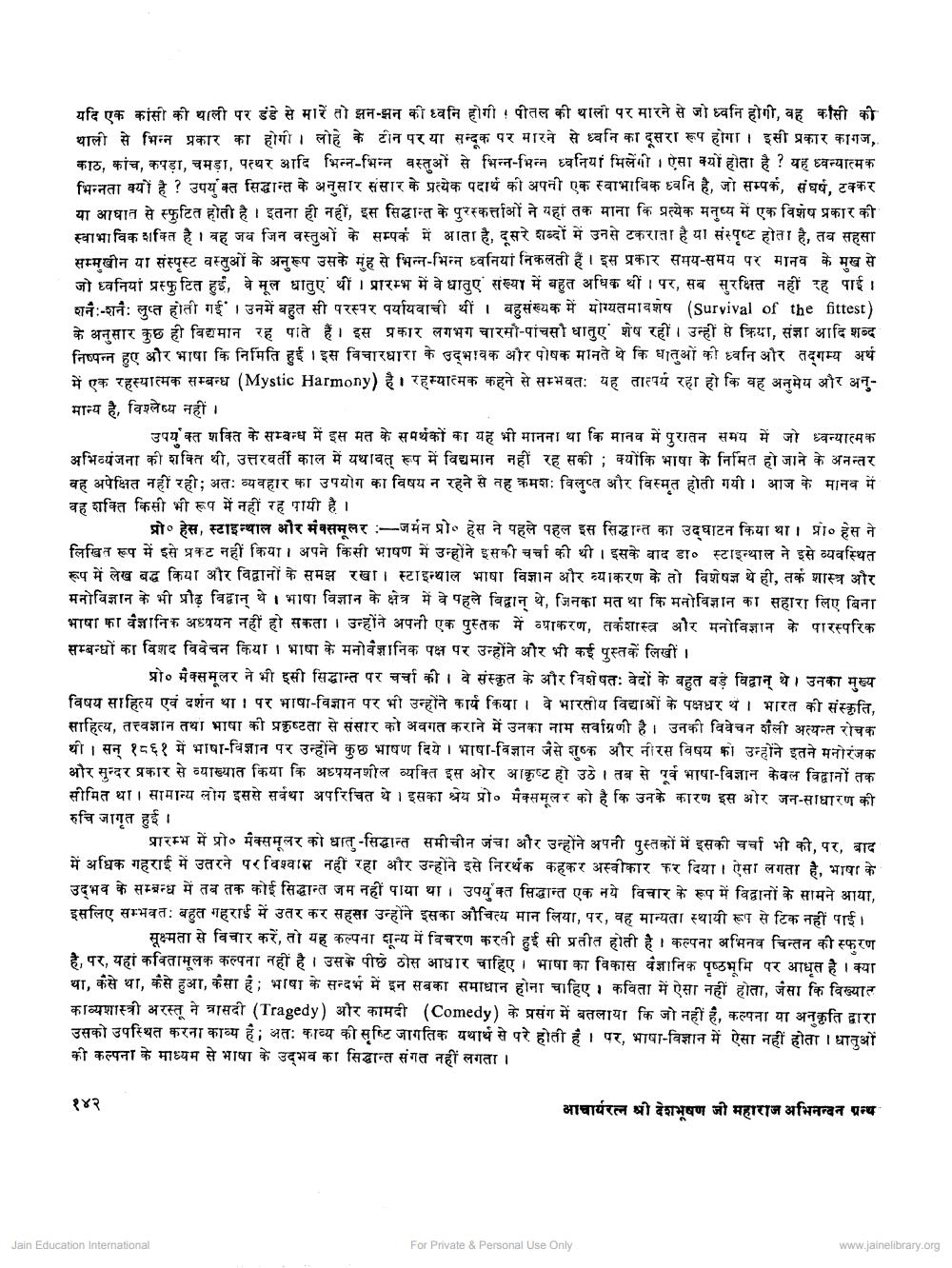________________
यदि एक कांसी की थाली पर डंडे से मारें तो झन-झन की ध्वनि होगी। पीतल की थाली पर मारने से जो ध्वनि होगी, वह कौसी की थाली से भिन्न प्रकार का होगी। लोहे के टीन पर या सन्दूक पर मारने से ध्वनि का दूसरा रूप होगा। इसी प्रकार कागज, काठ, कांच, कपड़ा, चमड़ा, पत्थर आदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं से भिन्न-भिन्न ध्वनियां मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है ? यह ध्वन्यात्मक भिन्नता क्यों है ? उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक स्वाभाविक ध्वनि है, जो सम्पर्क, संघर्ष, टक्कर या आघात से स्फुटित होती है । इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त के पुरस्कर्ताओं ने यहां तक माना कि प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है । वह जब जिन वस्तुओं के सम्पर्क में आता है, दूसरे शब्दों में उनसे टकराता है या संस्पृष्ट होता है, तब सहसा सम्मुखीन या संस्पृस्ट वस्तुओं के अनुरूप उसके मुंह से भिन्न-भिन्न ध्वनियां निकलती हैं । इस प्रकार समय-समय पर मानव के मुख से जो ध्वनियां प्रस्फुटित हुई, वे मूल धातुए थीं । प्रारम्भ में वे धातुए संख्या में बहुत अधिक थीं। पर, सब सुरक्षित नहीं रह पाई। शनैः-शनैः लुप्त होती गई। उनमें बहुत सी परस्पर पर्यायवाची थीं । बहुसंख्यक में योग्यतमावशेष (Survival of the fittest) के अनुसार कुछ ही विद्यमान रह पाते हैं। इस प्रकार लगभग चारमौ-पांचसौ धातुएं शेष रहीं। उन्हीं से क्रिया, संज्ञा आदि शब्द निष्पन्न हुए और भाषा कि निर्मिति हुई । इस विचारधारा के उद्भावक और पोषक मानते थे कि धातुओं की ध्वनि और तद्गम्य अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (Mystic Harmony) है। रहस्यात्मक कहने से सम्भवत: यह तात्पर्य रहा हो कि वह अनुमेय और अनुमान्य है, विश्लेष्य नहीं।
उपयुक्त शक्ति के सम्बन्ध में इस मत के समर्थकों का यह भी मानना था कि मानव में पुरातन समय में जो ध्वन्यात्मक अभिव्यंजना की शक्ति थी, उत्तरवर्ती काल में यथावत् रूप में विद्यमान नहीं रह सकी ; क्योंकि भाषा के निमित हो जाने के अनन्तर वह अपेक्षित नहीं रही; अतः व्यवहार का उपयोग का विषय न रहने से वह क्रमशः विलुप्त और विस्मत होती गयी। आज के मानव में वह शक्ति किसी भी रूप में नहीं रह पायी है।
प्रो० हेस, स्टाइन्थाल और मैक्समूलर :-जर्मन प्रो० हेस ने पहले पहल इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया था। प्रो० हेस ने लिखित रूप में इसे प्रकट नहीं किया। अपने किसी भाषण में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। इसके बाद डा० स्टाइन्थाल ने इसे व्यवस्थित रूप में लेख बद्ध किया और विद्वानों के समझ रखा। स्टाइन्थाल भाषा विज्ञान और व्याकरण के तो विशेषज्ञ थे ही, तर्क शास्त्र और मनोविज्ञान के भी प्रौढ़ विद्वान् थे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में वे पहले विद्वान थे, जिनका मत था कि मनोविज्ञान का सहारा लिए बिना भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता । उन्होंने अपनी एक पुस्तक में व्याकरण, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के पारस्परिक सम्बन्धों का विशद विवेचन किया । भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखीं।
प्रो० मैक्समूलर ने भी इसी सिद्धान्त पर चर्चा की। वे संस्कृत के और विशेषतः वेदों के बहुत बड़े विद्वान् थे। उनका मुख्य विषय साहित्य एवं दर्शन था। पर भाषा-विज्ञान पर भी उन्होंने कार्य किया। वे भारतीय विद्याओं के पक्षधर थ। भारत की संस्कृति, साहित्य, तत्त्वज्ञान तथा भाषा की प्रकृष्टता से संसार को अवगत कराने में उनका नाम सर्वाग्रणी है। उनकी विवेचन शैली अत्यन्त रोचक थी। सन १८६१ में भाषा-विज्ञान पर उन्होंने कुछ भाषण दिये । भाषा-विज्ञान जैसे शुष्क और नीरस विषय को उन्होंने इतने मनोरंजक और सुन्दर प्रकार से व्याख्यात किया कि अध्ययनशील व्यक्ति इस ओर आकृष्ट हो उठे। तब से पूर्व भाषा-विज्ञान केवल विद्वानों तक सीमित था। सामान्य लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे। इसका श्रेय प्रो० मैक्समूलर को है कि उनके कारण इस ओर जन-साधारण की रुचि जागृत हुई।
प्रारम्भ में प्रो० मैक्समूलर को धातु -सिद्धान्त समीचीन जंचा और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसकी चर्चा भी की, पर, बाद में अधिक गहराई में उतरने पर विश्वास नहीं रहा और उन्होंने इसे निरर्थक कहकर अस्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है, भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में तब तक कोई सिद्धान्त जम नहीं पाया था। उपयुक्त सिद्धान्त एक नये विचार के रूप में विद्वानों के सामने आया, इसलिए सम्भवत: बहुत गहराई में उतर कर सहसा उन्होंने इसका औचित्य मान लिया, पर, वह मान्यता स्थायी रूप से टिक नहीं पाई।
सूक्ष्मता से विचार करें, तो यह कल्पना शून्य में विचरण करती हुई सी प्रतीत होती है। कल्पना अभिनव चिन्तन की स्फुरण है, पर, यहां कवितामूलक कल्पना नहीं है । उसके पीछे ठोस आधार चाहिए। भाषा का विकास वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधृत है । क्या था, कैसे था, कैसे हुआ, कैसा है; भाषा के सन्दर्भ में इन सबका समाधान होना चाहिए। कविता में ऐसा नहीं होता, जैसा कि विख्यात काव्यशास्त्री अरस्तू ने त्रासदी (Tragedy) और कामदी (Comedy) के प्रसंग में बतलाया कि जो नहीं है, कल्पना या अनुकृति द्वारा उसको उपस्थित करना काव्य है; अतः काव्य की सृष्टि जागतिक यथार्थ से परे होती है। पर, भाषा-विज्ञान में ऐसा नहीं होता । धातुओं की कल्पना के माध्यम से भाषा के उद्भव का सिद्धान्त संगत नहीं लगता।
१४२
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन अन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org