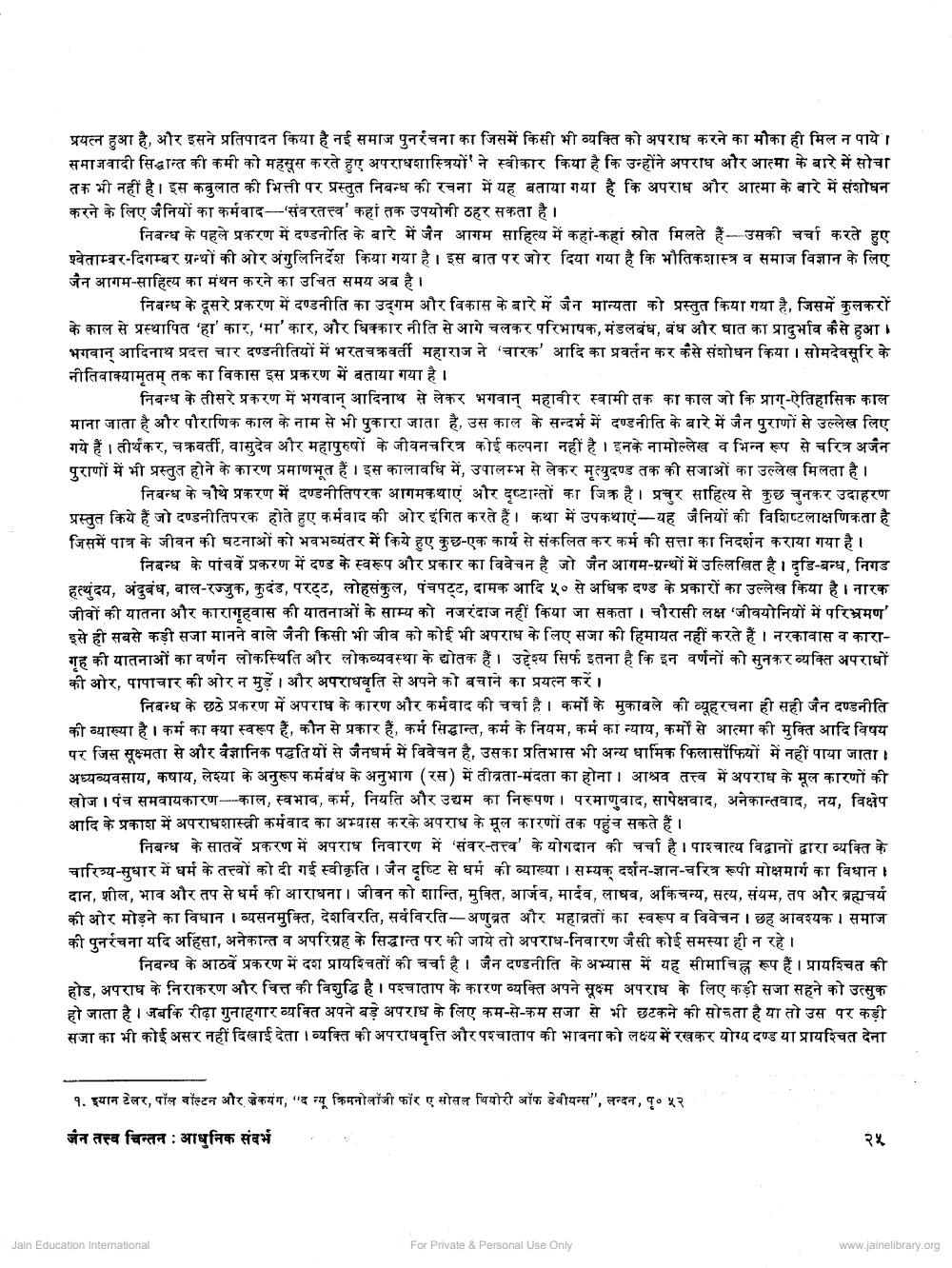________________
प्रयत्न हुआ है, और इसने प्रतिपादन किया है नई समाज पुनर्रचना का जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपराध करने का मौका ही मिल न पाये । समाजवादी सिद्धान्त की कमी को महसूस करते हुए अपराधशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपराध और आत्मा के बारे में सोचा तक भी नहीं है। इस कबुलात की भित्ती पर प्रस्तुत निबन्ध की रचना में यह बताया गया है कि अपराध और आत्मा के बारे में संशोधन करने के लिए जैनियों का कर्मवाद - 'संवरतत्त्व' कहां तक उपयोगी ठहर सकता है।
निबन्ध के पहले प्रकरण में दण्डनीति के बारे में जैन आगम साहित्य में कहां-कहां स्रोत मिलते हैं - उसकी चर्चा करते हुए श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थों की ओर अंगुलिनिर्देश किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि भौतिकशास्त्र व समाज विज्ञान के लिए जैन आगम - साहित्य का मंथन करने का उचित समय अब है ।
निबन्ध के दूसरे प्रकरण में दण्डनीति का उद्गम और विकास के बारे में जैन मान्यता को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुलकरों के काल से प्रस्थापित 'हा' कार, 'मा' कार, और धिक्कार नीति से आगे चलकर परिभाषक, मंडलबंध, बंध और घात का प्रादुर्भाव कैसे हुआ । भगवान् आदिनाथ प्रदत्त चार दण्डनीतियों में भरतचक्रवर्ती महाराज ने 'चारक' आदि का प्रवर्तन कर कैसे संशोधन किया । सोमदेवसूरि के नीतिवाक्यामृतम् तक का विकास इस प्रकरण में बताया गया है ।
निबन्ध के तीसरे प्रकरण में भगवान् आदिनाथ से लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक का काल जो कि प्राग्- ऐतिहासिक काल माना जाता है और पौराणिक काल के नाम से भी पुकारा जाता है, उस काल के सन्दर्भ में दण्डनीति के बारे में जैन पुराणों से उल्लेख लिए गये हैं। तीर्थकर चक्रवर्ती वासुदेव और महापुरुषों के जीवनचरित्र कोई कल्पना नहीं है। इनके नामोल्लेख व भिन्न रूप से चरित्र अर्जन पुराणों में भी प्रस्तुत होने के कारण प्रमाणभूत हैं। इस कालावधि में, उपालम्भ से लेकर मृत्युदण्ड तक की सजाओं का उल्लेख मिलता है ।
निबन्ध के चौथे प्रकरण में दण्डनीतिपरक आगमकथाएं और दृष्टान्तों का जिक्र है । प्रचुर साहित्य से कुछ चुनकर उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जो दण्डनीतिपरक होते हुए कर्मवाद की ओर इंगित करते हैं। कथा में उपकथाएं - यह जैनियों की विशिष्टलाक्षणिकता है जिसमें पात्र के जीवन की घटनाओं को भवभव्यंतर में किये हुए कुछ एक कार्य से संकलित कर कर्म की सत्ता का निदर्शन कराया गया है । निबन्ध के पांचवें प्रकरण में दण्ड के स्वरूप और प्रकार का विवेचन है जो जैन आगम ग्रन्थों में उल्लिखित है । दृडि-बन्ध, निगड हत्सुंदर, दुबंध, बाल-रज्जु कुदंड पट्ट, लोहसंकुल, पंचपट्ट, दामक आदि ५० से अधिक दण्ड के प्रकारों का उल्लेख किया है। नारक जीवों की यातना और कारागृहवास की यातनाओं के साम्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। चौरासी लक्ष 'जीवयोनियों में परिभ्रमण' इसे ही सबसे कड़ी सजा मानने वाले जैनी किसी भी जीव को कोई भी अपराध के लिए सजा की हिमायत नहीं करते हैं । नरकावास व कारागृह की यातनाओं का वर्णन लोकस्थिति और लोकव्यवस्था के द्योतक हैं । उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन वर्णनों को सुनकर व्यक्ति अपराधों की ओर, पापाचार की ओर न मुड़ें। और अपराधवृति से अपने को बचाने का प्रयत्न करें
1
निबन्ध के छठे प्रकरण में अपराध के कारण और कर्मवाद की चर्चा है । कर्मों के मुकाबले की व्यूहरचना ही सही जैन दण्डनीति की व्याख्या है। कर्म का क्या स्वरूप हैं, कौन से प्रकार हैं, कर्म सिद्धान्त, कर्म के नियम, कर्म का न्याय, कर्मों से आत्मा की मुक्ति आदि विषय पर जिस सूक्ष्मता से और वैज्ञानिक पद्धतियों से जैनधर्म में विवेचन है, उसका प्रतिभास भी अन्य धार्मिक फिलासॉफियों में नहीं पाया जाता । अध्यव्यवसाय, कषाय, लेश्या के अनुरूप कर्मबंध के अनुभाग (रस) में तीव्रता-मंदता का होना। आश्रव तत्त्व में अपराध के मूल कारणों की खोज । पंच समवायकारण काल, स्वभाव, कर्म, नियति और उद्यम का निरूपण । परमाणुवाद, सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद, नय, विक्षेप आदि के प्रकाश में अपराधशास्त्री कर्मवाद का अभ्यास करके अपराध के मूल कारणों तक पहुंच सकते हैं ।
निबन्ध के सातवें प्रकरण में अपराध निवारण में 'संवर-तत्त्व' के योगदान की चर्चा है । पाश्चात्य विद्वानों द्वारा व्यक्ति के चारित्र्य-सुधार में धर्म के तत्त्वों को दी गई स्वीकृति । जैन दृष्टि से धर्म की व्याख्या । सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चरित्र रूपी मोक्षमार्ग का विधान । दान, शील, भाव और तप से धर्म की आराधना । जीवन को शान्ति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, अकिंचन्य, सत्य, संयम, तप और ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ने का विधान । व्यसनमुक्ति, देशविरति, सर्वविरति - अणुव्रत और महाव्रतों का स्वरूप व विवेचन । छह आवश्यक । समाज की पुनर्रचना यदि अहिसा अनेकान्त व अपरिग्रह के सिद्धान्त पर की जाये तो अपराध-निवारण जैसी कोई समस्या ही न रहे।
निबन्ध के आठवें प्रकरण में दश प्रायश्चितों की चर्चा है। जैन दण्डनीति के अभ्यास में यह सीमाचिह्न रूप हैं। प्रायश्चित की होड, अपराध के निराकरण और चित्त की विशुद्धि है । पश्चाताप के कारण व्यक्ति अपने सूक्ष्म अपराध के लिए कड़ी सजा सहने को उत्सुक हो जाता है । जबकि रीढ़ा गुनाहगार व्यक्ति अपने बड़े अपराध के लिए कम-से-कम सजा से भी छटकने की सोचता है या तो उस पर कड़ी सजा का भी कोई असर नहीं दिखाई देता । व्यक्ति की अपराधवृत्ति और पश्चाताप की भावना को लक्ष्य में रखकर योग्य दण्ड या प्रायश्चित देना
१. इयान टेलर, पॉल वॉल्टन और जेकयंग, "द न्यू क्रिमनोलॉजी फॉर ए सोसल थियोरी ऑफ डेवीयन्स", लन्दन, पृ० ५२
जंन तत्व चिन्तन आधुनिक संदर्भ
:
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
२५
www.jainelibrary.org