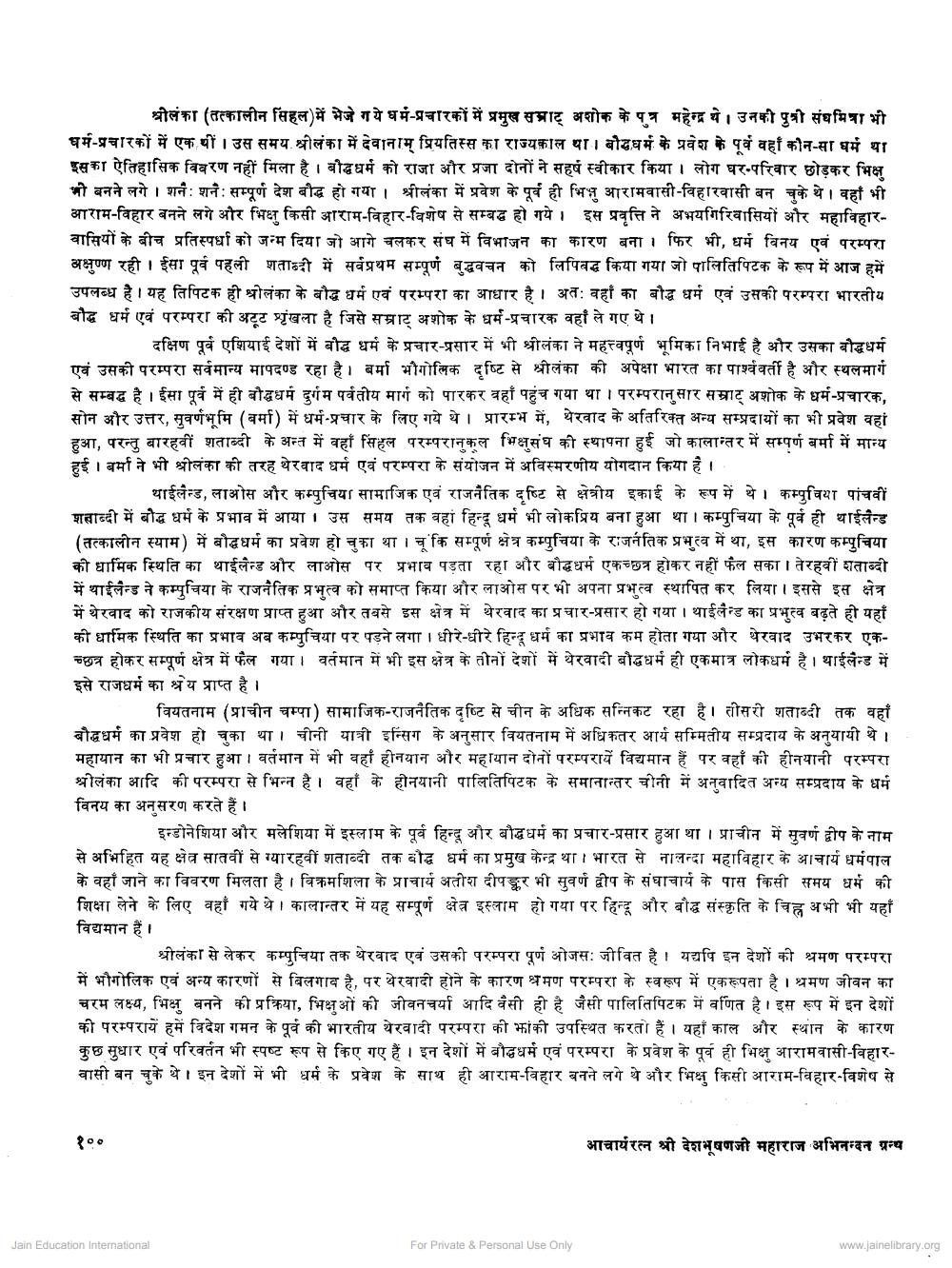________________
श्रीलंका (तत्कालीन सिंहल)में भेजे गये धर्म-प्रचारकों में प्रमुख सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र थे। उनकी पुत्री संघमित्रा भी धर्म-प्रचारकों में एक थीं। उस समय श्रीलंका में देवानाम् प्रियतिस्स का राज्यकाल था। बौद्धधर्म के प्रवेश के पूर्व वहाँ कौन-सा धर्म था इसका ऐतिहासिक विवरण नहीं मिला है । बौद्धधर्म को राजा और प्रजा दोनों ने सहर्ष स्वीकार किया। लोग घर-परिवार छोड़कर भिक्ष भी बनने लगे । शनैः शनैः सम्पूर्ण देश बौद्ध हो गया। श्रीलंका में प्रवेश के पूर्व ही भिक्षु आरामवासी-विहारवासी बन चुके थे। वहाँ भी आराम-विहार बनने लगे और भिक्षु किसी आराम-विहार-विशेष से सम्बद्ध हो गये। इस प्रवृत्ति ने अभयगिरिवासियों और महाविहारवासियों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया जो आगे चलकर संघ में विभाजन का कारण बना। फिर भी, धर्म विनय एवं परम्परा अक्षुण्ण रही । ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सर्वप्रथम सम्पूर्ण बुद्धवचन को लिपिबद्ध किया गया जो पालितिपिटक के रूप में आज हमें उपलब्ध है। यह तिपिटक ही श्रीलंका के बौद्ध धर्म एवं परम्परा का आधार है। अत: वहाँ का बौद्ध धर्म एवं उसकी परम्परा भारतीय बौद्ध धर्म एवं परम्परा की अटूट शृंखला है जिसे सम्राट अशोक के धर्म-प्रचारक वहाँ ले गए थे।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में भी श्रीलंका ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसका बौद्धधर्म एवं उसकी परम्परा सर्वमान्य मापदण्ड रहा है। बर्मा भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका की अपेक्षा भारत का पार्श्ववर्ती है और स्थलमार्ग से सम्बद्ध है । ईसा पूर्व में ही बौद्धधर्म दुर्गम पर्वतीय मार्ग को पारकर वहाँ पहुंच गया था। परम्परानुसार सम्राट अशोक के धर्म-प्रचारक, सोन और उत्तर, सुवर्णभूमि (बर्मा) में धर्म प्रचार के लिए गये थे। प्रारम्भ में, थेरवाद के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों का भी प्रवेश वहां हुआ, परन्तु बारहवीं शताब्दी के अन्त में वहाँ सिंहल परम्परानुकल भिक्षुसंघ की स्थापना हुई जो कालान्तर में सम्पर्ण बर्मा में मान्य हुई । बर्मा ने भी श्रीलंका की तरह थेरवाद धर्म एवं परम्परा के संयोजन में अविस्मरणीय योगदान किया है।
थाईलैन्ड, लाओस और कम्पुचिया सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से क्षेत्रीय इकाई के रूप में थे। कम्पुचिया पांचवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। उस समय तक वहां हिन्दू धर्म भी लोकप्रिय बना हुआ था। कम्पुचिया के पूर्व ही थाईलैन्ड (तत्कालीन स्याम) में बौद्धधर्म का प्रवेश हो चुका था । चूकि सम्पूर्ण क्षेत्र कम्पुचिया के राजनैतिक प्रभुत्व में था, इस कारण कम्पुचिया की धार्मिक स्थिति का थाईलैन्ड और लाओस पर प्रभाव पड़ता रहा और बौद्धधर्म एकच्छत्र होकर नहीं फैल सका । तेरहवीं शताब्दी में थाईलैन्ड ने कम्पुचिया के राजनैतिक प्रभुत्व को समाप्त किया और लाओस पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इससे इस क्षेत्र में थेरवाद को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और तबसे इस क्षेत्र में थेरवाद का प्रचार-प्रसार हो गया । थाईलैन्ड का प्रभुत्व बढ़ते ही यहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव अब कम्पुचिया पर पड़ने लगा । धीरे-धीरे हिन्दू धर्म का प्रभाव कम होता गया और थेरवाद उभर कर एकच्छत्र होकर सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल गया। वर्तमान में भी इस क्षेत्र के तीनों देशों में थेरवादी बौद्धधर्म ही एकमात्र लोकधर्म है। थाईलैन्ड में इसे राजधर्म का श्रेय प्राप्त है।
वियतनाम (प्राचीन चम्पा) सामाजिक-राजनैतिक दृष्टि से चीन के अधिक सन्निकट रहा है। तीसरी शताब्दी तक वहाँ बौद्धधर्म का प्रवेश हो चुका था। चीनी यात्री इन्सिग के अनुसार वियतनाम में अधिकतर आर्य सम्मितीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। महायान का भी प्रचार हुआ। वर्तमान में भी वहाँ हीनयान और महायान दोनों परम्परायें विद्यमान हैं पर वहाँ की हीनयानी परम्परा श्रीलंका आदि की परम्परा से भिन्न है। वहाँ के हीनयानी पालितिपिटक के समानान्तर चीनी में अनुवादित अन्य सम्प्रदाय के धर्म विनय का अनुसरण करते हैं।
___ इन्डोनेशिया और मलेशिया में इस्लाम के पूर्व हिन्दू और बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार हुआ था । प्राचीन में सुवर्ण द्वीप के नाम से अभिहित यह क्षेत्र सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था। भारत से नालन्दा महाविहार के आचार्य धर्मपाल के वहाँ जाने का विवरण मिलता है। विक्रमशिला के प्राचार्य अतीश दीपङ्कर भी सुवर्ण द्वीप के संघाचार्य के पास किसी समय धर्म की शिक्षा लेने के लिए वहाँ गये थे। कालान्तर में यह सम्पूर्ण क्षेत्र इस्लाम हो गया पर हिन्दू और बौद्ध संस्कृति के चिह्न अभी भी यहाँ विद्यमान हैं।
श्रीलंका से लेकर कम्पुचिया तक थेरवाद एवं उसकी परम्परा पूर्ण ओजसः जीवित है। यद्यपि इन देशों की श्रमण परम्परा में भौगोलिक एवं अन्य कारणों से बिलगाव है, पर थेरवादी होने के कारण श्रमण परम्परा के स्वरूप में एकरूपता है । श्रमण जीवन का चरम लक्ष्य, भिक्षु बनने की प्रक्रिया, भिक्षुओं की जीवनचर्या आदि वैसी ही है जैसी पालितिपिटक में वर्णित है। इस रूप में इन देशों की परम्परायें हमें विदेश गमन के पूर्व की भारतीय थेरवादी परम्परा की झांकी उपस्थित करतो हैं । यहाँ काल और स्थान के कारण कुछ सुधार एवं परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से किए गए हैं । इन देशों में बौद्धधर्म एवं परम्परा के प्रवेश के पूर्व ही भिक्षु आरामवासी-विहारवासी बन चुके थे। इन देशों में भी धर्म के प्रवेश के साथ ही आराम-विहार बनने लगे थे और भिक्षु किसी आराम-विहार-विशेष से
आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org