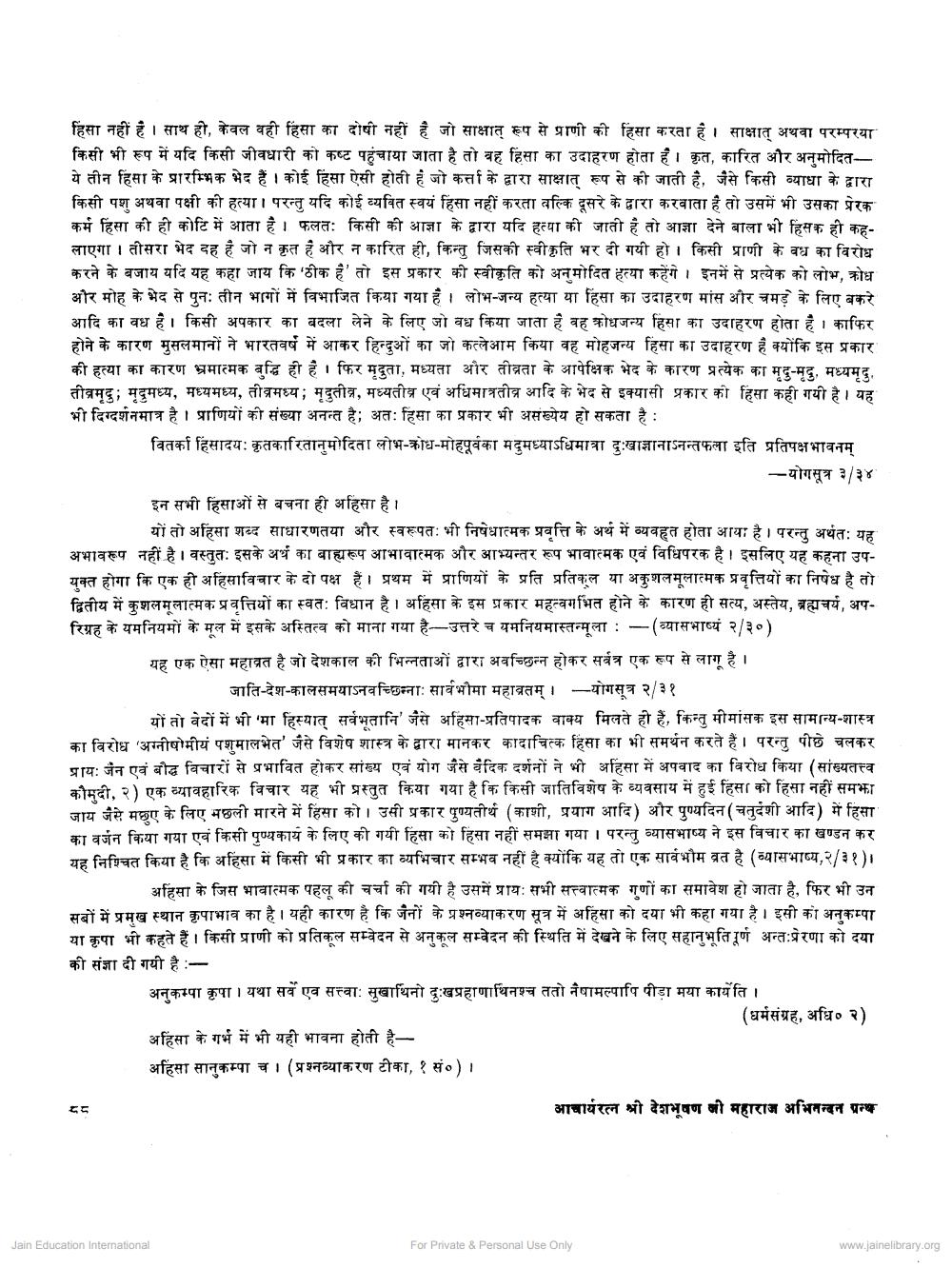________________
हिंसा नहीं है । साथ ही, केवल वही हिंसा का दोषी नहीं है जो साक्षात् रूप से प्राणी की हिंसा करता है। साक्षात् अथवा परम्परया किसी भी रूप में यदि किसी जीवधारी को कष्ट पहुंचाया जाता है तो वह हिंसा का उदाहरण होता है। कृत, कारित और अनुमोदितये तीन हिंसा के प्रारम्भिक भेद हैं । कोई हिंसा ऐसी होती है जो कर्ता के द्वारा साक्षात् रूप से की जाती है, जैसे किसी व्याधा के द्वारा किसी पशु अथवा पक्षी की हत्या। परन्तु यदि कोई व्यवित स्वयं हिंसा नहीं करता बल्कि दूसरे के द्वारा करवाता है तो उसमें भी उसका प्रेरक कर्म हिंसा की ही कोटि में आता है। फलत: किसी की आज्ञा के द्वारा यदि हत्या की जाती है तो आज्ञा देने बाला भी हिसक ही कहलाएगा। तीसरा भेद दह है जो न कृत है और न कारित ही, किन्तु जिसकी स्वीकृति भर दी गयी हो। किसी प्राणी के वध का विरोध करने के बजाय यदि यह कहा जाय कि 'ठीक है' तो इस प्रकार की स्वीकृति को अनुमोदित हत्या कहेंगे। इनमें से प्रत्येक को लोभ, क्रोध और मोह के भेद से पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। लोभ-जन्य हत्या या हिंसा का उदाहरण मांस और चमड़े के लिए बकरे आदि का वध है। किसी अपकार का बदला लेने के लिए जो वध किया जाता है वह क्रोधजन्य हिसा का उदाहरण होता है । काफिर होने के कारण मुसलमानों ने भारतवर्ष में आकर हिन्दुओं का जो कत्लेआम किया वह मोहजन्य हिंसा का उदाहरण है क्योंकि इस प्रकार की हत्या का कारण भ्रमात्मक बुद्धि ही है। फिर मृदुता, मध्यता और तीव्रता के आपेक्षिक भेद के कारण प्रत्येक का मदु-मद्, मध्यमद, तीव्रमदु; मृदुमध्य, मध्यमध्य, तीव्रमध्य; मृदुतीन, मध्यतीव्र एवं अधिमात्रतीव्र आदि के भेद से इक्यासी प्रकार को हिंसा कही गयी है। यह भी दिग्दर्शनमात्र है । प्राणियों की संख्या अनन्त है; अतः हिंसा का प्रकार भी असंख्येय हो सकता है : वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ-क्रोध-मोहपूर्वका मदुमध्याऽधिमात्रा दुःखाज्ञानाऽनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्
-योगसूत्र ३/३४ इन सभी हिंसाओं से बचना ही अहिंसा है।
यों तो अहिंसा शब्द साधारणतया और स्वरूपतः भी निषेधात्मक प्रवृत्ति के अर्थ में व्यवहृत होता आया है। परन्तु अर्थत: यह अभावरूप नहीं है। वस्तुतः इसके अर्थ का बाह्यरूप आभावात्मक और आभ्यन्तर रूप भावात्मक एवं विधिपरक है। इसलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि एक ही अहिंसाविचार के दो पक्ष हैं। प्रथम में प्राणियों के प्रति प्रतिकुल या अकुशलमूलात्मक प्रवृत्तियों का निषेध है तो द्वितीय में कुशलमूलात्मक प्रवृत्तियों का स्वत: विधान है। अहिंसा के इस प्रकार महत्वगभित होने के कारण ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के यमनियमों के मूल में इसके अस्तित्व को माना गया है-उत्तरे च यमनियमास्तन्मूला : -(व्यासभाष्यं २/३०) यह एक ऐसा महाव्रत है जो देशकाल की भिन्नताओं द्वारा अवच्छिन्न होकर सर्वत्र एक रूप से लागू है।
जाति-देश-कालसमयाऽनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। -योगसूत्र २/३१ यों तो वेदों में भी 'मा हिस्यात् सर्वभूतानि' जैसे अहिंसा-प्रतिपादक वाक्य मिलते ही हैं, किन्तु मीमांसक इस सामान्य-शास्त्र का विरोध 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' जैसे विशेष शास्त्र के द्वारा मानकर कादाचित्क हिंसा का भी समर्थन करते हैं। परन्तु पीछे चलकर प्राय: जैन एवं बौद्ध विचारों से प्रभावित होकर सांख्य एवं योग जैसे वैदिक दर्शनों ने भी अहिंसा में अपवाद का विरोध किया (सांख्यतत्त्व कौमदी, २) एक व्यावहारिक विचार यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी जातिविशेष के व्यवसाय में हुई हिंसा को हिसा नहीं समझा जाय जैसे मछुए के लिए मछली मारने में हिंसा को। उसी प्रकार पुण्यतीर्थ (काशी, प्रयाग आदि) और पुण्यदिन (चतुर्दशी आदि) में हिंसा का वर्जन किया गया एवं किसी पुण्यकार्य के लिए की गयी हिंसा को हिंसा नहीं समझा गया । परन्तु व्यासभाष्य ने इस विचार का खण्डन कर यह निश्चित किया है कि अहिंसा में किसी भी प्रकार का व्यभिचार सम्भव नहीं है क्योंकि यह तो एक सार्वभौम व्रत है (व्यासभाष्य,२/३१)।
अहिंसा के जिस भावात्मक पहलू की चर्चा की गयी है उसमें प्रायः सभी सत्त्वात्मक गुणों का समावेश हो जाता है, फिर भी उन सबों में प्रमख स्थान कृपाभाव का है। यही कारण है कि जैनों के प्रश्नव्याकरण सूत्र में अहिंसा को दया भी कहा गया है। इसी को अनुकम्पा या कृपा भी कहते हैं। किसी प्राणी को प्रतिकूल सम्वेदन से अनुकूल सम्वेदन की स्थिति में देखने के लिए सहानुभूति पूर्ण अन्तःप्रेरणा को दया की संज्ञा दी गयी है :अनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एव सत्त्वाः सुखाथिनो दुःखप्रहाणार्थिनश्च ततो नैषामल्पापि पीड़ा मया कार्यति ।
(धर्मसंग्रह, अधि० २) अहिंसा के गर्भ में भी यही भावना होती हैअहिंसा सानुकम्पा च । (प्रश्नव्याकरण टीका, १ सं०)।
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org