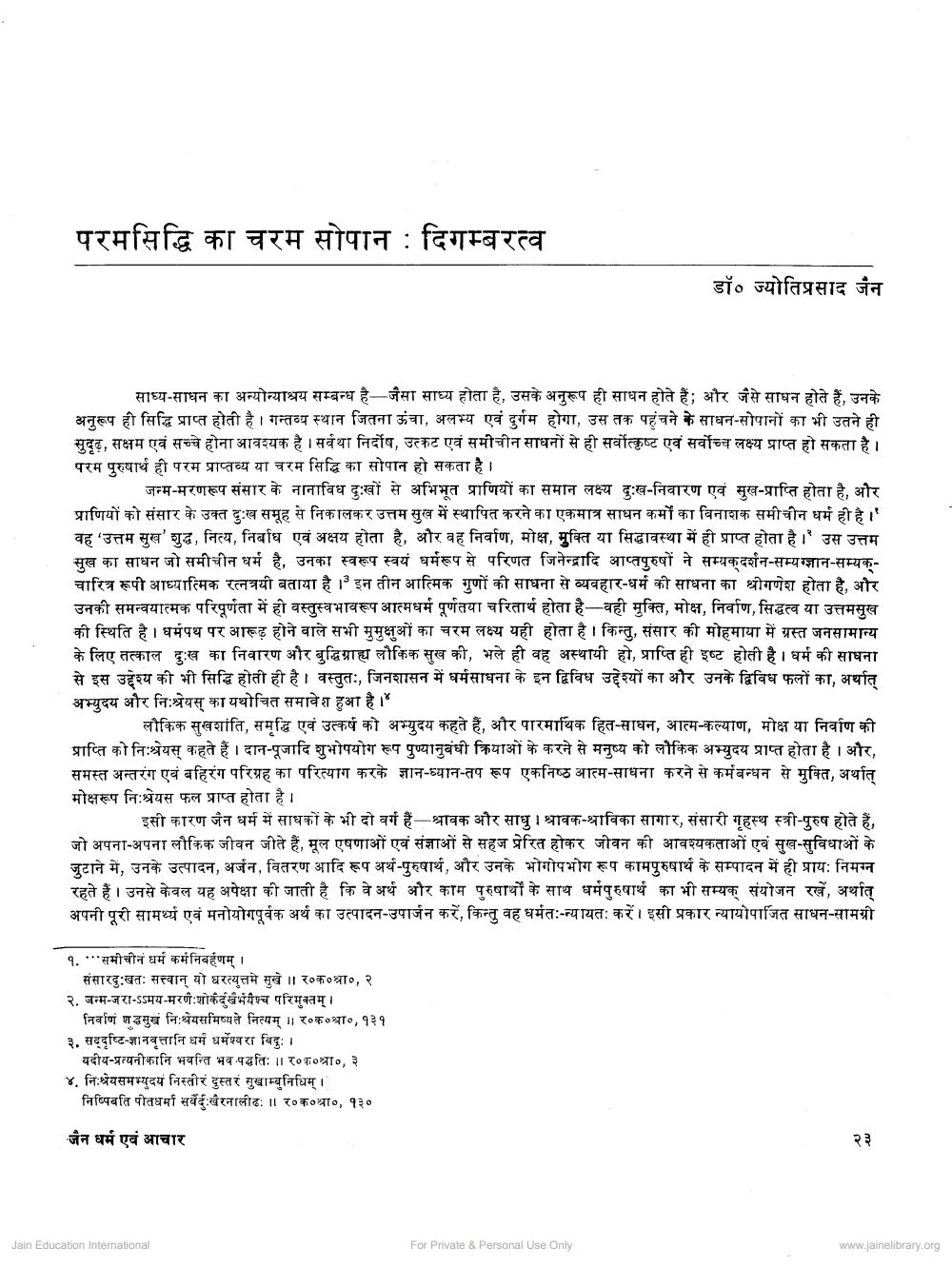________________
परमसिद्धि का चरम सोपान : दिगम्बरत्व
डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन
साध्य-साधन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है—जैसा साध्य होता है, उसके अनुरूप ही साधन होते हैं; और जैसे साधन होते हैं, उनके अनुरूप ही सिद्धि प्राप्त होती है। गन्तव्य स्थान जितना ऊंचा, अलभ्य एवं दुर्गम होगा, उस तक पहुंचने के साधन-सोपानों का भी उतने ही सुदृढ़, सक्षम एवं सच्चे होना आवश्यक है । सर्वथा निर्दोष, उत्कट एवं समीचीन साधनों से ही सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। परम पुरुषार्थ ही परम प्राप्तव्य या चरम सिद्धि का सोपान हो सकता है।
जन्म-मरणरूप संसार के नानाविध दुःखों से अभिभूत प्राणियों का समान लक्ष्य दुःख-निवारण एवं सुख-प्राप्ति होता है, और प्राणियों को संसार के उक्त दुःख समूह से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करने का एकमात्र साधन कर्मों का विनाशक समीचीन धर्म ही है।' वह 'उत्तम सुख' शुद्ध, नित्य, निर्बाध एवं अक्षय होता है, और वह निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या सिद्धावस्था में ही प्राप्त होता है। उस उत्तम सुख का साधन जो समीचीन धर्म है, उनका स्वरूप स्वयं धर्मरूप से परिणत जिनेन्द्रादि आप्तपुरुषों ने सम्यक् दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्र रूपी आध्यात्मिक रत्नत्रयी बताया है। इन तीन आत्मिक गुणों की साधना से व्यवहार-धर्म की साधना का श्रीगणेश होता है, और उनकी समन्वयात्मक परिपूर्णता में ही वस्तुस्वभावरूप आत्मधर्म पूर्णतया चरितार्थ होता है-वही मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, सिद्धत्व या उत्तमसुख की स्थिति है। धर्मपथ पर आरूढ़ होने वाले सभी मुमुक्षुओं का चरम लक्ष्य यही होता है। किन्तु, संसार की मोहमाया में ग्रस्त जनसामान्य के लिए तत्काल दुःख का निवारण और बुद्धिग्राह्य लौकिक सुख की, भले ही वह अस्थायी हो, प्राप्ति ही इष्ट होती है। धर्म की साधना से इस उद्देश्य की भी सिद्धि होती ही है। वस्तुतः, जिनशासन में धर्मसाधना के इन द्विविध उद्देश्यों का और उनके द्विविध फलों का, अर्थात् अभ्युदय और निःश्रेयस् का यथोचित समावेश हुआ है।
लौकिक सुखशांति, समृद्धि एवं उत्कर्ष को अभ्युदय कहते हैं, और पारमार्थिक हित-साधन, आत्म-कल्याण, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति को निःश्रेयस् कहते हैं । दान-पूजादि शुभोपयोग रूप पुण्यानुबंधी क्रियाओं के करने से मनुष्य को लौकिक अभ्युदय प्राप्त होता है । और, समस्त अन्तरंग एवं बहिरंग परिग्रह का परित्याग करके ज्ञान-ध्यान-तप रूप एकनिष्ठ आत्म-साधना करने से कर्मबन्धन से मुक्ति, अर्थात मोक्षरूप निःश्रेयस फल प्राप्त होता है।
इसी कारण जैन धर्म में साधकों के भी दो वर्ग हैं-श्रावक और साधु । श्रावक-श्राविका सागार, संसारी गृहस्थ स्त्री-पुरुष होते हैं, जो अपना-अपना लौकिक जीवन जीते हैं, मूल एषणाओं एवं संज्ञाओं से सहज प्रेरित होकर जीवन की आवश्यकताओं एवं सुख-सुविधाओं के जुटाने में, उनके उत्पादन, अर्जन, वितरण आदि रूप अर्थ-पुरुषार्थ, और उनके भोगोपभोग रूप कामपुरुषार्थ के सम्पादन में ही प्रायः निमग्न रहते हैं । उनसे केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वे अर्थ और काम पुरुषार्थों के साथ धर्मपुरुषार्थ का भी सम्यक् संयोजन रखें, अर्थात् अपनी पूरी सामर्थ्य एवं मनोयोगपूर्वक अर्थ का उत्पादन-उपार्जन करें, किन्तु वह धर्मत:-न्यायत: करें। इसी प्रकार न्यायोपाजित साधन-सामग्री
१. ''समीचीनं धर्म कर्मनिबर्हणम् ।
संसारदु:खतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे । र०क० श्रा०, २ २. जन्म-जरा-ऽऽमय-मरणःशोकदुखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥ र०कश्रा०, १३१ ३. सद्दृष्टि-ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धतिः ।। २००श्रा०,३ ४. निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् ।
निष्पिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः ।। र०क०या०, १३०
जैन धर्म एवं आचार
२३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org